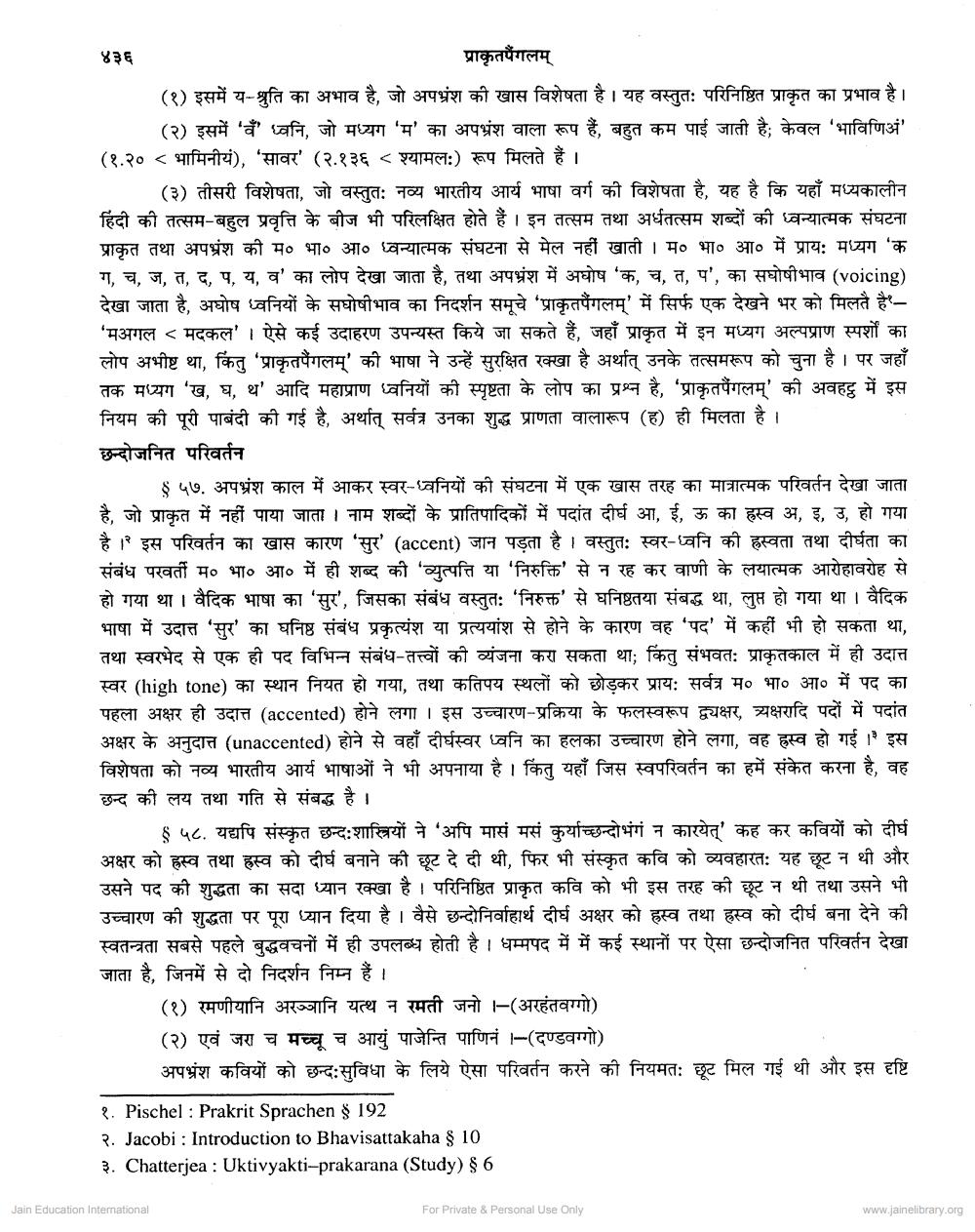________________
प्राकृतपैंगलम्
(१) इसमें य- श्रुति का अभाव है, जो अपभ्रंश की खास विशेषता है। यह वस्तुतः परिनिष्ठित प्राकृत का प्रभाव है। (२) इसमें 'वँ' ध्वनि, जो मध्यग 'म' का अपभ्रंश वाला रूप हैं, बहुत कम पाई जाती है; केवल 'भाविणिअं' ( १.२० < भामिनीयं), 'सावर' (२.१३६ ८ श्यामलः) रूप मिलते हैं।
४३६
"
(३) तीसरी विशेषता, जो वस्तुतः नव्य भारतीय आर्य भाषा वर्ग की विशेषता है, यह है कि यहाँ मध्यकालीन हिंदी की तत्सम बहुल प्रवृत्ति के बीज भी परिलक्षित होते हैं। इन तत्सम तथा अर्धतत्सम शब्दों की ध्वन्यात्मक संघटना प्राकृत तथा अपभ्रंश की म० भा० आ० ध्वन्यात्मक संघटना से मेल नहीं खाती। म० भा० आ० में प्रायः मध्यग 'क ग, च, ज, त, द, प, य, व' का लोप देखा जाता है, तथा अपभ्रंश में अघोष 'क, च, त, प' का सघोषीभाव (voicing) देखा जाता है, अघोष ध्वनियों के सघोषीभाव का निदर्शन समूचे 'प्राकृतपैंगलम्' में सिर्फ एक देखने भर को मिलते है''मअगल - मदकल' । ऐसे कई उदाहरण उपन्यस्त किये जा सकते हैं, जहाँ प्राकृत में इन मध्यग अल्पप्राण स्पर्शो का लोप अभीष्ट था, किंतु 'प्राकृतपैंगलम्' की भाषा ने उन्हें सुरक्षित रक्खा है अर्थात् उनके तत्समरूप को चुना है । पर जहाँ तक मध्यग 'ख, घ, थ' आदि महाप्राण ध्वनियों की स्पृष्टता के लोप का प्रश्न है, 'प्राकृतपैंगलम्' की अवहट्ट में इस नियम की पूरी पाबंदी की गई है, अर्थात् सर्वत्र उनका शुद्ध प्राणता वालारूप (ह) ही मिलता है।
छन्दोजनित परिवर्तन
५७. अपभ्रंश काल में आकर स्वर-ध्वनियों की संघटना में एक खास तरह का मात्रात्मक परिवर्तन देखा जाता है, जो प्राकृत में नहीं पाया जाता। नाम शब्दों के प्रातिपादिकों में पदांत दीर्घ आ, ई, ऊ का ह्रस्व अ, इ, उ, हो गया है। इस परिवर्तन का खास कारण 'सुर' (accent) जान पड़ता है। वस्तुतः स्वर ध्वनि की हस्वता तथा दीर्घता का संबंध परवर्ती म० भा० आ० में ही शब्द की व्युत्पत्ति या 'निरुक्ति' से न रह कर वाणी के लयात्मक आरोहावरोह से हो गया था। वैदिक भाषा का 'सुर', जिसका संबंध वस्तुतः 'निरुक्त' से घनिष्ठतया संबद्ध था, लुप्त हो गया था। वैदिक भाषा में उदात्त 'सुर' का घनिष्ठ संबंध प्रकृत्यंश या प्रत्ययांश से होने के कारण वह 'पद' में कहीं भी हो सकता था, तथा स्वरभेद से एक ही पद विभिन्न संबंध-तत्त्वों की व्यंजना करा सकता था; किंतु संभवत: प्राकृतकाल में ही उदात्त स्वर (high tone) का स्थान नियत हो गया, तथा कतिपय स्थलों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र म० भा० आ० में पद का पहला अक्षर ही उदात्त (accented) होने लगा। इस उच्चारण प्रक्रिया के फलस्वरूप द्वयक्षर, त्र्यक्षरादि पदों में पदांत अक्षर के अनुदात्त (unaccented) होने से वहाँ दीर्घस्वर ध्वनि का हलका उच्चारण होने लगा, वह ह्रस्व हो गई । इस विशेषता को नव्य भारतीय आर्य भाषाओं ने भी अपनाया है। किंतु यहाँ जिस स्वपरिवर्तन का हमें संकेत करना है, वह छन्द की लय तथा गति से संबद्ध है ।
$ ५८. यद्यपि संस्कृत छन्दः शास्त्रियों ने 'अपि मासं मसं कुर्याच्छन्दोभंगं न कारयेत्' कह कर कवियों को दीर्घ अक्षर को ह्रस्व तथा ह्रस्व को दीर्घ बनाने की छूट दे दी थी, फिर भी संस्कृत कवि को व्यवहारतः यह छूट न थी और उसने पद की शुद्धता का सदा ध्यान रक्खा है। परिनिष्ठित प्राकृत कवि को भी इस तरह की छूट न थी तथा उसने भी उच्चारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया है। वैसे छन्दोनिर्वाहार्थ दीर्घ अक्षर को हस्व तथा ह्रस्व को दीर्घ बना देने की स्वतन्त्रता सबसे पहले बुद्धवचनों में ही उपलब्ध होती है। धम्मपद में में कई स्थानों पर ऐसा छन्दोजनित परिवर्तन देखा जाता है, जिनमें से दो निदर्शन निम्न हैं ।
(१) रमणीयानि अरञ्ञानि यत्थ न रमती जनो । - ( अरहंतवग्गो)
(२) एवं जरा च मच्चू च आयुं पाजेन्ति पाणिनं । - ( दण्डवग्गो)
अपभ्रंश कवियों को छन्दः सुविधा के लिये ऐसा परिवर्तन करने की नियमतः छूट मिल गई थी और इस दृष्टि
१. Pischel : Prakrit Sprachen $ 192
२. Jacobi : Introduction to Bhavisattakaha $ 10
3. Chatterjea: Uktivyakti-prakarana (Study) § 6
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org