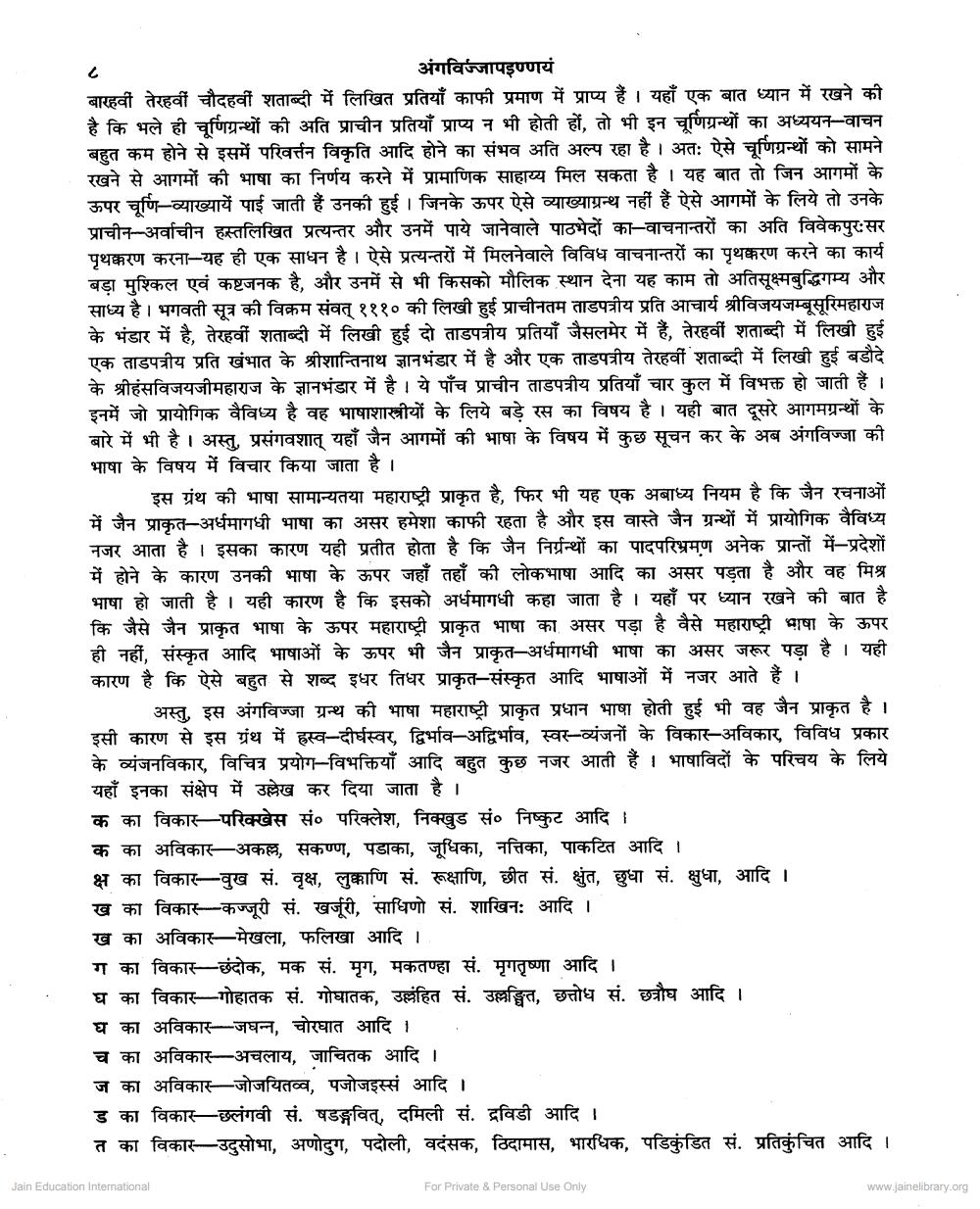________________
अंगविज्जापइण्णयं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में लिखित प्रतियाँ काफी प्रमाण में प्राप्य हैं । यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि भले ही चूर्णिग्रन्थों की अति प्राचीन प्रतियाँ प्राप्य न भी होती हों, तो भी इन चूर्णिग्रन्थों का अध्ययन-वाचन बहुत कम होने से इसमें परिवर्तन विकृति आदि होने का संभव अति अल्प रहा है। अत: ऐसे चूर्णिग्रन्थों को सामने रखने से आगमों की भाषा का निर्णय करने में प्रामाणिक साहाय्य मिल सकता है । यह बात तो जिन आगमों के ऊपर चूर्णि-व्याख्यायें पाई जाती हैं उनकी हुई । जिनके ऊपर ऐसे व्याख्याग्रन्थ नहीं हैं ऐसे आगमों के लिये तो उनके प्राचीन-अर्वाचीन हस्तलिखित प्रत्यन्तर और उनमें पाये जानेवाले पाठभेदों का-वाचनान्तरों का अति विवेकपुरःसर पृथक्करण करना-यह ही एक साधन है। ऐसे प्रत्यन्तरों में मिलनेवाले विविध वाचनान्तरों का पृथक्करण करने का कार्य बड़ा मुश्किल एवं कष्टजनक है, और उनमें से भी किसको मौलिक स्थान देना यह काम तो अतिसूक्ष्मबुद्धिगम्य और साध्य है। भगवती सूत्र की विक्रम संवत् १११० की लिखी हुई प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रति आचार्य श्रीविजयजम्बूसूरिमहाराज के भंडार में है, तेरहवीं शताब्दी में लिखी हुई दो ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेर में हैं, तेरहवीं शताब्दी में लिखी हुई एक ताडपत्रीय प्रति खंभात के श्रीशान्तिनाथ ज्ञानभंडार में है और एक ताडपत्रीय तेरहवीं शताब्दी में लिखी हुई बडौदे के श्रीहंसविजयजीमहाराज के ज्ञानभंडार में है। ये पाँच प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियाँ चार कुल में विभक्त हो जाती हैं । इनमें जो प्रायोगिक वैविध्य है वह भाषाशास्त्रीयों के लिये बड़े रस का विषय है। यही बात दूसरे आगमग्रन्थों के बारे में भी है। अस्तु, प्रसंगवशात् यहाँ जैन आगमों की भाषा के विषय में कुछ सूचन कर के अब अंगविज्जा की भाषा के विषय में विचार किया जाता है।
इस ग्रंथ की भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्राकृत है, फिर भी यह एक अबाध्य नियम है कि जैन रचनाओं में जैन प्राकृत-अर्धमागधी भाषा का असर हमेशा काफी रहता है और इस वास्ते जैन ग्रन्थों में प्रायोगिक वैविध्य नजर आता है । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि जैन निर्ग्रन्थों का पादपरिभ्रमण अनेक प्रान्तों में प्रदेशों में होने के कारण उनकी भाषा के ऊपर जहाँ तहाँ की लोकभाषा आदि का असर पड़ता है और वह मिश्र भाषा हो जाती है। यही कारण है कि इसको अर्धमागधी कहा जाता है । यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जैसे जैन प्राकृत भाषा के ऊपर महाराष्ट्री प्राकृत भाषा का असर पड़ा है वैसे महाराष्ट्री भाषा के ऊपर ही नहीं, संस्कृत आदि भाषाओं के ऊपर भी जैन प्राकृत-अर्धमागधी भाषा का असर जरूर पड़ा है । यही कारण है कि ऐसे बहुत से शब्द इधर तिधर प्राकृत-संस्कृत आदि भाषाओं में नजर आते हैं।
अस्तु, इस अंगविज्जा ग्रन्थ की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत प्रधान भाषा होती हुई भी वह जैन प्राकृत है । इसी कारण से इस ग्रंथ में ह्रस्व-दीर्घस्वर, द्विर्भाव-अद्विर्भाव, स्वर-व्यंजनों के विकार-अविकार, विविध प्रकार के व्यंजनविकार, विचित्र प्रयोग-विभक्तियाँ आदि बहुत कुछ नजर आती हैं । भाषाविदों के परिचय के लिये यहाँ इनका संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाता है । क का विकार-परिक्खेस सं० परिक्लेश, निक्खुड सं० निष्कुट आदि । क का अविकार-अकल्ल, सकण्ण, पडाका, जूधिका, नत्तिका, पाकटित आदि । क्ष का विकार-वुख सं. वृक्ष, लुक्काणि सं. रूक्षाणि, छीत सं. झुंत, छुधा सं. क्षुधा, आदि । ख का विकार-कज्जूरी सं. खजूरी, साधिणो सं. शाखिनः आदि । ख का अविकार-मेखला, फलिखा आदि । ग का विकार-छंदोक, मक सं. मृग, मकतण्हा सं. मृगतृष्णा आदि । घ का विकार-गोहातक सं. गोघातक, उल्लंहित सं. उल्लङ्गित, छत्तोध सं. छत्रौघ आदि । घ का अविकार-जघन्न, चोरघात आदि । च का अविकार-अचलाय, जाचितक आदि । ज का अविकार-जोजयितव्व, पजोजइस्सं आदि । ड का विकार—छलंगवी सं. षडङ्गवित्, दमिली सं. द्रविडी आदि । त का विकार-उदुसोभा, अणोदुग, पदोली, वदंसक, ठिदामास, भारधिक, पडिकुंडित सं. प्रतिकुंचित आदि ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org