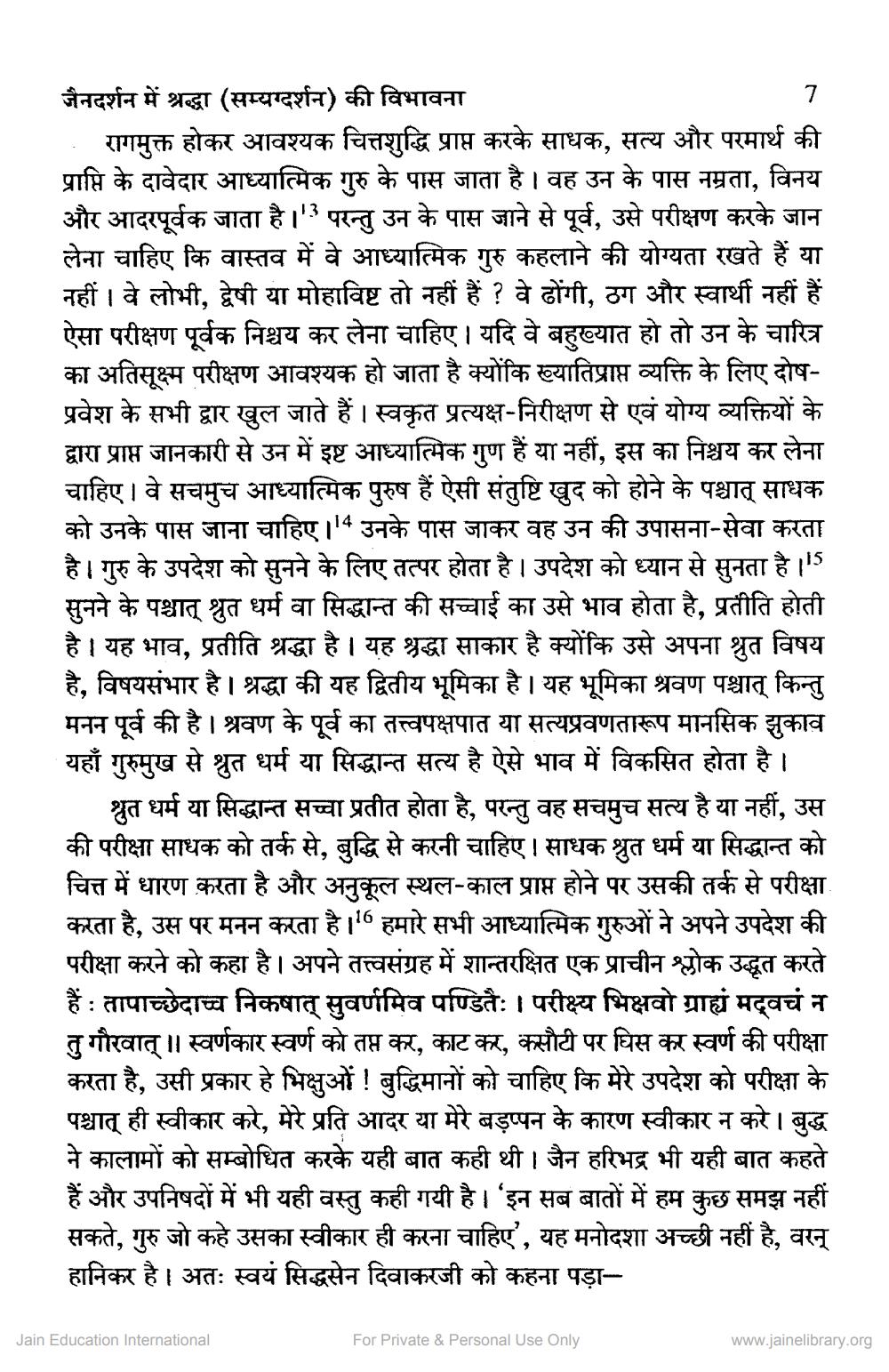________________
जैनदर्शन में श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) की विभावना . रागमुक्त होकर आवश्यक चित्तशुद्धि प्राप्त करके साधक, सत्य और परमार्थ की प्राप्ति के दावेदार आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है। वह उन के पास नम्रता, विनय
और आदरपूर्वक जाता है। परन्तु उन के पास जाने से पूर्व, उसे परीक्षण करके जान लेना चाहिए कि वास्तव में वे आध्यात्मिक गुरु कहलाने की योग्यता रखते हैं या नहीं । वे लोभी, द्वेषी या मोहाविष्ट तो नहीं हैं ? वे ढोंगी, ठग और स्वार्थी नहीं हैं ऐसा परीक्षण पूर्वक निश्चय कर लेना चाहिए। यदि वे बहुख्यात हो तो उन के चारित्र का अतिसूक्ष्म परीक्षण आवश्यक हो जाता है क्योंकि ख्यातिप्राप्त व्यक्ति के लिए दोषप्रवेश के सभी द्वार खुल जाते हैं। स्वकृत प्रत्यक्ष-निरीक्षण से एवं योग्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त जानकारी से उन में इष्ट आध्यात्मिक गुण हैं या नहीं, इस का निश्चय कर लेना चाहिए। वे सचमुच आध्यात्मिक पुरुष हैं ऐसी संतुष्टि खुद को होने के पश्चात् साधक को उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर वह उन की उपासना-सेवा करता है। गुरु के उपदेश को सुनने के लिए तत्पर होता है। उपदेश को ध्यान से सुनता है। सुनने के पश्चात् श्रुत धर्म वा सिद्धान्त की सच्चाई का उसे भाव होता है, प्रतीति होती है। यह भाव, प्रतीति श्रद्धा है । यह श्रद्धा साकार है क्योंकि उसे अपना श्रुत विषय है, विषयसंभार है। श्रद्धा की यह द्वितीय भूमिका है। यह भूमिका श्रवण पश्चात् किन्तु मनन पूर्व की है। श्रवण के पूर्व का तत्त्वपक्षपात या सत्यप्रवणतारूप मानसिक झुकाव यहाँ गुरुमुख से श्रुत धर्म या सिद्धान्त सत्य है ऐसे भाव में विकसित होता है।
श्रुत धर्म या सिद्धान्त सच्चा प्रतीत होता है, परन्तु वह सचमुच सत्य है या नहीं, उस की परीक्षा साधक को तर्क से, बुद्धि से करनी चाहिए। साधक श्रुत धर्म या सिद्धान्त को चित्त में धारण करता है और अनुकूल स्थल-काल प्राप्त होने पर उसकी तर्क से परीक्षा करता है, उस पर मनन करता है। हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने उपदेश की परीक्षा करने को कहा है। अपने तत्त्वसंग्रह में शान्तरक्षित एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं : तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः । परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचं न तु गौरवात् ॥ स्वर्णकार स्वर्ण को तप्त कर, काट कर, कसौटी पर घिस कर स्वर्ण की परीक्षा करता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं ! बुद्धिमानों को चाहिए कि मेरे उपदेश को परीक्षा के पश्चात् ही स्वीकार करे, मेरे प्रति आदर या मेरे बड़प्पन के कारण स्वीकार न करे । बुद्ध ने कालामों को सम्बोधित करके यही बात कही थी। जैन हरिभद्र भी यही बात कहते हैं और उपनिषदों में भी यही वस्तु कही गयी है। इन सब बातों में हम कुछ समझ नहीं सकते, गुरु जो कहे उसका स्वीकार ही करना चाहिए', यह मनोदशा अच्छी नहीं है, वरन् हानिकर है। अतः स्वयं सिद्धसेन दिवाकरजी को कहना पड़ा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org