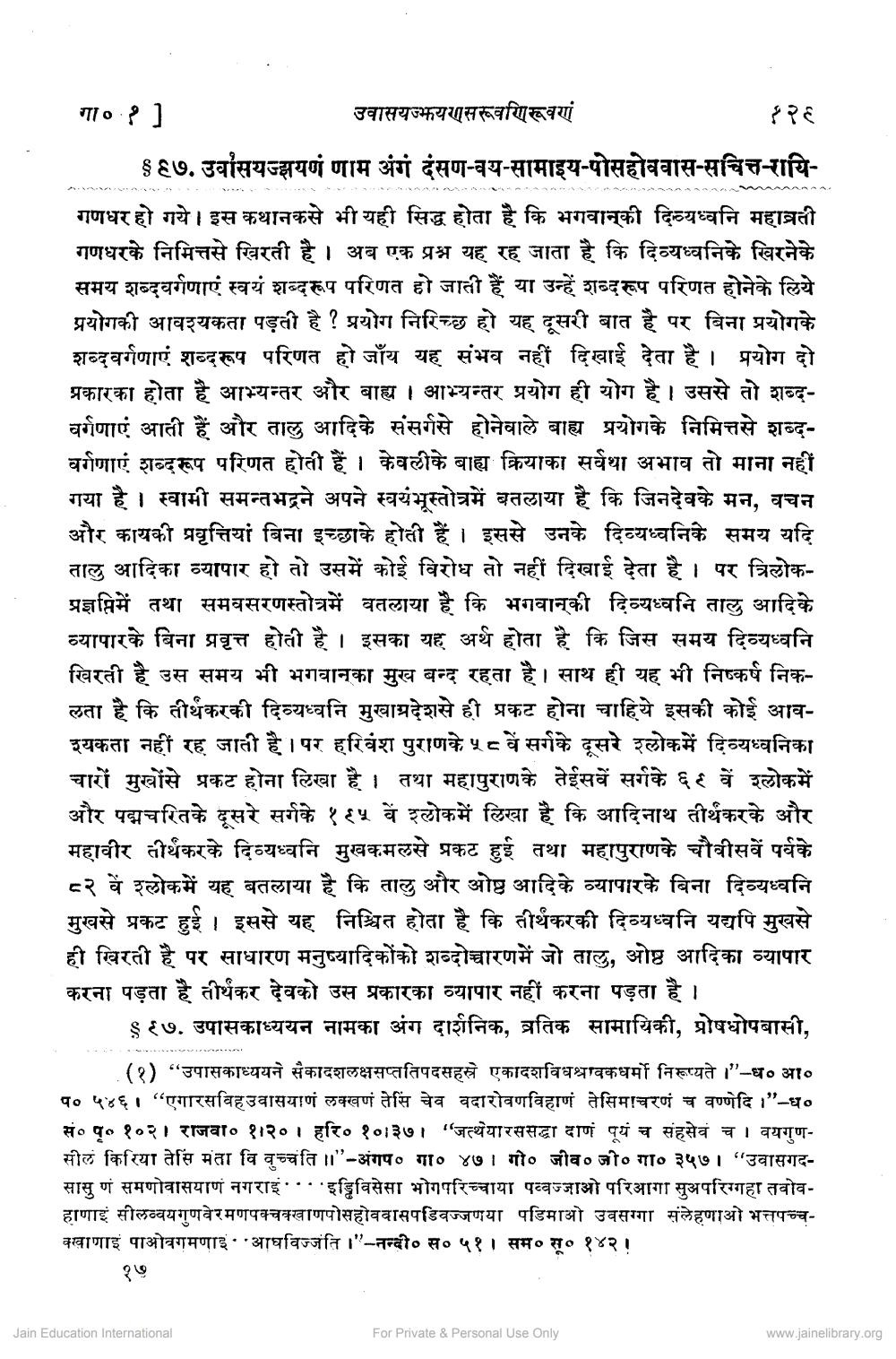________________
गा० १ ]
उवासयज्य सरूवणिरूवणं
१२६
६७. उवसयज्झयणं णाम अंगं दंसण-वय-सामाइय-पोसहोववास- सचित्त-रायिगणधर हो गये। इस कथानकसे भी यही सिद्ध होता है कि भगवान्की दिव्यध्वनि महाव्रती गणधर के निमित्तसे खिरती है । अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि दिव्यध्वनिके खिरने के समय शब्दवर्गणाएं स्वयं शब्दरूप परिणत हो जाती हैं या उन्हें शब्दरूप परिणत होनेके लिये प्रयोगकी आवश्यकता पड़ती है ? प्रयोग निरिच्छ हो यह दूसरी बात है पर बिना प्रयोगके शब्दवर्गणाएं शब्दरूप परिणत हो जाँय यह संभव नहीं दिखाई देता है । प्रयोग दो प्रकारका होता है आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर प्रयोग ही योग है। उससे तो शब्द - वर्गणाएं आती हैं और तालु आदिके संसर्गसे होनेवाले बाह्य प्रयोग के निमित्तसे शब्द - वर्गणाएं शब्दरूप परिणत होती हैं । केवलीके बाह्य क्रियाका सर्वथा अभाव तो माना नहीं गया है । स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयंभू स्तोत्रमें बतलाया है कि जिनदेवके मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियां बिना इच्छाके होती हैं । इससे उनके दिव्यध्वनिके समय यदि तालु आदिका व्यापार हो तो उसमें कोई विरोध तो नहीं दिखाई देता है । पर त्रिलोकप्रज्ञप्ति तथा समवसरणस्तोत्रमें वतलाया है कि भगवान्की दिव्यध्वनि तालु आदिके व्यापार के बिना प्रवृत्त होती है । इसका यह अर्थ होता है कि जिस समय दिव्यध्वनि खिरती है उस समय भी भगवानका मुख बन्द रहता है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थंकरकी दिव्यध्वनि मुखाग्रदेश से ही प्रकट होना चाहिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । पर हरिवंश पुराणके ५८ वें सर्गके दूसरे श्लोक में दिव्यध्वनिका चारों मुखोंसे प्रकट होना लिखा है । तथा महापुराणके तेईसवें सर्गके ६६ वें श्लोक में और पद्मचरित के दूसरे सर्गके १६५ वें श्लोक में लिखा है कि आदिनाथ तीर्थंकरके और महावीर तीर्थंकर के दिव्यध्वनि मुखकमलसे प्रकट हुई तथा महापुराणके चौबीसवें पर्वके ८२ वें श्लोक में यह बतलाया है कि तालु और ओष्ठ आदिके व्यापार के बिना दिव्यध्वनि मुख प्रकट हुई । इससे यह निश्चित होता है कि तीर्थंकरकी दिव्यध्वनि यद्यपि मुख ही खिरती है पर साधारण मनुष्यादिकोंको शब्दोच्चारणमें जो तालु, ओष्ठ आदिका व्यापार करना पड़ता है तीर्थंकर देवको उस प्रकारका व्यापार नहीं करना पड़ता है ।
$ २७. उपासकाध्ययन नामका अंग दार्शनिक, व्रतिक सामायिकी, प्रोषधोपबासी,
(१) “ उपासकाध्ययने सैकादशलक्षसप्ततिपदसहस्रे एकादशविधश्रावकधर्मो निरूप्यते ।" -ध० अ० प० ५४६ । “एगारसविहउवासयाणं लक्खणं तेसिं चेव वदारोवणविहाणं तेसिमाचरणं च वण्णेदि । " - ध० सं० पृ० १०२ । राजवा० १।२० । हरि० १० ३७ । “ जत्थेयारससद्धा दाणं पूयं च संहसेवं च । वयगुणसील किरिया तेसि मंता वि वुच्चति ।। " - अंगप० गा० ४७ । गो० जीव० जी० गा० ३५७ । “उवासगदसासु णं समणोवासयाणं नगराई इड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ परिआगा सुअपरिग्गहा तवोवहाणाई सीलव्वयगुणवेरमणपक्चक्खाणपोस होववासपडिवज्जणया पडिमाओ उवसग्गा संलेहणाओ भत्तपच्चक्वाणाई पाओवगमणाई आघविज्जति ।" - नन्दी० स० ५१ । सम० सू० १४२ ।
१७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org