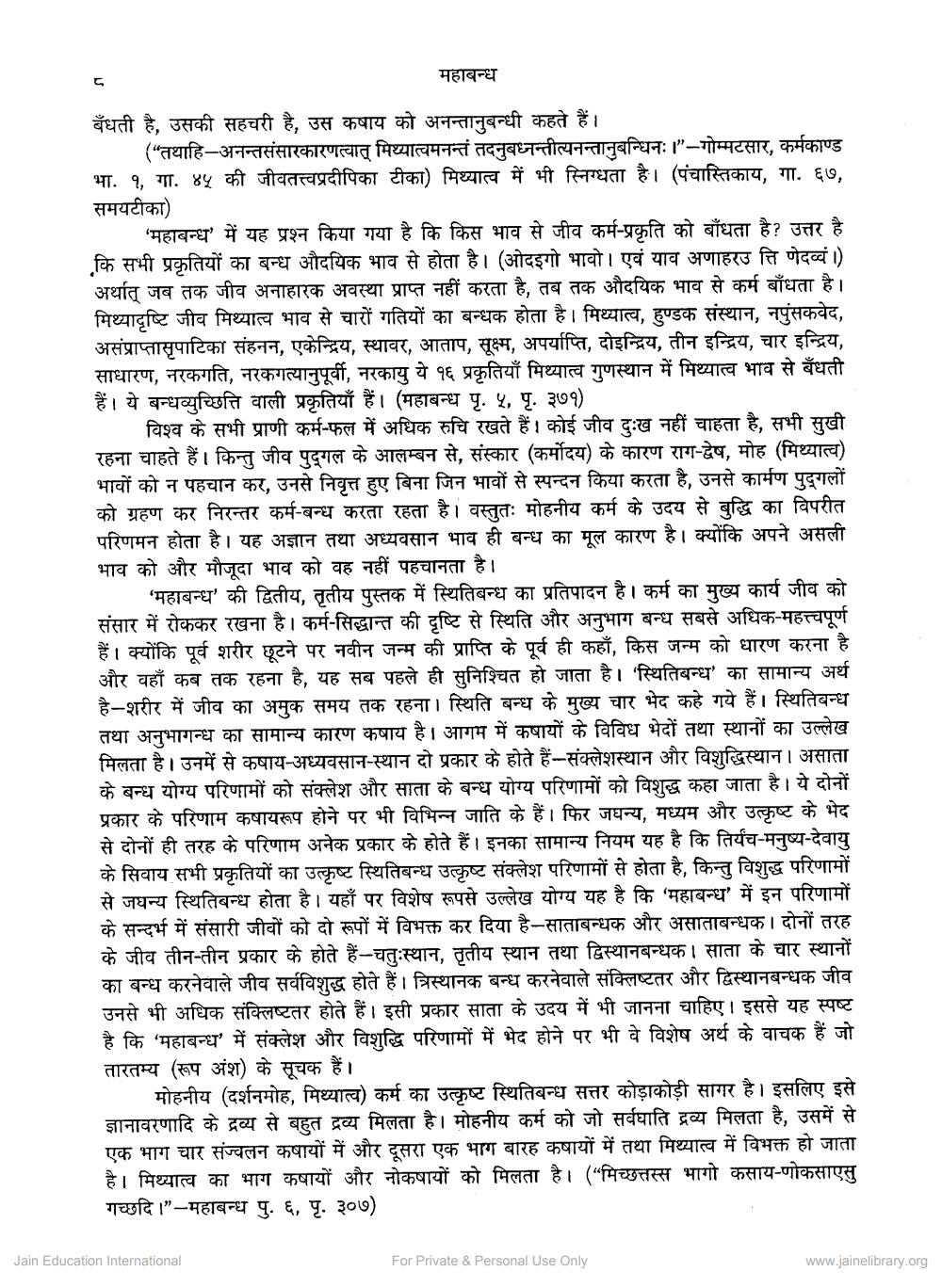________________
महाबन्ध
बँधती है, उसकी सहचरी है, उस कषाय को अनन्तानुबन्धी कहते हैं।
("तथाहि-अनन्तसंसारकारणत्वात् मिथ्यात्वमनन्तं तदनुबध्नन्तीत्यनन्तानुबन्धिनः।"-गोम्मटसार, कर्मकाण्ड भा. १, गा. ४५ की जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका) मिथ्यात्व में भी स्निग्धता है। (पंचास्तिकाय, गा. ६७, समयटीका)
'महाबन्ध' में यह प्रश्न किया गया है कि किस भाव से जीव कर्म-प्रकृति को बाँधता है? उत्तर है कि सभी प्रकृतियों का बन्ध औदयिक भाव से होता है। (ओदइगो भावो। एवं याव अणाहरउ त्ति णेदव्यं ।) अर्थात् जब तक जीव अनाहारक अवस्था प्राप्त नहीं करता है, तब तक औदयिक भाव से कर्म बाँधता है। मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व भाव से चारों गतियों का बन्धक होता है। मिथ्यात्व, हुण्डक संस्थान, नपुंसकवेद, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, साधारण, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु ये १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व भाव से बँधती हैं। ये बन्धव्युच्छित्ति वाली प्रकृतियाँ हैं। (महाबन्ध पृ. ५, पृ. ३७१)
विश्व के सभी प्राणी कर्म-फल में अधिक रुचि रखते हैं। कोई जीव दुःख नहीं चाहता है, सभी सुखी रहना चाहते हैं। किन्तु जीव पुद्गल के आलम्बन से, संस्कार (कर्मोदय) के कारण राग-द्वेष, मोह (मिथ्यात्व) भावों को न पहचान कर, उनसे निवृत्त हुए बिना जिन भावों से स्पन्दन किया करता है, उनसे कार्मण पुद्गलों को ग्रहण कर निरन्तर कर्म-बन्ध करता रहता है। वस्तुतः मोहनीय कर्म के उदय से बुद्धि का विपरीत परिणमन होता है। यह अज्ञान तथा अध्यवसान भाव ही बन्ध का मूल कारण है। क्योंकि अपने असली भाव को और मौजूदा भाव को वह नहीं पहचानता है।
'महाबन्ध' की द्वितीय, तृतीय पुस्तक में स्थितिबन्ध का प्रतिपादन है। कर्म का मुख्य कार्य जीव को संसार में रोककर रखना है। कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से स्थिति और अनुभाग बन्ध सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि पूर्व शरीर छूटने पर नवीन जन्म की प्राप्ति के पूर्व ही कहाँ, किस जन्म को धारण करना है
और वहाँ कब तक रहना है, यह सब पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। स्थितिबन्ध' का सामान्य अर्थ है-शरीर में जीव का अमुक समय तक रहना। स्थिति बन्ध के मुख्य चार भेद कहे गये हैं। स्थितिबन्ध तथा अनुभागन्ध का सामान्य कारण कषाय है। आगम में कषायों के विविध भेदों तथा स्थानों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कषाय-अध्यवसान-स्थान दो प्रकार के होते हैं-संक्लेशस्थान और विशुद्धिस्थान । असाता के बन्ध योग्य परिणामों को संक्लेश और साता के बन्ध योग्य परिणामों को विशुद्ध कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के परिणाम कषायरूप होने पर भी विभिन्न जाति के हैं। फिर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से दोनों ही तरह के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य नियम यह है कि तिर्यंच-मनुष्य-देवायु के सिवाय सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है, किन्तु विशुद्ध परिणामों से जघन्य स्थितिबन्ध होता है। यहाँ पर विशेष रूपसे उल्लेख योग्य यह है कि 'महाबन्ध' में इन परिणामों के सन्दर्भ में संसारी जीवों को दो रूपों में विभक्त कर दिया है-साताबन्धक और असाताबन्धक। दोनों तरह के जीव तीन-तीन प्रकार के होते हैं-चतुःस्थान, तृतीय स्थान तथा द्विस्थानबन्धक। साता के चार स्थानों का बन्ध करनेवाले जीव सर्वविशुद्ध होते हैं। त्रिस्थानक बन्ध करनेवाले संक्लिष्टतर और द्विस्थानबन्धक जीव उनसे भी अधिक संक्लिष्टतर होते हैं। इसी प्रकार साता के उदय में भी जानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि 'महाबन्ध' में संक्लेश और विशद्धि परिणामों में भेद होने पर भी वे विशेष अर्थ के वाचक हैं जो तारतम्य (रूप अंश) के सूचक हैं।
मोहनीय (दर्शनमोह, मिथ्यात्व) कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। इसलिए इसे ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है। मोहनीय कर्म को जो सर्वघाति द्रव्य मिलता है, उसमें से एक भाग चार संज्वलन कषायों में और दूसरा एक भाग बारह कषायों में तथा मिथ्यात्व में विभक्त हो जाता है। मिथ्यात्व का भाग कषायों और नोकषायों को मिलता है। (“मिच्छत्तस्स भागो कसाय-णोकसाएसु गच्छदि।"-महाबन्ध पु. ६, पृ. ३०७)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org