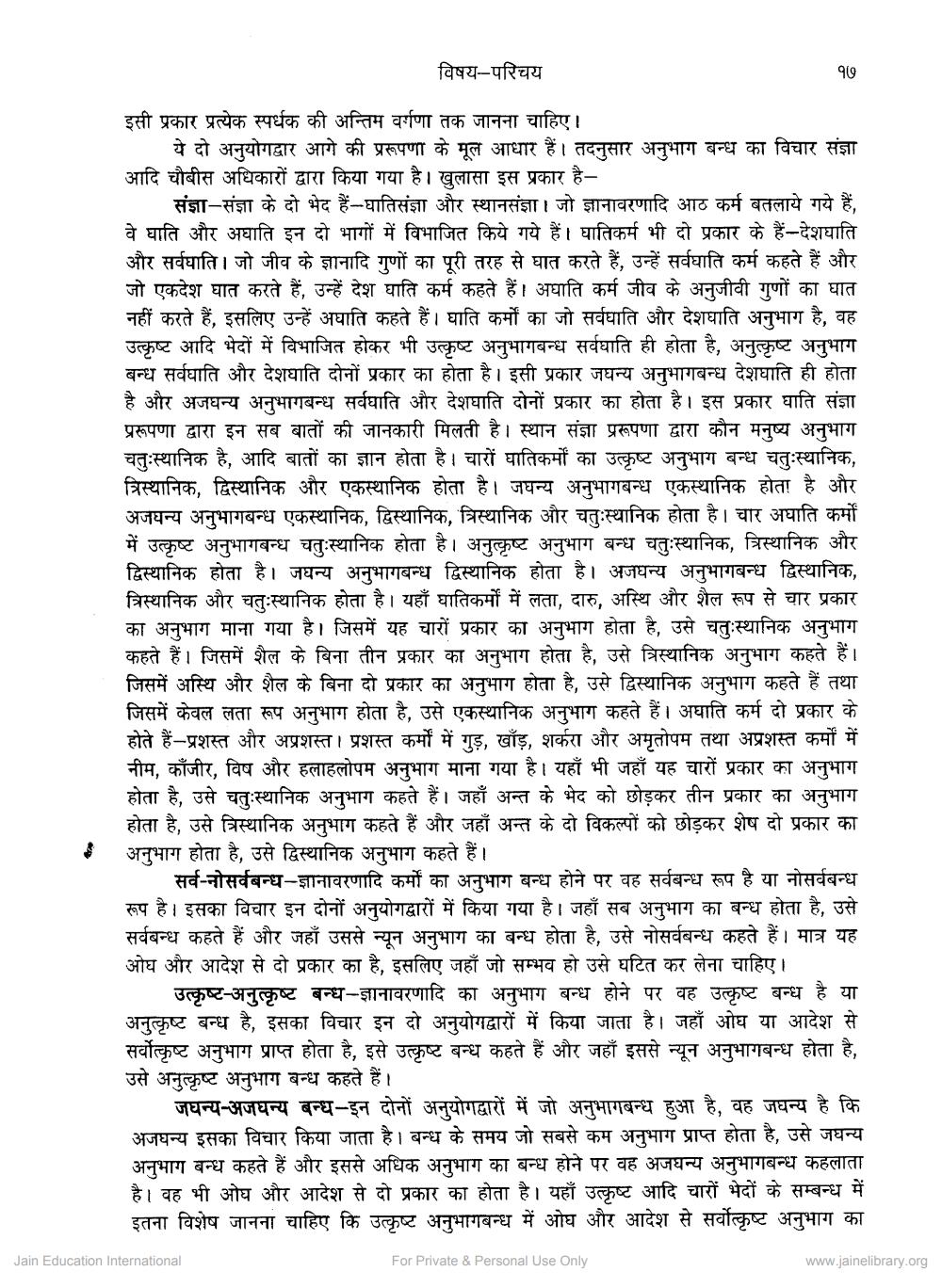________________
विषय-परिचय
१७
इसी प्रकार प्रत्येक स्पर्धक की अन्तिम वर्गणा तक जानना चाहिए।
ये दो अनुयोगद्वार आगे की प्ररूपणा के मूल आधार हैं। तदनुसार अनुभाग बन्ध का विचार संज्ञा आदि चौबीस अधिकारों द्वारा किया गया है। खुलासा इस प्रकार है
संज्ञा-संज्ञा के दो भेद हैं-घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा। जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म बतलाये गये हैं, वे घाति और अघाति इन दो भागों में विभाजित किये गये हैं। घातिकर्म भी दो प्रकार के हैं-देशघाति और सर्वघाति। जो जीव के ज्ञानादि गुणों का पूरी तरह से घात करते हैं, उन्हें सर्वघाति कर्म कहते हैं और जो एकदेश घात करते हैं, उन्हें देश घाति कर्म कहते हैं। अघाति कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अघाति कहते हैं। घाति कर्मों का जो सर्वघाति और देशघाति अनुभाग है, वह उत्कृष्ट आदि भेदों में विभाजित होकर भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति ही होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध सर्वघाति और देशघाति दोनों प्रकार का होता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभागबन्ध देशघाति ही होता है और अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वघाति और देशघाति दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार घाति संज्ञा प्ररूपणा द्वारा इन सब बातों की जानकारी मिलती है। स्थान संज्ञा प्ररूपणा द्वारा कौन मनुष्य अनुभाग चतुःस्थानिक है, आदि बातों का ज्ञान होता है। चारों घातिकर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध चतःस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एकस्थानिक होता है। जघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक होता है और अजघन्य अनुभागबन्ध एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। चार अघाति कर्मों में उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुःस्थानिक होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक होता है। जघन्य अनुभागबन्ध विस्थानिक होता है। अजघन्य अनुभागबन्ध विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। यहाँ घातिकर्मों में लता, दारु, अस्थि और शैल रूप से चार प्रकार का अनुभाग माना गया है। जिसमें यह चारों प्रकार का अनुभाग होता है, उसे चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें शैल के बिना तीन प्रकार का अनुभाग होता है, उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें अस्थि और शैल के बिना दो प्रकार का अनुभाग होता है, उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा जिसमें केवल लता रूप अनुभाग होता है, उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं। अघाति कर्म दो प्रकार के होते हैं-प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त कर्मों में गुड़, खाँड़, शर्करा और अमृतोपम तथा अप्रशस्त कर्मों में नीम, काँजीर, विष और हलाहलोपम अनुभाग माना गया है। यहाँ भी जहाँ यह चारों प्रकार का अनुभाग होता है, उसे चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जहाँ अन्त के भेद को छोड़कर तीन प्रकार का अनुभाग होता है, उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं और जहाँ अन्त के दो विकल्पों को छोड़कर शेष दो प्रकार का अनुभाग होता है, उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं।
सर्व-नोसर्वबन्ध-ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग बन्ध होने पर वह सर्वबन्ध रूप है या नोसर्वबन्ध रूप है। इसका विचार इन दोनों अनुयोगद्वारों में किया गया है। जहाँ सब अनुभाग का बन्ध होता है, उसे सर्वबन्ध कहते हैं और जहाँ उससे न्यून अनुभाग का बन्ध होता है, उसे नोसर्वबन्ध कहते हैं। मात्र यह ओघ और आदेश से दो प्रकार का है, इसलिए जहाँ जो सम्भव हो उसे घटित कर लेना चाहिए।
उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट बन्ध-ज्ञानावरणादि का अनुभाग बन्ध होने पर वह उत्कृष्ट बन्ध है या अनुत्कृष्ट बन्ध है, इसका विचार इन दो अनुयोगद्वारों में किया जाता है। जहाँ ओघ या आदेश से सर्वोत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है, इसे उत्कृष्ट बन्ध कहते हैं और जहाँ इससे न्यून अनुभागबन्ध होता है, उसे अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध कहते हैं।
जघन्य-अजघन्य बन्ध-इन दोनों अनुयोगद्वारों में जो अनुभागबन्ध हुआ है, वह जघन्य है कि अजघन्य इसका विचार किया जाता है। बन्ध के समय जो सबसे कम अनुभाग प्राप्त होता है, उसे जघन्य अनुभाग बन्ध कहते हैं और इससे अधिक अनुभाग का बन्ध होने पर वह अजघन्य अनुभागबन्ध कहलाता है। वह भी ओघ और आदेश से दो प्रकार का होता है। यहाँ उत्कृष्ट आदि चारों भेदों के सम्बन्ध में इतना विशेष जानना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुभागबन्ध में ओघ और आदेश से सर्वोत्कृष्ट अनुभाग का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org