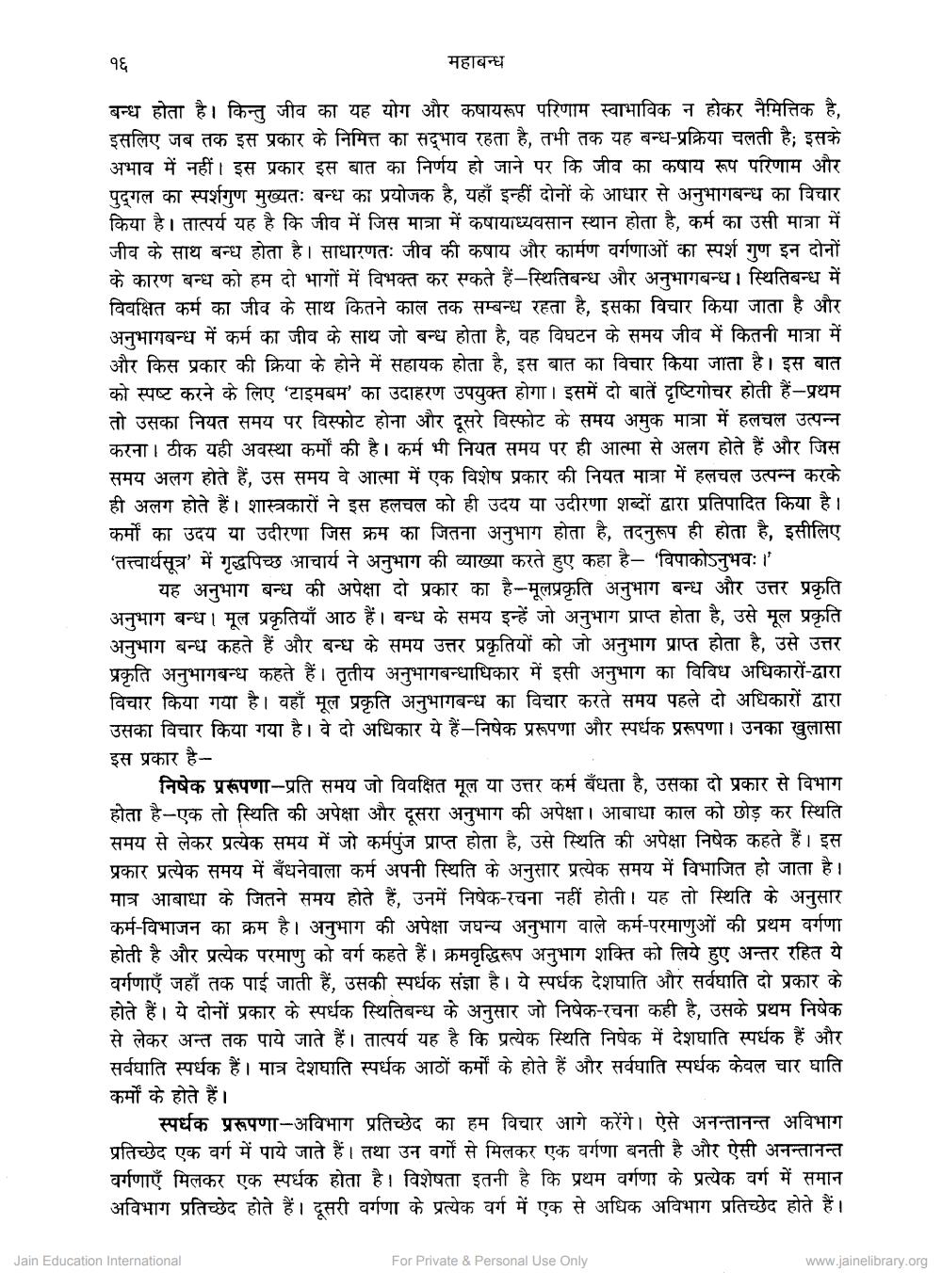________________
१६
महाबन्ध
बन्ध होता है। किन्तु जीव का यह योग और कषायरूप परिणाम स्वाभाविक न होकर नैमित्तिक है, इसलिए जब तक इस प्रकार के निमित्त का सद्भाव रहता है, तभी तक यह बन्ध-प्रक्रिया चलती है; इसके अभाव में नहीं। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो जाने पर कि जीव का कषाय रूप परिणाम और पुद्गल का स्पर्शगुण मुख्यतः बन्ध का प्रयोजक है, यहाँ इन्हीं दोनों के आधार से अनुभागबन्ध का विचार किया है। तात्पर्य यह है कि जीव में जिस मात्रा में कषायाध्यवसान स्थान होता है, कर्म का उसी मात्रा में जीव के साथ बन्ध होता है। साधारणतः जीव की कषाय और कार्मण वर्गणाओं का स्पर्श गुण इन दोनों के कारण बन्ध को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । स्थितिबन्ध में विवक्षित कर्म का जीव के साथ कितने काल तक सम्बन्ध रहता है, इसका विचार किया जाता है और अनुभागबन्ध में कर्म का जीव के साथ जो बन्ध होता है, वह विघटन के समय जीव में कितनी मात्रा में और किस प्रकार की क्रिया के होने में सहायक होता है, इस बात का विचार किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'टाइमबम' का उदाहरण उपयुक्त होगा। इसमें दो बातें दृष्टिगोचर होती हैं-प्रथम तो उसका नियत समय पर विस्फोट होना और दूसरे विस्फोट के समय अमुक मात्रा में हलचल उत्पन्न करना। ठीक यही अवस्था कर्मों की है। कर्म भी नियत समय पर ही आत्मा से अलग होते हैं और जिस समय अलग होते हैं, उस समय वे आत्मा में एक विशेष प्रकार की नियत मात्रा में हलचल उत्पन्न करके ही अलग होते हैं। शास्त्रकारों ने इस हलचल को ही उदय या उदीरणा शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है। कर्मों का उदय या उदीरणा जिस क्रम का जितना अनुभाग होता है, तदनुरूप ही होता है, इसीलिए 'तत्त्वार्थसूत्र' में गृद्धपिच्छ आचार्य ने अनुभाग की व्याख्या करते हुए कहा है- 'विपाकोऽनुभवः।"
यह अनुभाग बन्ध की अपेक्षा दो प्रकार का है-मूलप्रकृति अनुभाग बन्ध और उत्तर प्रकृति अनुभाग बन्ध । मूल प्रकृतियाँ आठ हैं। बन्ध के समय इन्हें जो अनुभाग प्राप्त होता है, उसे मूल प्रकृति अनुभाग बन्ध कहते हैं और बन्ध के समय उत्तर प्रकृतियों को जो अनुभाग प्राप्त होता है, उसे उत्तर प्रकृति अनभागबन्ध कहते हैं। तृतीय अनुभागबन्धाधिकार में इसी अनुभाग का विविध अधिकारों-द्वारा विचार किया गया है। वहाँ मूल प्रकृति अनुभागबन्ध का विचार करते समय पहले दो अधिकारों द्वारा उसका विचार किया गया है। वे दो अधिकार ये हैं-निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा। उनका खुलासा इस प्रकार है
निषेक प्ररूपणा-प्रति समय जो विवक्षित मूल या उत्तर कर्म बँधता है, उसका दो प्रकार से विभाग होता है-एक तो स्थिति की अपेक्षा और दूसरा अनुभाग की अपेक्षा। आबाधा काल को छोड़ कर स्थिति समय से लेकर प्रत्येक समय में जो कर्मपुंज प्राप्त होता है, उसे स्थिति की अपेक्षा निषेक कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समय में बँधनेवाला कर्म अपनी स्थिति के अनुसार प्रत्येक समय में विभाजित हो जाता है। मात्र आबाधा के जितने समय होते हैं, उनमें निषेक-रचना नहीं होती। यह तो स्थिति के अनुसार कर्म-विभाजन का क्रम है। अनुभाग की अपेक्षा जघन्य अनुभाग वाले कर्म-परमाणुओं की प्रथम वर्गणा होती है और प्रत्येक परमाण को वर्ग कहते हैं। क्रमवृद्धिरूप अनुभाग शक्ति को लिये हुए अन्तर रहित ये वर्गणाएँ जहाँ तक पाई जाती हैं, उसकी स्पर्धक संज्ञा है। ये स्पर्धक देशघाति और सर्वघाति दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों प्रकार के स्पर्धक स्थितिबन्ध के अनुसार जो निषेक-रचना कही है, उसके प्रथम निषेक से लेकर अन्त तक पाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थिति निषेक में देशघाति स्पर्धक हैं और सर्वघाति स्पर्धक हैं। मात्र देशघाति स्पर्धक आठों कर्मों के होते हैं और सर्वघाति स्पर्धक केवल चार घाति कर्मों के होते हैं।
स्पर्धक प्ररूपणा-अविभाग प्रतिच्छेद का हम विचार आगे करेंगे। ऐसे अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद एक वर्ग में पाये जाते हैं। तथा उन वर्गों से मिलकर एक वर्गणा बनती है और ऐसी अनन्तानन्त वर्गणाएँ मिलकर एक स्पर्धक होता है। विशेषता इतनी है कि प्रथम वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। दूसरी वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में एक से अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org