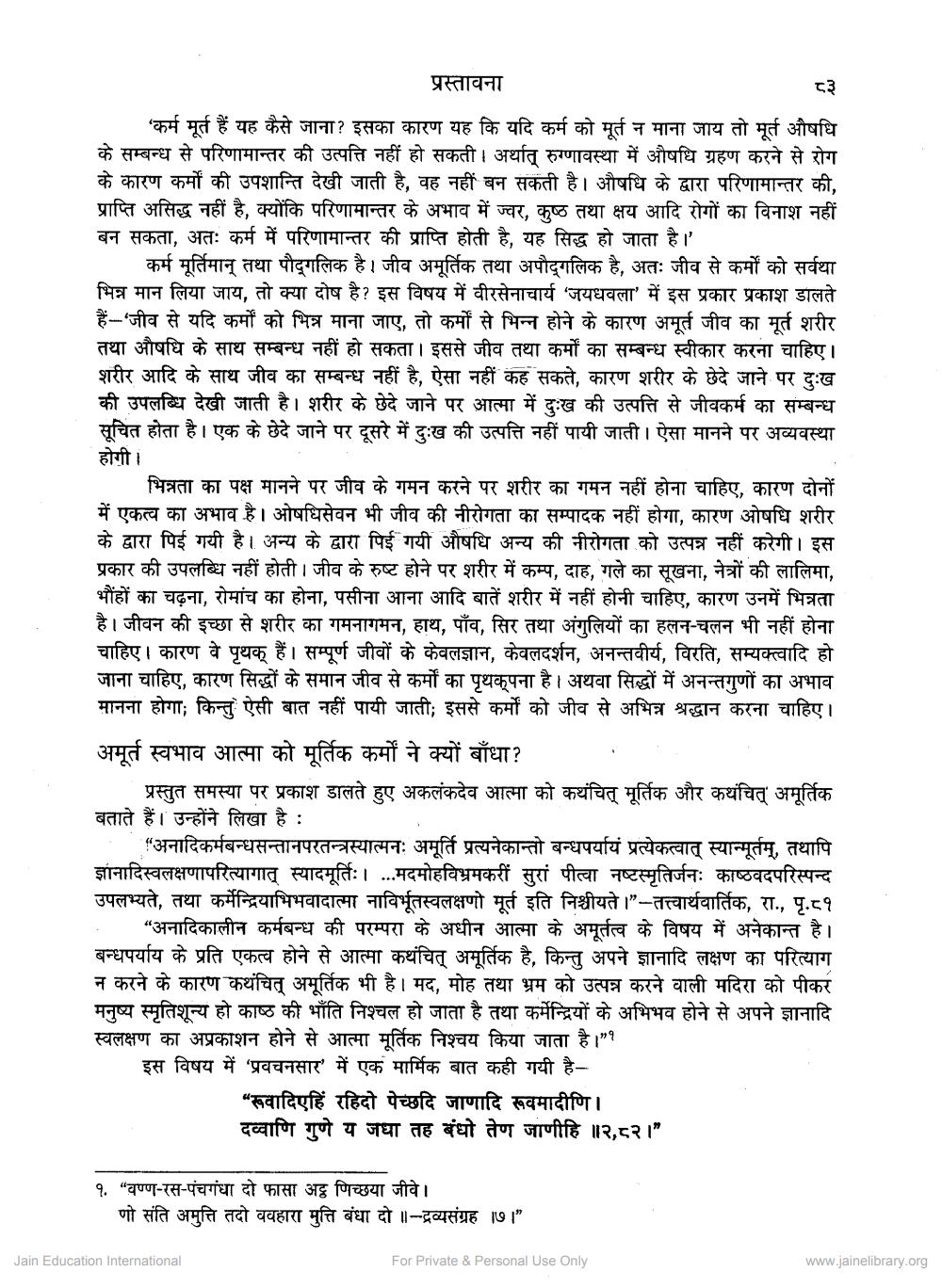________________
प्रस्तावना
८३ 'कर्म मूर्त हैं यह कैसे जाना? इसका कारण यह कि यदि कर्म को मूर्त न माना जाय तो मूर्त औषधि के सम्बन्ध से परिणामान्तर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् रुग्णावस्था में औषधि ग्रहण करने से रोग के कारण कर्मों की उपशान्ति देखी जाती है, वह नहीं बन सकती है। औषधि के द्वारा परिणामान्तर की, प्राप्ति असिद्ध नहीं है, क्योंकि परिणामान्तर के अभाव में ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय आदि रोगों का विनाश नहीं बन सकता, अतः कर्म में परिणामान्तर की प्राप्ति होती है, यह सिद्ध हो जाता है।' ।
कर्म मूर्तिमान् तथा पौद्गलिक है। जीव अमूर्तिक तथा अपौद्गलिक है, अतः जीव से कर्मों को सर्वथा भिन्न मान लिया जाय, तो क्या दोष है? इस विषय में वीरसेनाचार्य 'जयधवला' में इस प्रकार प्रकाश डालते हैं- 'जीव से यदि कर्मों को भिन्न माना जाए, तो कर्मों से भिन्न होने के कारण अमूर्त जीव का मूर्त शरीर तथा औषधि के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे जीव तथा कर्मों का सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिए। शरीर आदि के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कारण शरीर के छेदे जाने पर दुःख की उपलब्धि देखी जाती है। शरीर के छेदे जाने पर आत्मा में दुःख की उत्पत्ति से जीवकर्म का सम्बन्ध सूचित होता है। एक के छेदे जाने पर दूसरे में दुःख की उत्पत्ति नहीं पायी जाती। ऐसा मानने पर अव्यवस्था होगी।
भिन्नता का पक्ष मानने पर जीव के गमन करने पर शरीर का गमन नहीं होना चाहिए, कारण दोनों में एकत्व का अभाव है। ओषधिसेवन भी जीव की नीरोगता का सम्पादक नहीं होगा, कारण ओषधि शरीर के द्वारा पिई गयी है। अन्य के द्वारा पिई गयी औषधि अन्य की नीरोगता को उत्पन्न नहीं करेगी। इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होती। जीव के रुष्ट होने पर शरीर में कम्प, दाह, गले का सूखना, नेत्रों की लालिमा, भौंहों का चढ़ना, रोमांच का होना, पसीना आना आदि बातें शरीर में नहीं होनी चाहिए, कारण उनमें भिन्नता है। जीवन की इच्छा से शरीर का गमनागमन, हाथ, पाँव, सिर तथा अंगुलियों का हलन-चलन भी नहीं होना चाहिए। कारण वे पृथक् हैं। सम्पूर्ण जीवों के केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति, सम्यक्त्वादि हो जाना चाहिए, कारण सिद्धों के समान जीव से कर्मों का पृथक्पना है। अथवा सिद्धों में अनन्तगुणों का अभाव मानना होगा; किन्तु ऐसी बात नहीं पायी जाती; इससे कर्मों को जीव से अभिन्न श्रद्धान करना चाहिए। अमूर्त स्वभाव आत्मा को मूर्तिक कर्मों ने क्यों बाँधा?
प्रस्तुत समस्या पर प्रकाश डालते हुए अकलंकदेव आत्मा को कथंचित् मूर्तिक और कथंचित् अमूर्तिक बताते हैं। उन्होंने लिखा है :
"अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमूर्ति प्रत्यनेकान्तो बन्धपर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्तम्, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्तिः। ...मदमोहविभ्रमकरी सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा कर्मेन्द्रियाभिभवादात्मा नाविभूतस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।"-तत्त्वार्थवार्तिक, रा., पृ.८१
___ “अनादिकालीन कर्मबन्ध की परम्परा के अधीन आत्मा के अमूर्तत्व के विषय में अनेकान्त है। बन्धपर्याय के प्रति एकत्व होने से आत्मा कथंचित् अमूर्तिक है, किन्तु अपने ज्ञानादि लक्षण का परित्याग न करने के कारण कथंचित् अमूर्तिक भी है। मद, मोह तथा भ्रम को उत्पन्न करने वाली मदिरा को पीकर मनुष्य स्मृतिशून्य हो काष्ठ की भाँति निश्चल हो जाता है तथा कर्मेन्द्रियों के अभिभव होने से अपने ज्ञानादि स्वलक्षण का अप्रकाशन होने से आत्मा मूर्तिक निश्चय किया जाता है।"१ इस विषय में 'प्रवचनसार' में एक मार्मिक बात कही गयी है
__ "रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि।
दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥२,८२।"
१. “वण्ण-रस-पंचगंधा दो फासा अट्ठ णिच्छया जीवे।
णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥-द्रव्यसंग्रह ७।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org