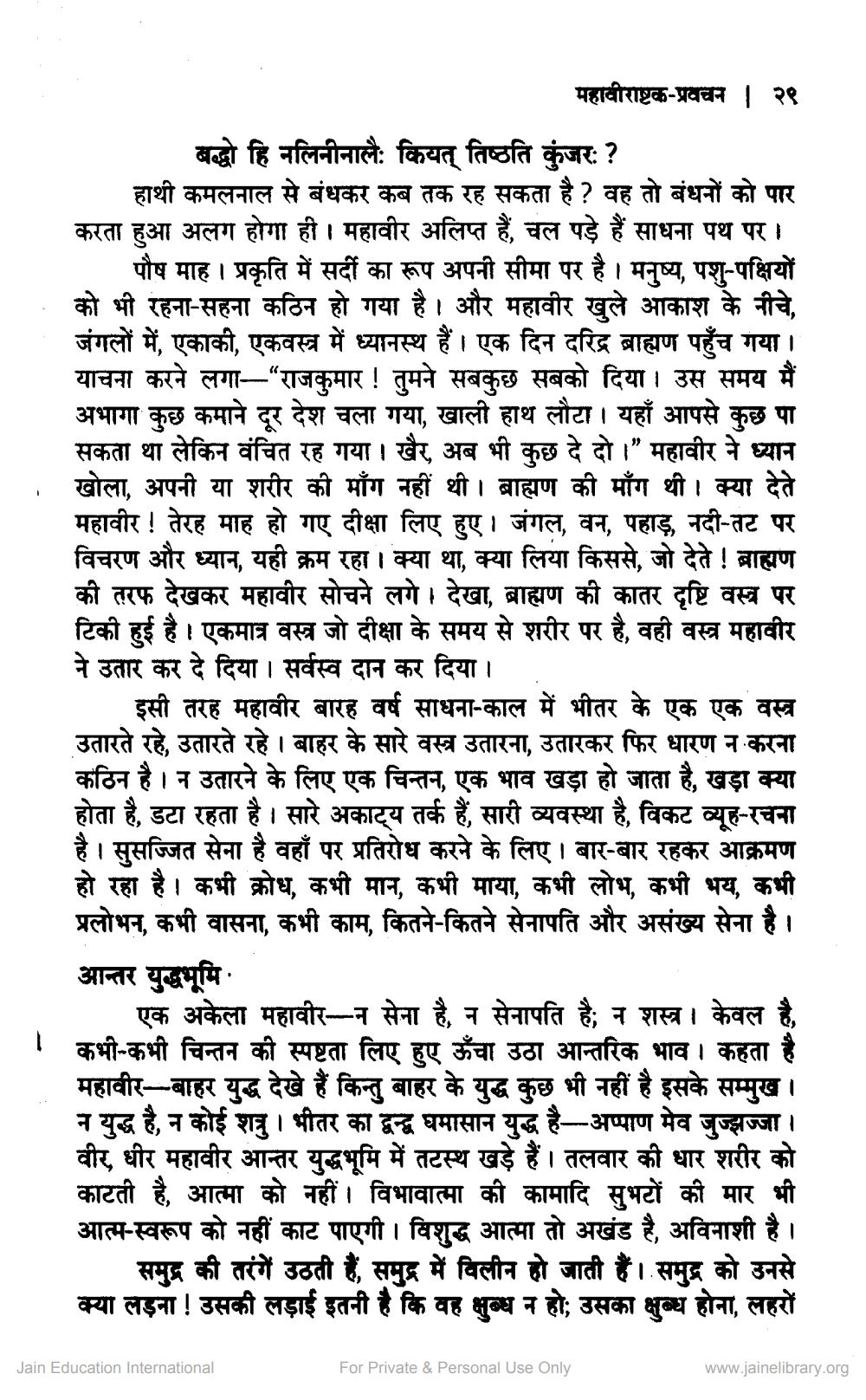________________
महावीराष्टक-प्रवचन | २९ बद्धो हि नलिनीनालैः कियत् तिष्ठति कुंजर: ? हाथी कमलनाल से बंधकर कब तक रह सकता है? वह तो बंधनों को पार करता हुआ अलग होगा ही। महावीर अलिप्त हैं, चल पड़े हैं साधना पथ पर।
पौष माह । प्रकृति में सर्दी का रूप अपनी सीमा पर है। मनुष्य, पशु-पक्षियों को भी रहना-सहना कठिन हो गया है। और महावीर खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, एकाकी, एकवस्त्र में ध्यानस्थ हैं। एक दिन दरिद्र ब्राह्मण पहुँच गया। याचना करने लगा-"राजकुमार ! तुमने सबकुछ सबको दिया। उस समय मैं अभागा कुछ कमाने दूर देश चला गया, खाली हाथ लौटा । यहाँ आपसे कुछ पा सकता था लेकिन वंचित रह गया। खैर, अब भी कुछ दे दो।" महावीर ने ध्यान खोला, अपनी या शरीर की माँग नहीं थी। ब्राह्मण की माँग थी। क्या देते महावीर ! तेरह माह हो गए दीक्षा लिए हुए। जंगल, वन, पहाड़, नदी-तट पर विचरण और ध्यान, यही क्रम रहा। क्या था, क्या लिया किससे, जो देते ! ब्राह्मण की तरफ देखकर महावीर सोचने लगे। देखा, ब्राह्मण की कातर दृष्टि वस्त्र पर टिकी हई है। एकमात्र वस्त्र जो दीक्षा के समय से शरीर पर है, वही वस्त्र महावीर ने उतार कर दे दिया। सर्वस्व दान कर दिया।
इसी तरह महावीर बारह वर्ष साधना-काल में भीतर के एक एक वस्त्र उतारते रहे, उतारते रहे। बाहर के सारे वस्त्र उतारना, उतारकर फिर धारण न करना कठिन है। न उतारने के लिए एक चिन्तन, एक भाव खड़ा हो जाता है, खड़ा क्या होता है, डटा रहता है। सारे अकाट्य तर्क हैं, सारी व्यवस्था है, विकट व्यूह-रचना है । सुसज्जित सेना है वहाँ पर प्रतिरोध करने के लिए। बार-बार रहकर आक्रमण हो रहा है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी भय, कभी प्रलोभन, कभी वासना, कभी काम, कितने-कितने सेनापति और असंख्य सेना है। आन्तर युद्धभूमि
एक अकेला महावीर-न सेना है, न सेनापति है; न शस्त्र । केवल है, कभी-कभी चिन्तन की स्पष्टता लिए हुए ऊँचा उठा आन्तरिक भाव। कहता है महावीर-बाहर युद्ध देखे हैं किन्तु बाहर के युद्ध कुछ भी नहीं है इसके सम्मुख । न युद्ध है, न कोई शत्र । भीतर का द्वन्द्व घमासान युद्ध है-अप्याण मेव जुज्झज्जा। वीर, धीर महावीर आन्तर युद्धभूमि में तटस्थ खड़े हैं। तलवार की धार शरीर को काटती है, आत्मा को नहीं। विभावात्मा की कामादि सुभटों की मार भी आत्म-स्वरूप को नहीं काट पाएगी। विशुद्ध आत्मा तो अखंड है, अविनाशी है।
समुद्र की तरंगें उठती है, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। समुद्र को उनसे क्या लड़ना ! उसकी लड़ाई इतनी है कि वह क्षुब्ध न हो; उसका क्षुब्ध होना, लहरों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org