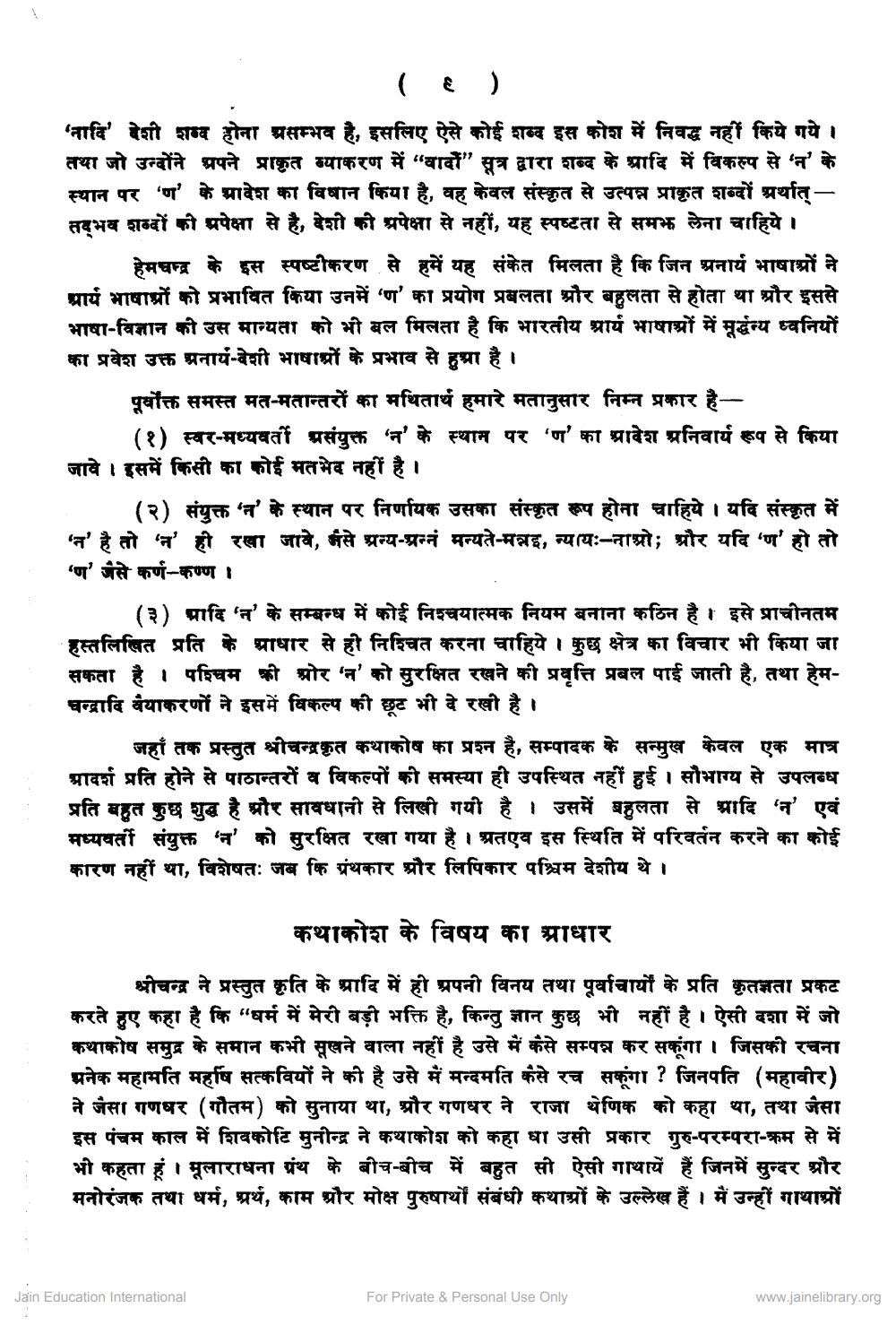________________
'नादि' देशी शब्द होना असम्भव है, इसलिए ऐसे कोई शब्द इस कोश में निवद्ध नहीं किये गये। तथा जो उन्दोंने अपने प्राकृत व्याकरण में "वादों" सूत्र द्वारा शब्द के प्रादि में विकल्प से 'न' के स्थान पर 'ण' के आदेश का विधान किया है, वह केवल संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत शब्दों अर्थात्सद्भव शब्दों को अपेक्षा से है, देशी को अपेक्षा से नहीं, यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिये।
हेमचन्द्र के इस स्पष्टीकरण से हमें यह संकेत मिलता है कि जिन अनार्य भाषाओं ने आर्य भाषाओं को प्रभावित किया उनमें 'ण' का प्रयोग प्रबलता और बहुलता से होता था और इससे भाषा-विज्ञान को उस मान्यता को भी बल मिलता है कि भारतीय आर्य भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रवेश उक्त अनार्य-वेशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है।
पूर्वोक्त समस्त मत-मतान्तरों का मथितार्थ हमारे मतानुसार निम्न प्रकार है
(१) स्वर-मध्यवर्ती प्रसंयुक्त 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रादेश अनिवार्य रूप से किया जावे । इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है।
(२) संयुक्त 'न' के स्थान पर निर्णायक उसका संस्कृत रूप होना चाहिये । यदि संस्कृत में 'न' है तो 'न' ही रखा जावे, असे अन्य-अन्नं मन्यते-मन्नाइ, न्यायः-नाओ; और यदि 'ण' हो तो 'ण' जैसे कर्ण-कण्ण ।
(३) प्रावि 'न' के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक नियम बनाना कठिन है। इसे प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति के प्राधार से ही निश्चित करना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भी किया जा सकता है। पश्चिम की ओर 'न' को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हेमचन्द्रादि वैयाकरणों ने इसमें विकल्प की छूट भी दे रखी है।
जहाँ तक प्रस्तुत श्रीचन्द्रकृत कथाकोष का प्रश्न है, सम्पादक के सन्मुख केवल एक मात्र आदर्श प्रति होने से पाठान्तरों व विकल्पों की समस्या ही उपस्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध प्रति बहुत कुछ शुद्ध है और सावधानी से लिखी गयी है । उसमें बहुलता से प्रादि 'न' एवं मध्यवर्ती संयुक्त 'न' को सुरक्षित रखा गया है । अतएव इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं था, विशेषतः जब कि ग्रंथकार और लिपिकार पश्चिम देशीय थे।
कथाकोश के विषय का प्राधार
श्रीचन्द्र ने प्रस्तुत कृति के प्रादि में ही अपनी विनय तथा पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा है कि "धर्म में मेरी बड़ी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहीं है । ऐसी दशा में जो कथाकोष समुद्र के समान कभी सूखने वाला नहीं है उसे मैं कैसे सम्पन्न कर सकूँगा। जिसकी रचना अनेक महामति महर्षि सत्कवियों ने की है उसे मैं मन्दमति कैसे रच सकूगा ? जिनपति (महावीर) ने जैसा गणषर (गौतम) को सुनाया था, और गणधर ने राजा थेणिक को कहा था, तथा जैसा इस पंचम काल में शिवकोटि मुनीन्द्र ने कथाकोश को कहा था उसी प्रकार गुरु-परम्परा-क्रम से में भी कहता हूं। मूलाराधना ग्रंथ के बीच-बीच में बहुत सी ऐसी गाथायें हैं जिनमें सुन्दर और मनोरंजक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों संबंधी कथाओं के उल्लेख हैं । मैं उन्हीं गाथाओं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org