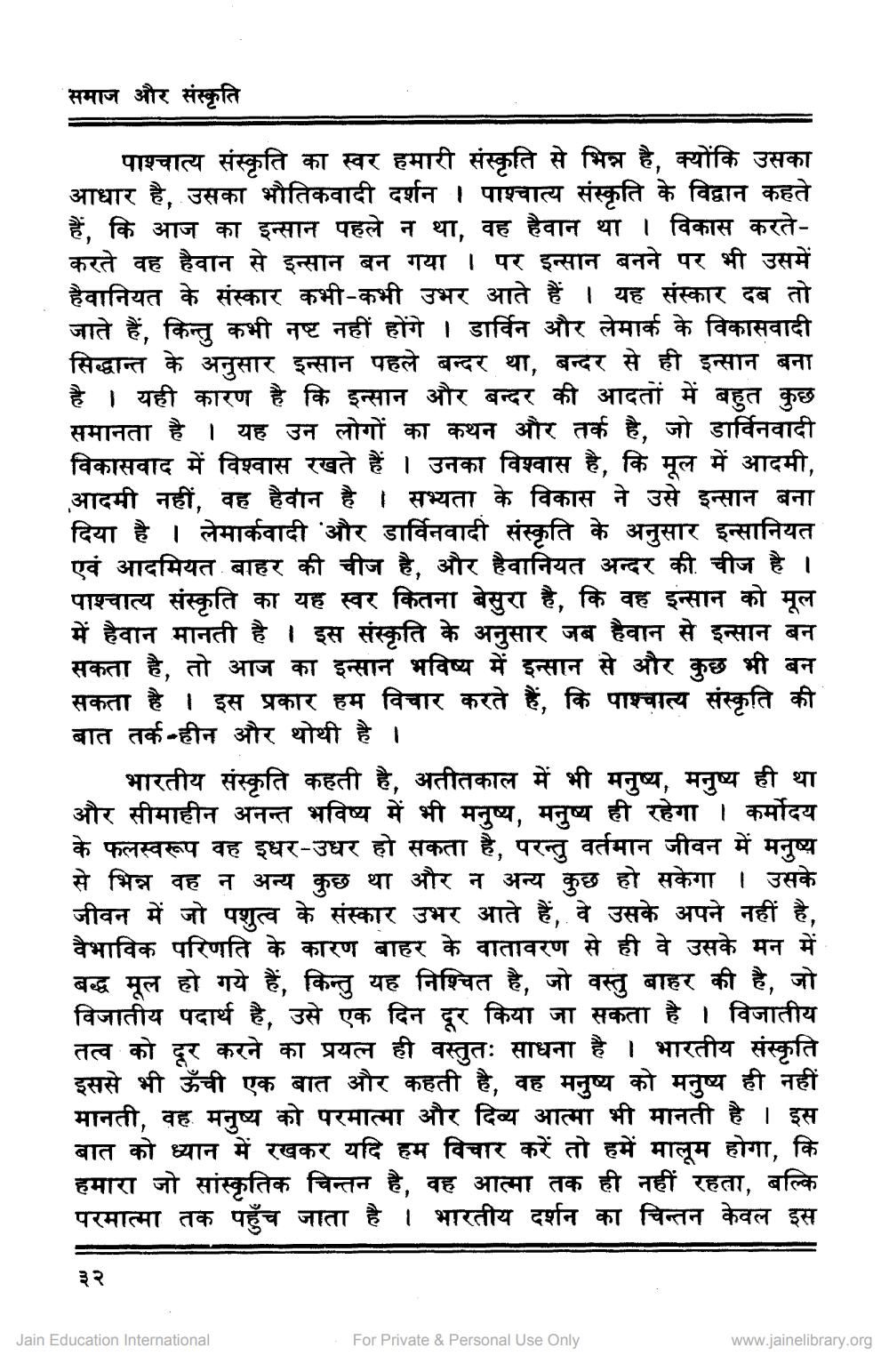________________
समाज और संस्कृति
पाश्चात्य संस्कृति का स्वर हमारी संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि उसका आधार है, उसका भौतिकवादी दर्शन । पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान कहते हैं, कि आज का इन्सान पहले न था, वह हैवान था । विकास करतेकरते वह हैवान से इन्सान बन गया । पर इन्सान बनने पर भी उसमें हैवानियत के संस्कार कभी-कभी उभर आते हैं । यह संस्कार दब तो जाते हैं, किन्तु कभी नष्ट नहीं होंगे । डार्विन और लेमार्क के विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार इन्सान पहले बन्दर था, बन्दर से ही इन्सान बना है । यही कारण है कि इन्सान और बन्दर की आदतों में बहुत कुछ समानता है । यह उन लोगों का कथन और तर्क है, जो डार्विनवादी विकासवाद में विश्वास रखते हैं । उनका विश्वास है, कि मूल में आदमी, आदमी नहीं, वह हैवान है । सभ्यता के विकास ने उसे इन्सान बना दिया है । लेमार्कवादी और डार्विनवादी संस्कृति के अनुसार इन्सानियत एवं आदमियत बाहर की चीज है, और हैवानियत अन्दर की चीज है । पाश्चात्य संस्कृति का यह स्वर कितना बेसुरा है, कि वह इन्सान को मूल में हैवान मानती है । इस संस्कृति के अनुसार जब हैवान से इन्सान बन सकता है, तो आज का इन्सान भविष्य में इन्सान से और कुछ भी बन सकता है । इस प्रकार हम विचार करते हैं, कि पाश्चात्य संस्कृति की बात तर्क-हीन और थोथी है ।
भारतीय संस्कृति कहती है, अतीतकाल में भी मनुष्य, मनुष्य ही था और सीमाहीन अनन्त भविष्य में भी मनुष्य, मनुष्य ही रहेगा । कर्मोदय के फलस्वरूप वह इधर-उधर हो सकता है, परन्तु वर्तमान जीवन में मनुष्य से भिन्न वह न अन्य कुछ था और न अन्य कुछ हो सकेगा । उसके जीवन में जो पशुत्व के संस्कार उभर आते हैं, वे उसके अपने नहीं है, वैभाविक परिणति के कारण बाहर के वातावरण से ही वे उसके मन में बद्ध मूल हो गये हैं, किन्तु यह निश्चित है, जो वस्तु बाहर की है, जो विजातीय पदार्थ है, उसे एक दिन दूर किया जा सकता है । विजातीय तत्व को दूर करने का प्रयत्न ही वस्तुतः साधना है । भारतीय संस्कृति इससे भी ऊँची एक बात और कहती है, वह मनुष्य को मनुष्य ही नहीं मानती, वह मनुष्य को परमात्मा और दिव्य आत्मा भी मानती है । इस बात को ध्यान में रखकर यदि हम विचार करें तो हमें मालूम होगा, कि हमारा जो सांस्कृतिक चिन्तन है, वह आत्मा तक ही नहीं रहता, बल्कि परमात्मा तक पहुँच जाता है । भारतीय दर्शन का चिन्तन केवल इस
३२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org