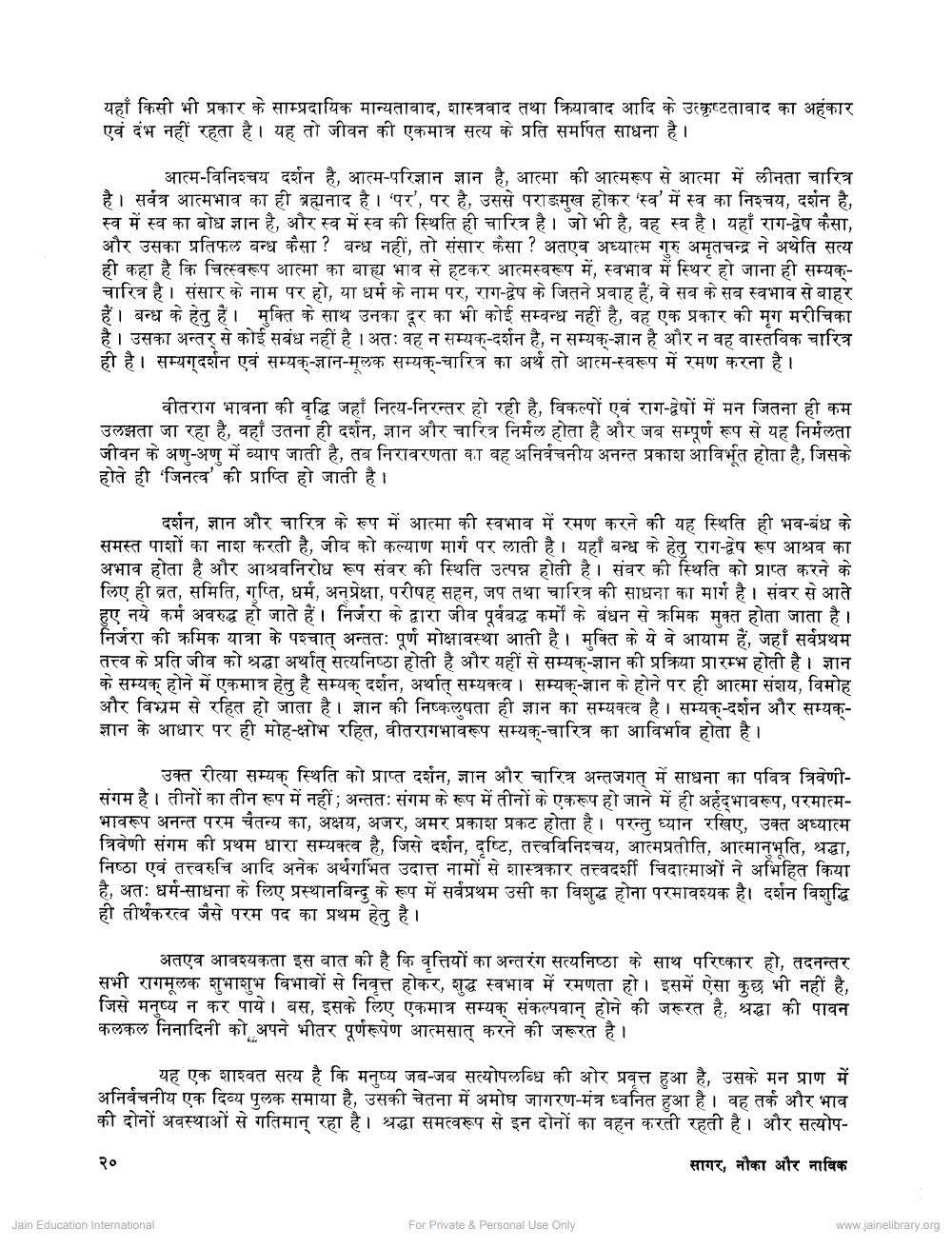________________
यहाँ किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक मान्यतावाद, शास्त्रवाद तथा क्रियावाद आदि के उत्कृष्टतावाद का अहंकार एवं दंभ नहीं रहता है। यह तो जीवन की एकमात्र सत्य के प्रति समर्पित साधना है।
आत्म-विनिश्चय दर्शन है, आत्म-परिज्ञान ज्ञान है, आत्मा की आत्मरूप से आत्मा में लीनता चारित्र है। सर्वत्र आत्मभाव का ही ब्रह्मनाद है। 'पर', पर है, उससे पराङमुख होकर 'स्व' में स्व का निश्चय, दर्शन है, स्व में स्व का बोध ज्ञान है, और स्व में स्व की स्थिति ही चारित्र है। जो भी है, वह स्व है। यहाँ राग-द्वेष कैसा, और उसका प्रतिफल बन्ध कैसा? बन्ध नहीं, तो संसार कैसा? अतएव अध्यात्म गुरु अमृतचन्द्र ने अथेति सत्य ही कहा है कि चित्स्वरूप आत्मा का बाह्य भाव से हटकर आत्मस्वरूप में, स्वभाव में स्थिर हो जाना ही सम्यकचारित्र है। संसार के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर, राग-द्वेष के जितने प्रवाह हैं, वे सब के सब स्वभाव से बाहर हैं। बन्ध के हेतु हैं। मुक्ति के साथ उनका दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है, वह एक प्रकार की मृग मरीचिका है। उसका अन्तर् से कोई सबंध नहीं है । अतः वह न सम्यक्-दर्शन है, न सम्यक्-ज्ञान है और न वह वास्तविक चारित्र ही है। सम्यग्दर्शन एवं सम्यक्-ज्ञान-मूलक सम्यक्-चारित्र का अर्थ तो आत्म-स्वरूप में रमण करना है।
हैं। बन्ध के हेतु
नहीं है । अतः वह न स
का अर्थ तो आत्म
वीतराग भावना की वृद्धि जहाँ नित्य-निरन्तर हो रही है, विकल्पों एवं राग-द्वेषों में मन जितना ही कम उलझता जा रहा है, वहाँ उतना ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र निर्मल होता है और जब सम्पूर्ण रूप से यह निर्मलता जीवन के अणु-अणु में व्याप जाती है, तब निरावरणता का वह अनिर्वचनीय अनन्त प्रकाश आविर्भूत होता है, जिसके होते ही 'जिनत्व' की प्राप्ति हो जाती है।
दर्शन, ज्ञान और चारित्र के रूप में आत्मा की स्वभाव में रमण करने की यह स्थिति ही भव-बंध के समस्त पाशों का नाश करती है, जीव को कल्याण मार्ग पर लाती है। यहाँ बन्ध के हेतु राग-द्वेष रूप आश्रव का अभाव होता है और आश्रवनिरोध रूप संवर की स्थिति उत्पन्न होती है। संवर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनप्रेक्षा, परीषह सहन, जप तथा चारित्र की साधना का मार्ग है। संवर से आते हुए नये कर्म अवरुद्ध हो जाते हैं। निर्जरा के द्वारा जीव पूर्वबद्ध कर्मों के बंधन से ऋमिक मुक्त होता जाता है। निर्जरा की क्रमिक यात्रा के पश्चात् अन्ततः पूर्ण मोक्षावस्था आती है। मुक्ति के ये वे आयाम हैं, जहाँ सर्वप्रथम तत्त्व के प्रति जीव को श्रद्धा अर्थात् सत्यनिष्ठा होती है और यहीं से सम्यक्-ज्ञान की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। ज्ञान के सम्यक् होने में एकमात्र हेतु है सम्यक् दर्शन, अर्थात् सम्यक्त्व। सम्यक-ज्ञान के होने पर ही आत्मा संशय, विमोह और विभ्रम से रहित हो जाता है। ज्ञान की निष्कलषता ही ज्ञान का सम्यक्त्व है। सम्यक-दर्शन और सम्यकज्ञान के आधार पर ही मोह-क्षोभ रहित, वीतरागभावरूप सम्यक-चारित्र का आविर्भाव होता है।
उक्त रीत्या सम्यक स्थिति को प्राप्त दर्शन, ज्ञान और चारित्र अन्तजगत् में साधना का पवित्र त्रिवेणीसंगम है। तीनों का तीन रूप में नहीं; अन्ततः संगम के रूप में तीनों के एकरूप हो जाने में ही अहंभावरूप, परमात्मभावरूप अनन्त परम चैतन्य का, अक्षय, अजर, अमर प्रकाश प्रकट होता है। परन्तु ध्यान रखिए, उक्त अध्यात्म त्रिवेणी संगम की प्रथम धारा सम्यक्त्व है, जिसे दर्शन, दृष्टि, तत्त्वविनिश्चय, आत्मप्रतीति, आत्मानुभूति, श्रद्धा, निष्ठा एवं तत्त्वरुचि आदि अनेक अर्थभित उदात्त नामों से शास्त्रकार तत्त्वदर्शी चिदात्माओं ने अभिहित किया है, अतः धर्म-साधना के लिए प्रस्थानबिन्दु के रूप में सर्वप्रथम उसी का विशुद्ध होना परमावश्यक है। दर्शन विशुद्धि ही तीर्थकरत्व जैसे परम पद का प्रथम हेतु है।
___अतएव आवश्यकता इस बात की है कि वृत्तियों का अन्तरंग सत्यनिष्ठा के साथ परिष्कार हो, तदनन्तर सभी रागमूलक शुभाशुभ विभावों से निवृत्त होकर, शुद्ध स्वभाव में रमणता हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे मनुष्य न कर पाये। बस, इसके लिए एकमात्र सम्यक् संकल्पवान् होने की जरूरत है, श्रद्धा की पावन कलकल निनादिनी को अपने भीतर पूर्णरूपेण आत्मसात् करने की जरूरत है।
यह एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य जब-जब सत्योपलब्धि की ओर प्रवृत्त हआ है, उसके मन प्राण में अनिर्वचनीय एक दिव्य पुलक समाया है, उसकी चेतना में अमोघ जागरण-मंत्र ध्वनित हुआ है। वह तर्क और भाव की दोनों अवस्थाओं से गतिमान रहा है। श्रद्धा समत्वरूप से इन दोनों का वहन करती रहती है। और सत्योप
२०
सागर, नौका और नाविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org