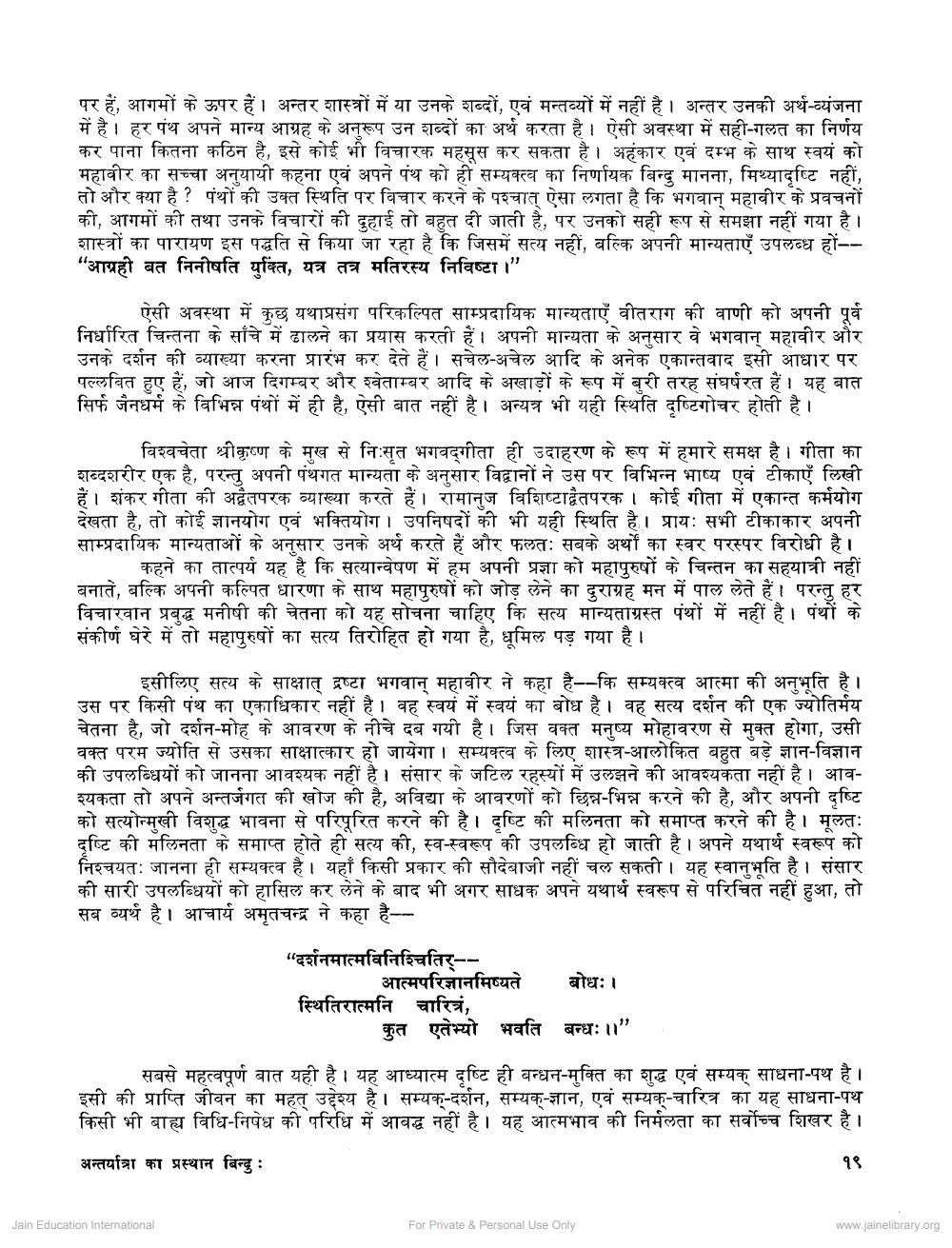________________
पर हैं, आगमों के ऊपर हैं। अन्तर शास्त्रों में या उनके शब्दों, एवं मन्तव्यों में नहीं है। अन्तर उनकी अर्थ-व्यंजना में है। हर पंथ अपने मान्य आग्रह के अनुरूप उन शब्दों का अर्थ करता है। ऐसी अवस्था में सही-गलत का निर्णय कर पाना कितना कठिन है, इसे कोई भी विचारक महसूस कर सकता है। अहंकार एवं दम्भ के साथ स्वयं को महावीर का सच्चा अनुयायी कहना एवं अपने पंथ को ही सम्यक्त्व का निर्णायक बिन्दु मानना, मिथ्यादृष्टि नहीं, तो और क्या है ? पंथों की उक्त स्थिति पर विचार करने के पश्चात् ऐसा लगता है कि भगवान् महावीर के प्रवचनों की, आगमों की तथा उनके विचारों की दुहाई तो बहुत दी जाती है, पर उनको सही रूप से समझा नहीं गया है। शास्त्रों का पारायण इस पद्धति से किया जा रहा है कि जिसमें सत्य नहीं, बल्कि अपनी मान्यताएँ उपलब्ध हों-- "आग्रही बत निनीषति यक्ति, यत्र तत्र मतिरस्य निविष्टा।"
ऐसी अवस्था में कुछ यथाप्रसंग परिकल्पित साम्प्रदायिक मान्यताएँ वीतराग की वाणी को अपनी पूर्व निर्धारित चिन्तना के साँचे में ढालने का प्रयास करती हैं। अपनी मान्यता के अनुसार वे भगवान महावीर और उनके दर्शन की व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं। सचेल-अचेल आदि के अनेक एकान्तवाद इसी आधार पर पल्लवित हुए हैं, जो आज दिगम्बर और श्वेताम्बर आदि के अखाड़ों के रूप में बुरी तरह संघर्षरत हैं। यह बात सिर्फ जैनधर्म के विभिन्न पंथों में ही है, ऐसी बात नहीं है। अन्यत्र भी यही स्थिति दृष्टिगोचर होती है।
विश्वचेता श्रीकृष्ण के मुख से निःसृत भगवद्गीता ही उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष है। गीता का शब्दशरीर एक है, परन्तु अपनी पंथगत मान्यता के अनुसार विद्वानों ने उस पर विभिन्न भाष्य एवं टीकाएँ लिखी हैं। शंकर गीता की अद्वैतपरक व्याख्या करते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतपरक । कोई गीता में एकान्त कर्मयोग देखता है, तो कोई ज्ञानयोग एवं भक्तियोग। उपनिषदों की भी यही स्थिति है। प्रायः सभी टीकाकार अपनी साम्प्रदायिक मान्यताओं के अनुसार उनके अर्थ करते हैं और फलत: सबके अर्थों का स्वर परस्पर विरोधी है।
कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यान्वेषण में हम अपनी प्रज्ञा को महापुरुषों के चिन्तन का सहयात्री नहीं बनाते, बल्कि अपनी कल्पित धारणा के साथ महापुरुषों को जोड़ लेने का दुराग्रह मन में पाल लेते हैं। परन्तु हर विचारवान प्रबुद्ध मनीषी की चेतना को यह सोचना चाहिए कि सत्य मान्यताग्रस्त पंथों में नहीं है। पंथों के संकीर्ण घेरे में तो महापुरुषों का सत्य तिरोहित हो गया है, धूमिल पड़ गया है।
इसीलिए सत्य के साक्षात् द्रष्टा भगवान् महावीर ने कहा है--कि सम्यक्त्व आत्मा की अनुभूति है। उस पर किसी पंथ का एकाधिकार नहीं है। वह स्वयं में स्वयं का बोध है। वह सत्य दर्शन की एक ज्योतिर्मय चेतना है, जो दर्शन-मोह के आवरण के नीचे दब गयी है। जिस वक्त मनुष्य मोहावरण से मुक्त होगा, उसी वक्त परम ज्योति से उसका साक्षात्कार हो जायेगा। सम्यक्त्व के लिए शास्त्र-आलोकित बहुत बड़े ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों को जानना आवश्यक नहीं है। संसार के जटिल रहस्यों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो अपने अन्तर्जगत की खोज की है, अविद्या के आवरणों को छिन्न-भिन्न करने की है, और अपनी दृष्टि को सत्योन्मुखी विशुद्ध भावना से परिपूरित करने की है। दृष्टि की मलिनता को समाप्त करने की है। मूलतः दृष्टि की मलिनता के समाप्त होते ही सत्य की, स्व-स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। अपने यथार्थ स्वरूप को निश्चयतः जानना ही सम्यक्त्व है। यहाँ किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं चल सकती। यह स्वानुभूति है। संसार की सारी उपलब्धियों को हासिल कर लेने के बाद भी अगर साधक अपने यथार्थ स्वरूप से परिचित नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ है। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है
"दर्शनमात्मविनिश्चितिर्--
आत्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः। स्थितिरात्मनि चारित्रं,
कुत एतेभ्यो भवति बन्धः॥"
सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यह आध्यात्म दष्टि ही बन्धन-मुक्ति का शुद्ध एवं सम्यक् साधना-पथ है। इसी की प्राप्ति जीवन का महत उद्देश्य है। सम्यक-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, एवं सम्यक्-चारित्र का यह साधना-पथ किसी भी बाह्य विधि-निषेध की परिधि में आबद्ध नहीं है। यह आत्मभाव की निर्मलता का सर्वोच्च शिखर है।
१९
अन्तर्यात्रा का प्रस्थान बिन्दु :
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org