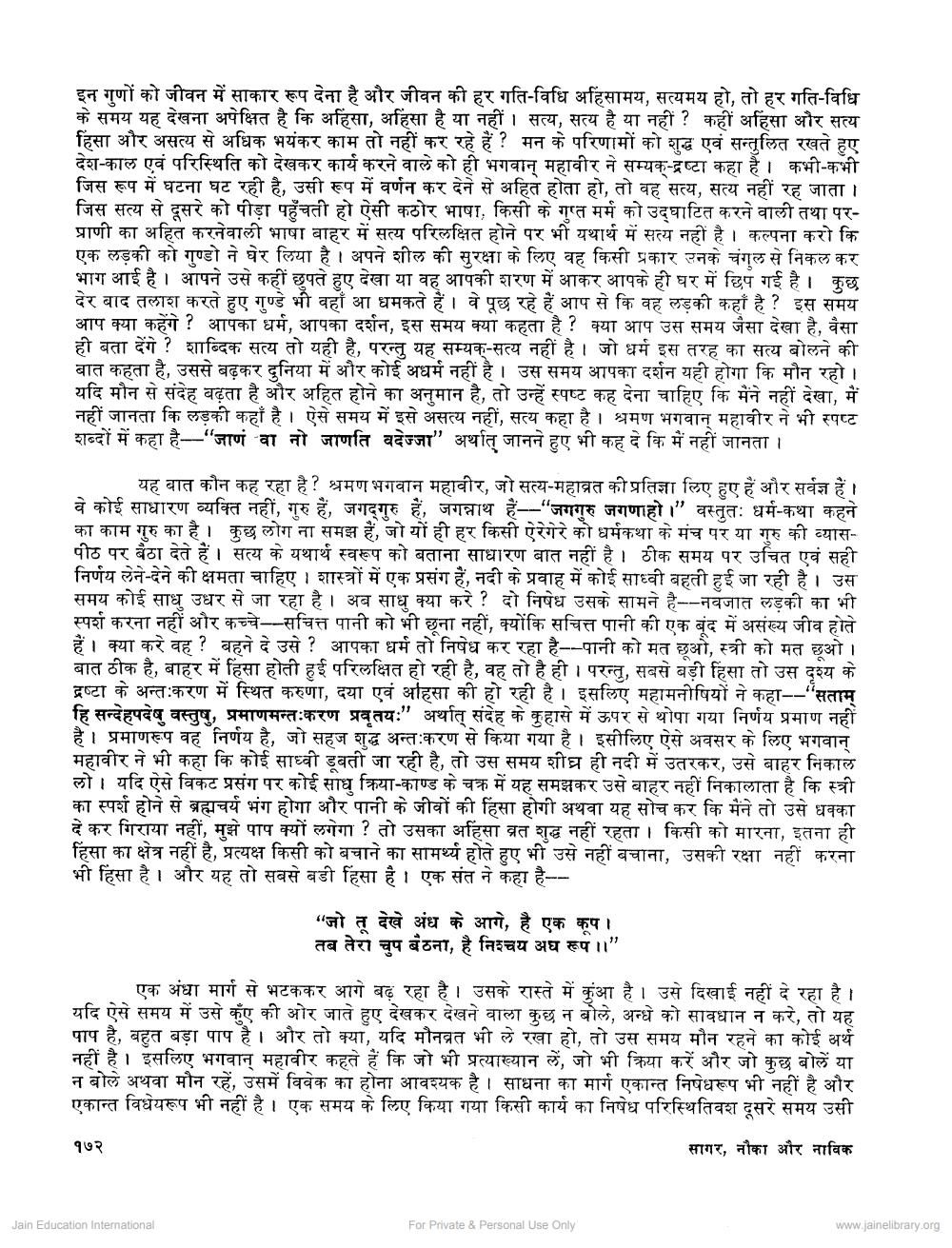________________
इन गुणों को जीवन में साकार रूप देना है और जीवन की हर गति-विधि अहिंसामय, सत्यमय हो, तो हर गति-विधि के समय यह देखना अपेक्षित है कि अहिंसा, अहिंसा है या नहीं। सत्य, सत्य है या नहीं? कहीं अहिंसा और सत्य हिंसा और असत्य से अधिक भयंकर काम तो नहीं कर रहे हैं? मन के परिणामों को शुद्ध एवं सन्तुलित रखते हुए देश-काल एवं परिस्थिति को देखकर कार्य करने वाले को ही भगवान् महावीर ने सम्यक्-द्रष्टा कहा है। कभी-कभी जिस रूप में घटना घट रही है, उसी रूप में वर्णन कर देने से अहित होता हो, तो वह सत्य, सत्य नहीं रह जाता। जिस सत्य से दूसरे को पीड़ा पहुँचती हो ऐसी कठोर भाषा, किसी के गुप्त मर्म को उद्घाटित करने वाली तथा परप्राणी का अहित करनेवाली भाषा बाहर में सत्य परिलक्षित होने पर भी यथार्थ में सत्य नहीं है। कल्पना करो कि एक लड़की को गुण्डो ने घेर लिया है। अपने शील की सुरक्षा के लिए वह किसी प्रकार उनके चंगुल से निकल कर भाग आई है। आपने उसे कहीं छुपते हए देखा या वह आपकी शरण में आकर आपके ही घर में छिप गई है। कुछ देर बाद तलाश करते हुए गुण्डे भी वहाँ आ धमकते हैं। वे पूछ रहे हैं आप से कि वह लड़की कहाँ है? इस समय आप क्या कहेंगे? आपका धर्म, आपका दर्शन, इस समय क्या कहता है ? क्या आप उस समय जैसा देखा है, वैसा ही बता देंगे? शाब्दिक सत्य तो यही है, परन्तु यह सम्यक्-सत्य नहीं है। जो धर्म इस तरह का सत्य बोलने की बात कहता है, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई अधर्म नहीं है। उस समय आपका दर्शन यही होगा कि मौन रहो। यदि मौन से संदेह बढ़ता है और अहित होने का अनुमान है, तो उन्हें स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि लड़की कहाँ है। ऐसे समय में इसे असत्य नहीं, सत्य कहा है। श्रमण भगवान महावीर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है-"जाणं वा नो जाणति वदेज्जा" अर्थात् जानने हुए भी कह दे कि मैं नहीं जानता।
त नहीं, गुरु हैं, जगद्गुरु
हर किसी ऐरेगेरे का
समय पर उचित
यह बात कौन कह रहा है? श्रमण भगवान महावीर, जो सत्य-महाव्रत की प्रतिज्ञा लिए हए हैं और सर्वज्ञ हैं। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु हैं, जगद्गुरु हैं, जगन्नाथ हैं-"जगगुरु जगणाहो।" वस्तुतः धर्म-कथा कहने का काम गुरु का है। कुछ लोग ना समझ हैं, जो यों ही हर किसी ऐरेगेरे को धर्मकथा के मंच पर या गुरु की व्यासपीठ पर बैठा देते हैं। सत्य के यथार्थ स्वरूप को बताना साधारण बात नहीं है। ठीक समय पर उचित एवं सही निर्णय लेने-देने की क्षमता चाहिए। शास्त्रों में एक प्रसंग हैं, नदी के प्रवाह में कोई साध्वी बहती हुई जा रही है। उस समय कोई साधु उधर से जा रहा है। अब साधु क्या करे? दो निषेध उसके सामने है--नवजात लड़की का भी स्पर्श करना नहीं और कच्चे-सचित्त पानी को भी छूना नहीं, क्योंकि सचित्त पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। क्या करे वह ? बहने दे उसे? आपका धर्म तो निषेध कर रहा है--पानी को मत छुओ, स्त्री को मत छओ। बात ठीक है, बाहर में हिंसा होती हुई परिलक्षित हो रही है, वह तो है ही। परन्तु, सबसे बड़ी हिंसा तो उस दृश्य के द्रष्टा के अन्तःकरण में स्थित करुणा, दया एवं हिसा की हो रही है। इसलिए महामनीषियों ने कहा--"सताम् हि सन्देहपदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तःकरण प्रवृतयः" अर्थात् संदेह के कुहासे में ऊपर से थोपा गया निर्णय प्रमाण नहीं है। प्रमाणरूप वह निर्णय है, जो सहज शुद्ध अन्तःकरण से किया गया है। इसीलिए ऐसे अवसर के लिए भगवान महावीर ने भी कहा कि कोई साध्वी डूबती जा रही है, तो उस समय शीघ्र ही नदी में उतरकर, उसे बाहर निकाल लो। यदि ऐसे विकट प्रसंग पर कोई साधु क्रिया-काण्ड के चक्र में यह समझकर उसे बाहर नहीं निकालाता है कि स्त्री का स्पर्श होने से ब्रह्मचर्य भंग होगा और पानी के जीवों की हिंसा होगी अथवा यह सोच कर कि मैंने तो उसे धक्का दे कर गिराया नहीं, मुझे पाप क्यों लगेगा? तो उसका अहिंसा व्रत शुद्ध नहीं रहता। किसी को मारना, इतना ही हिंसा का क्षेत्र नहीं है, प्रत्यक्ष किसी को बचाने का सामर्थ्य होते हुए भी उसे नहीं बचाना, उसकी रक्षा नहीं करना भी हिंसा है। और यह तो सबसे बडी हिंसा है। एक संत ने कहा है--
"जो त देखे अंध के आगे, है एक कूप। तब तेरा चुप बैठना, है निश्चय अघ रूप॥"
एक अंधा मार्ग से भटककर आगे बढ़ रहा है। उसके रास्ते में कुंआ है। उसे दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ऐसे समय में उसे कुँए की ओर जाते हुए देखकर देखने वाला कुछ न बोले, अन्धे को सावधान न करे, तो यह पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और तो क्या, यदि मौनव्रत भी ले रखा हो, तो उस समय मौन रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि जो भी प्रत्याख्यान लें, जो भी क्रिया करें और जो कुछ बोलें या न बोले अथवा मौन रहें, उसमें विवेक का होना आवश्यक है। साधना का मार्ग एकान्त निषेधरूप भी नहीं है और एकान्त विधेयरूप भी नहीं है। एक समय के लिए किया गया किसी कार्य का निषेध परिस्थितिवश दूसरे समय उसी
१७२
सागर, नौका और नाविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org