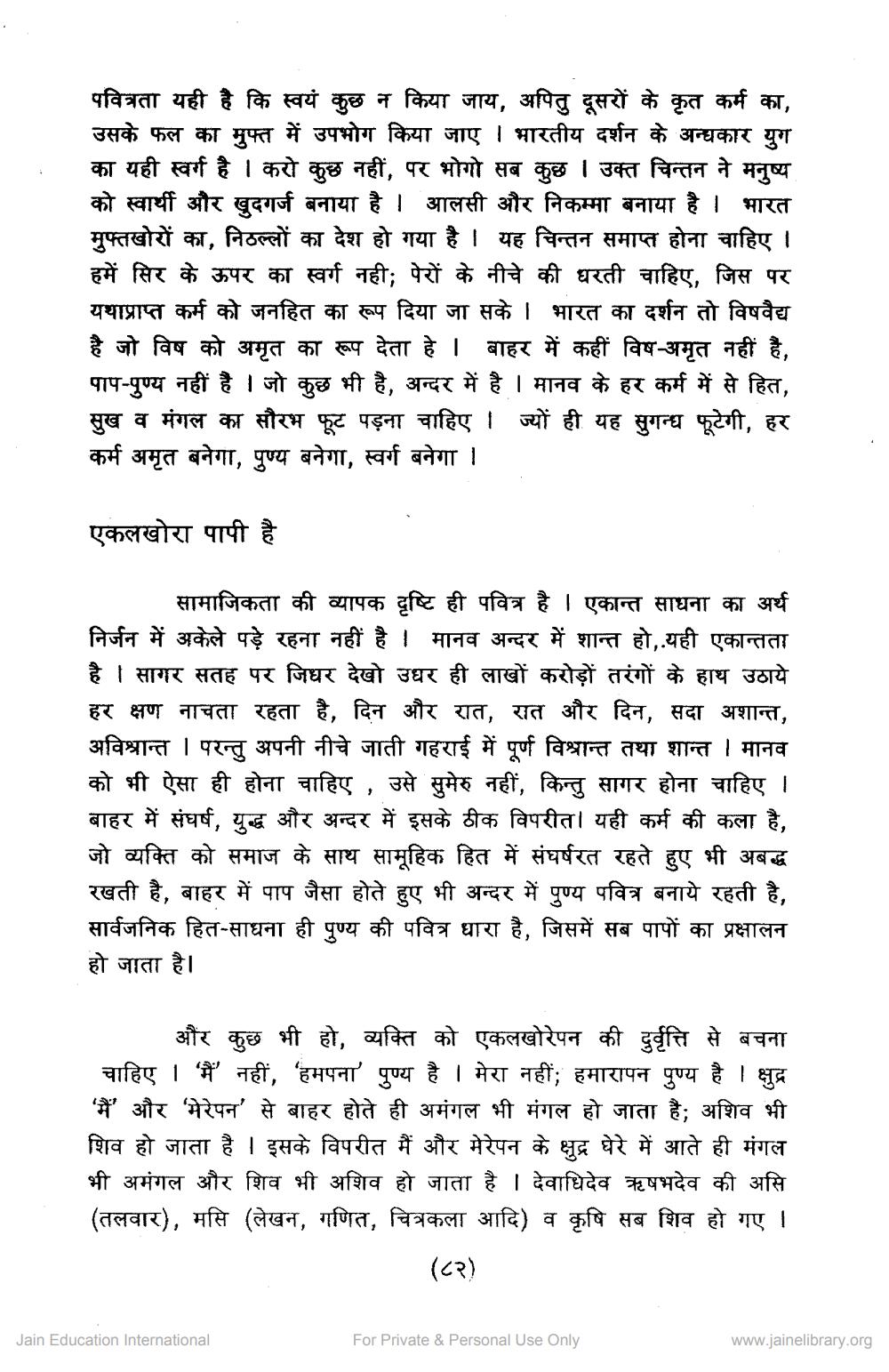________________
पवित्रता यही है कि स्वयं कुछ न किया जाय, अपितु दूसरों के कृत कर्म का, उसके फल का मुफ्त में उपभोग किया जाए । भारतीय दर्शन के अन्धकार युग का यही स्वर्ग है । करो कुछ नहीं, पर भोगो सब कुछ । उक्त चिन्तन ने मनुष्य को स्वार्थी और खुदगर्ज बनाया है । आलसी और निकम्मा बनाया है । भारत मुफ्तखोरों का, निठल्लों का देश हो गया है | यह चिन्तन समाप्त होना चाहिए । हमें सिर के ऊपर का स्वर्ग नही; पेरों के नीचे की धरती चाहिए, जिस पर यथाप्राप्त कर्म को जनहित का रूप दिया जा सके | भारत का दर्शन तो विषवैद्य है जो विष को अमृत का रूप देता हे | बाहर में कहीं विष-अमृत नहीं है, पाप-पुण्य नहीं है । जो कुछ भी है, अन्दर में है । मानव के हर कर्म में से हित, सुख व मंगल का सौरभ फूट पड़ना चाहिए । ज्यों ही यह सुगन्ध फूटेगी, हर कर्म अमृत बनेगा, पुण्य बनेगा, स्वर्ग बनेगा ।
एकलखोरा पापी है
सामाजिकता की व्यापक दृष्टि ही पवित्र है | एकान्त साधना का अर्थ निर्जन में अकेले पड़े रहना नहीं है । मानव अन्दर में शान्त हो,.यही एकान्तता है । सागर सतह पर जिधर देखो उधर ही लाखों करोड़ों तरंगों के हाथ उठाये हर क्षण नाचता रहता है, दिन और रात, रात और दिन, सदा अशान्त, अविश्रान्त | परन्तु अपनी नीचे जाती गहराई में पूर्ण विश्रान्त तथा शान्त । मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए , उसे सुमेरु नहीं, किन्तु सागर होना चाहिए । बाहर में संघर्ष, युद्ध और अन्दर में इसके ठीक विपरीत। यही कर्म की कला है, जो व्यक्ति को समाज के साथ सामूहिक हित में संघर्षरत रहते हुए भी अबद्ध रखती है, बाहर में पाप जैसा होते हुए भी अन्दर में पुण्य पवित्र बनाये रहती है, सार्वजनिक हित-साधना ही पुण्य की पवित्र धारा है, जिसमें सब पापों का प्रक्षालन हो जाता है।
और कुछ भी हो, व्यक्ति को एकलखोरेपन की दुर्वृत्ति से बचना चाहिए । 'मैं' नहीं, 'हमपना' पुण्य है । मेरा नहीं; हमारापन पुण्य है । क्षुद्र 'मैं' और 'मेरेपन' से बाहर होते ही अमंगल भी मंगल हो जाता है; अशिव भी शिव हो जाता है । इसके विपरीत मैं और मेरेपन के क्षुद्र घेरे में आते ही मंगल भी अमंगल और शिव भी अशिव हो जाता है । देवाधिदेव ऋषभदेव की असि (तलवार), मसि (लेखन, गणित, चित्रकला आदि) व कृषि सब शिव हो गए ।
(८२)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org