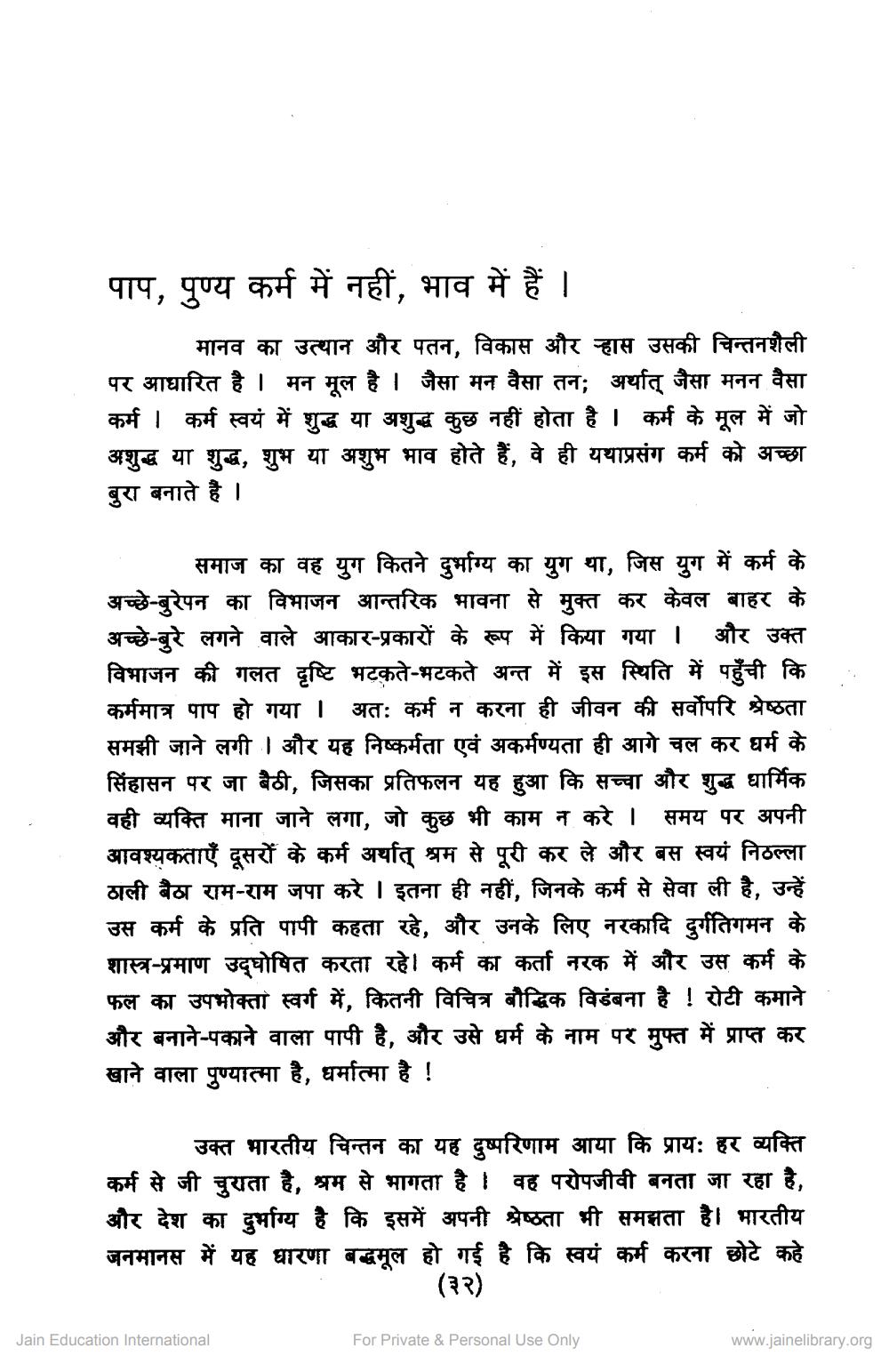________________
पाप, पुण्य कर्म में नहीं, भाव में हैं ।
मानव का उत्थान और पतन, विकास और न्हास उसकी चिन्तनशैली
अर्थात् जैसा मनन वैसा
पर आधारित है । मन मूल है । जैसा मन वैसा तन; कर्म । कर्म स्वयं में शुद्ध या अशुद्ध कुछ नहीं होता है । कर्म के मूल में जो अशुद्ध या शुद्ध, शुभ या अशुभ भाव होते हैं, वे ही यथाप्रसंग कर्म को अच्छा बुरा बनाते है ।
समाज का वह युग कितने दुर्भाग्य का युग था, जिस युग में कर्म के अच्छे-बुरेपन का विभाजन आन्तरिक भावना से मुक्त कर केवल बाहर के अच्छे-बुरे लगने वाले आकार-प्रकारों के रूप में किया गया । और उक्त विभाजन की गलत दृष्टि भटकते-भटकते अन्त में इस स्थिति में पहुँची कि कर्ममात्र पाप हो गया । अतः कर्म न करना ही जीवन की सर्वोपरि श्रेष्ठता समझी जाने लगी । और यह निष्कर्मता एवं अकर्मण्यता ही आगे चल कर धर्म के सिंहासन पर जा बैठी, जिसका प्रतिफलन यह हुआ कि सच्चा और शुद्ध धार्मिक वही व्यक्ति माना जाने लगा, जो कुछ भी काम न करे । समय पर अपनी आवश्यकताएँ दूसरों के कर्म अर्थात् श्रम से पूरी कर ले और बस स्वयं निठल्ला ठाली बैठा राम-राम जपा करे । इतना ही नहीं, जिनके कर्म से सेवा ली है, उन्हें उस कर्म के प्रति पापी कहता रहे, और उनके लिए नरकादि दुर्गतिगमन के शास्त्र - प्रमाण उद्घोषित करता रहे। कर्म का कर्ता नरक में और उस कर्म के फल का उपभोक्ता स्वर्ग में, कितनी विचित्र बौद्धिक विडंबना है ! रोटी कमाने और बनाने - पकाने वाला पापी है, और उसे धर्म के नाम पर मुफ्त में प्राप्त कर खाने वाला पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है !
उक्त भारतीय चिन्तन का यह दुष्परिणाम आया कि प्राय: हर व्यक्ति कर्म से जी चुराता है, श्रम से भागता है । वह परोपजीवी बनता जा रहा है, और देश का दुर्भाग्य है कि इसमें अपनी श्रेष्ठता भी समझता है। भारतीय जनमानस में यह धारणा बद्धमूल हो गई है कि स्वयं कर्म करना छोटे कहे
(३२)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org