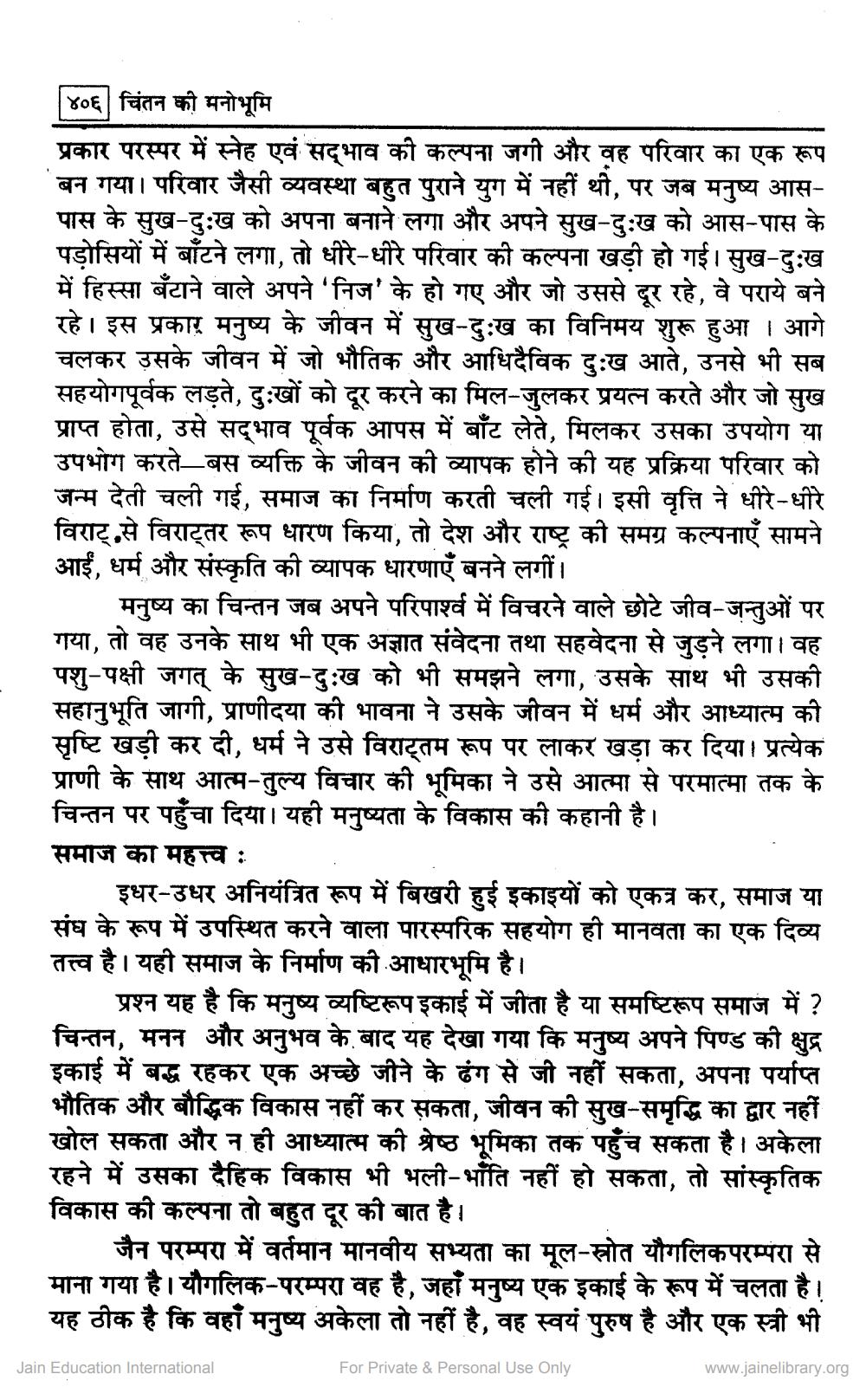________________
४०६ चिंतन की मनोभूमि
प्रकार परस्पर में स्नेह एवं सद्भाव की कल्पना जगी और वह परिवार का एक रूप बन गया। परिवार जैसी व्यवस्था बहुत पुराने युग में नहीं थी, पर जब मनुष्य आसपास के सुख-दुःख को अपना बनाने लगा और अपने सुख-दुःख को आस-पास के पड़ोसियों में बाँटने लगा, तो धीरे-धीरे परिवार की कल्पना खड़ी हो गई। सुख-दुःख में हिस्सा बँटाने वाले अपने 'निज' के हो गए और जो उससे दूर रहे, वे पराये बने रहे। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख-दुःख का विनिमय शुरू हुआ । आगे चलकर उसके जीवन में जो भौतिक और आधिदैविक दुःख आते, उनसे भी सब सहयोगपूर्वक लड़ते, दुःखों को दूर करने का मिल-जुलकर प्रयत्न करते और जो सुख प्राप्त होता, उसे सद्भाव पूर्वक आपस में बाँट लेते, मिलकर उसका उपयोग या उपभोग करते- बस व्यक्ति के जीवन की व्यापक होने की यह प्रक्रिया परिवार को जन्म देती चली गई, समाज का निर्माण करती चली गई। इसी वृत्ति ने धीरे-धीरे विराट् से विराट्तर रूप धारण किया, तो देश और राष्ट्र की समग्र कल्पनाएँ सामने आईं, धर्म और संस्कृति की व्यापक धारणाएँ बनने लगीं।
मनुष्य का चिन्तन जब अपने परिपार्श्व में विचरने वाले छोटे जीव-जन्तुओं पर गया, तो वह उनके साथ भी एक अज्ञात संवेदना तथा सहवेदना से जुड़ने लगा। वह पशु-पक्षी जगत् के सुख-दुःख को भी समझने लगा, उसके साथ भी उसकी सहानुभूति जागी, प्राणीदया की भावना ने उसके जीवन में धर्म और आध्यात्म की सृष्टि खड़ी कर दी, धर्म ने उसे विराट्तम रूप पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रत्येक प्राणी के साथ आत्म-तुल्य विचार की भूमिका ने उसे आत्मा से परमात्मा तक के चिन्तन पर पहुँचा दिया। यही मनुष्यता के विकास की कहानी है।
समाज का महत्त्व :
इधर-उधर अनियंत्रित रूप में बिखरी हुई इकाइयों को एकत्र कर, समाज या संघ के रूप में उपस्थित करने वाला पारस्परिक सहयोग ही मानवता का एक दिव्य तत्त्व है। यही समाज के निर्माण की आधारभूमि है।
प्रश्न यह है कि मनुष्य व्यष्टिरूप इकाई में जीता है या समष्टिरूप समाज में ? चिन्तन, मनन और अनुभव के बाद यह देखा गया कि मनुष्य अपने पिण्ड की क्षुद्र इकाई में बद्ध रहकर एक अच्छे जीने के ढंग से जी नहीं सकता, अपना पर्याप्त भौतिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता, जीवन की सुख-समृद्धि का द्वार नहीं खोल सकता और न ही आध्यात्म की श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है। अकेला रहने में उसका दैहिक विकास भी भली-भाँति नहीं हो सकता, तो सांस्कृतिक विकास की कल्पना तो बहुत दूर की बात है।
जैन परम्परा में वर्तमान मानवीय सभ्यता का मूल स्रोत यौगलिकपरम्परा से माना गया है। यौगलिक परम्परा वह है, जहाँ मनुष्य एक इकाई के रूप में चलता है। यह ठीक है कि वहाँ मनुष्य अकेला तो नहीं है, वह स्वयं पुरुष है और एक स्त्री भी
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International