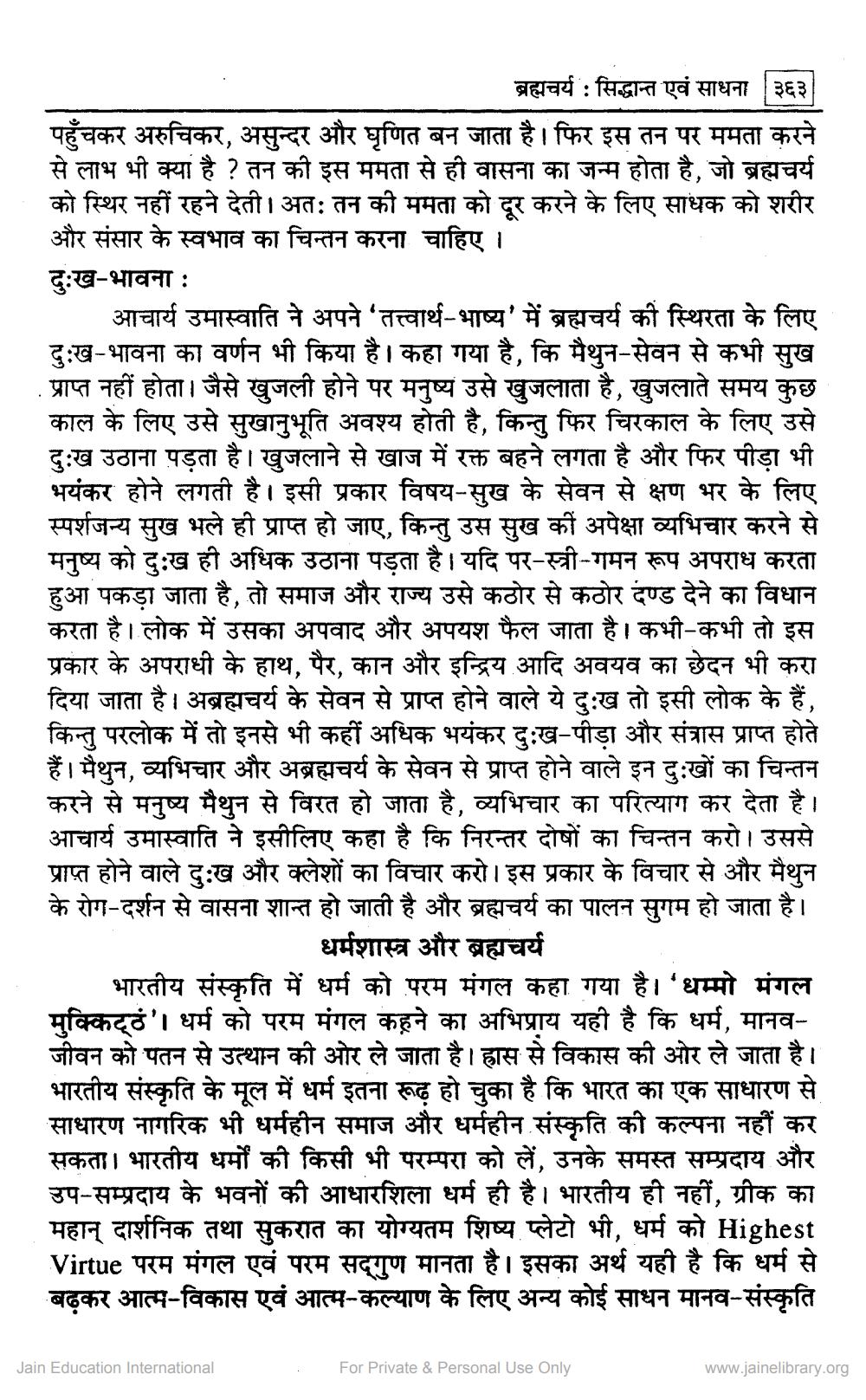________________
ब्रह्मचर्य : सिद्धान्त एवं साधना ३६३) पहुँचकर अरुचिकर, असुन्दर और घृणित बन जाता है। फिर इस तन पर ममता करने से लाभ भी क्या है ? तन की इस ममता से ही वासना का जन्म होता है, जो ब्रह्मचर्य को स्थिर नहीं रहने देती। अतः तन की ममता को दूर करने के लिए साधक को शरीर और संसार के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए। दुःख-भावना :
आचार्य उमास्वाति ने अपने 'तत्त्वार्थ-भाष्य' में ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए दु:ख-भावना का वर्णन भी किया है। कहा गया है, कि मैथुन-सेवन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे खुजली होने पर मनुष्य उसे खुजलाता है, खुजलाते समय कुछ काल के लिए उसे सुखानुभूति अवश्य होती है, किन्तु फिर चिरकाल के लिए उसे दुःख उठाना पड़ता है। खुजलाने से खाज में रक्त बहने लगता है और फिर पीड़ा भी भयंकर होने लगती है। इसी प्रकार विषय-सुख के सेवन से क्षण भर के लिए स्पर्शजन्य सुख भले ही प्राप्त हो जाए, किन्तु उस सुख की अपेक्षा व्यभिचार करने से मनुष्य को दुःख ही अधिक उठाना पड़ता है। यदि पर-स्त्री-गमन रूप अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है, तो समाज और राज्य उसे कठोर से कठोर दण्ड देने का विधान करता है। लोक में उसका अपवाद और अपयश फैल जाता है। कभी-कभी तो इस प्रकार के अपराधी के हाथ, पैर, कान और इन्द्रिय आदि अवयव का छेदन भी करा दिया जाता है। अब्रह्मचर्य के सेवन से प्राप्त होने वाले ये दुःख तो इसी लोक के हैं, किन्तु परलोक में तो इनसे भी कहीं अधिक भयंकर दुःख-पीड़ा और संत्रास प्राप्त होते हैं। मैथुन, व्यभिचार और अब्रह्मचर्य के सेवन से प्राप्त होने वाले इन दुःखों का चिन्तन करने से मनुष्य मैथुन से विरत हो जाता है, व्यभिचार का परित्याग कर देता है। आचार्य उमास्वाति ने इसीलिए कहा है कि निरन्तर दोषों का चिन्तन करो। उससे प्राप्त होने वाले दुःख और क्लेशों का विचार करो। इस प्रकार के विचार से और मैथुन के रोग-दर्शन से वासना शान्त हो जाती है और ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो जाता है।
धर्मशास्त्र और ब्रह्मचर्य ___ भारतीय संस्कृति में धर्म को परम मंगल कहा गया है। 'धम्मो मंगल मुक्किळं'। धर्म को परम मंगल कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म, मानवजीवन को पतन से उत्थान की ओर ले जाता है। ह्रास से विकास की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल में धर्म इतना रूढ़ हो चुका है कि भारत का एक साधारण से साधारण नागरिक भी धर्महीन समाज और धर्महीन संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकता। भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा को लें, उनके समस्त सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय के भवनों की आधारशिला धर्म ही है। भारतीय ही नहीं, ग्रीक का महान् दार्शनिक तथा सुकरात का योग्यतम शिष्य प्लेटो भी, धर्म को Highest Virtue परम मंगल एवं परम सद्गुण मानता है। इसका अर्थ यही है कि धर्म से बढ़कर आत्म-विकास एवं आत्म-कल्याण के लिए अन्य कोई साधन मानव-संस्कृति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org