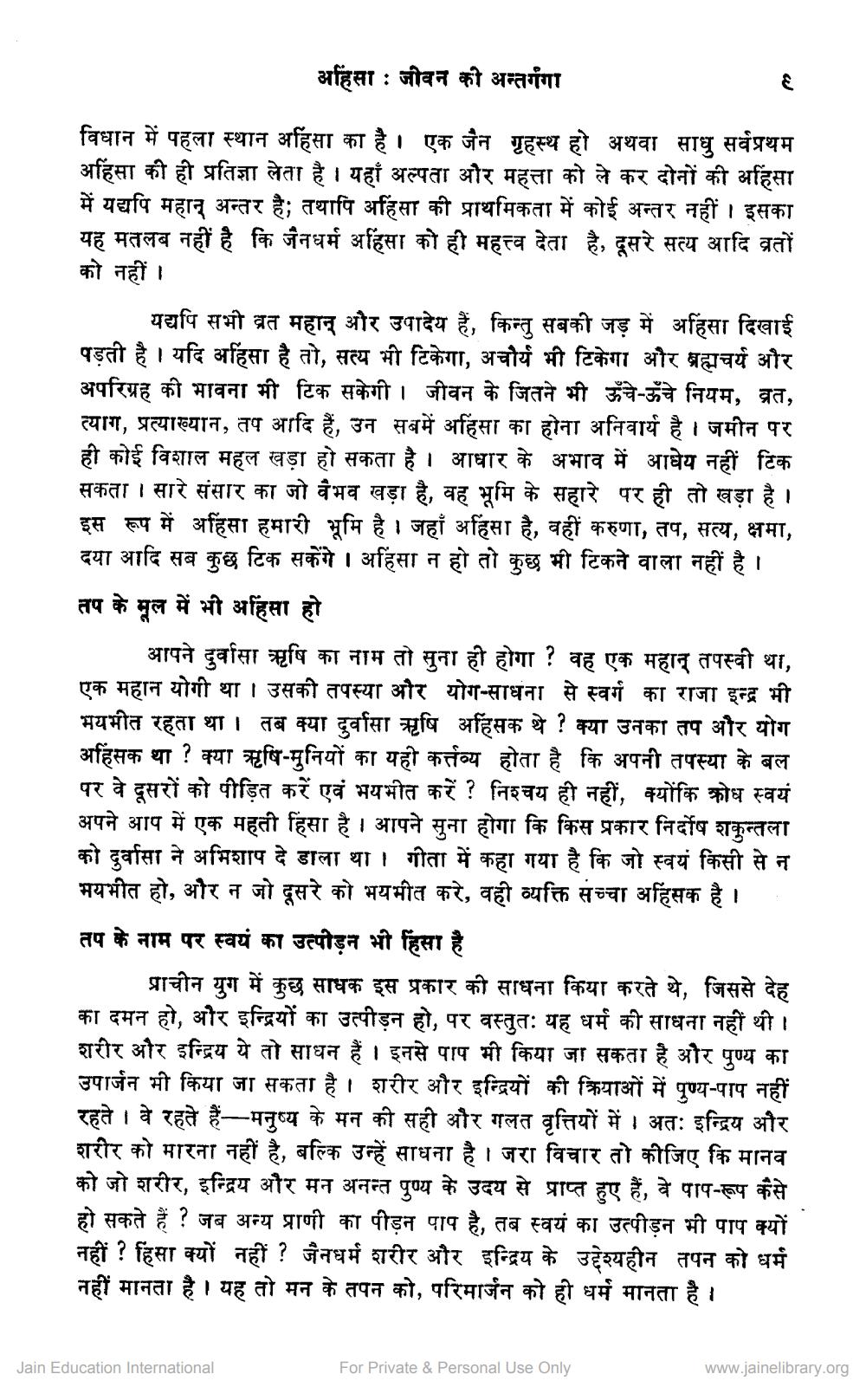________________
अहिंसा : जीवन को अन्तगंगा
विधान में पहला स्थान अहिंसा का है। एक जैन गृहस्थ हो अथवा साधु सर्वप्रथम अहिंसा की ही प्रतिज्ञा लेता है। यहाँ अल्पता और महत्ता को ले कर दोनों की अहिंसा में यद्यपि महान् अन्तर है; तथापि अहिंसा की प्राथमिकता में कोई अन्तर नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि जैनधर्म अहिंसा को ही महत्त्व देता है, दूसरे सत्य आदि व्रतों को नहीं।
यद्यपि सभी व्रत महान् और उपादेय हैं, किन्तु सबकी जड़ में अहिंसा दिखाई पड़ती है। यदि अहिंसा है तो, सत्य भी टिकेगा, अचौर्य भी टिकेगा और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की भावना भी टिक सकेगी। जीवन के जितने भी ऊँचे-ऊँचे नियम, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान, तप आदि हैं, उन सबमें अहिंसा का होना अनिवार्य है । जमीन पर ही कोई विशाल महल खड़ा हो सकता है। आधार के अभाव में आधेय नहीं टिक सकता । सारे संसार का जो वैभव खड़ा है, वह भूमि के सहारे पर ही तो खड़ा है । इस रूप में अहिंसा हमारी भूमि है । जहाँ अहिंसा है, वहीं करुणा, तप, सत्य, क्षमा, दया आदि सब कुछ टिक सकेंगे । अहिंसा न हो तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तप के मूल में भी अहिंसा हो
आपने दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुना ही होगा ? वह एक महान् तपस्वी था, एक महान योगी था। उसकी तपस्या और योग-साधना से स्वर्ग का राजा इन्द्र भी भयभीत रहता था। तब क्या दुर्वासा ऋषि अहिंसक थे ? क्या उनका तप और योग अहिंसक था ? क्या ऋषि-मुनियों का यही कर्तव्य होता है कि अपनी तपस्या के बल पर वे दूसरों को पीड़ित करें एवं भयभीत करें ? निश्चय ही नहीं, क्योंकि क्रोध स्वयं अपने आप में एक महती हिंसा है । आपने सुना होगा कि किस प्रकार निर्दोष शकुन्तला को दुर्वासा ने अभिशाप दे डाला था। गीता में कहा गया है कि जो स्वयं किसी से न भयभीत हो, और न जो दूसरे को भयभीत करे, वही व्यक्ति सच्चा अहिंसक है। तप के नाम पर स्वयं का उत्पीड़न भी हिंसा है
प्राचीन युग में कुछ साधक इस प्रकार की साधना किया करते थे, जिससे देह का दमन हो, और इन्द्रियों का उत्पीड़न हो, पर वस्तुतः यह धर्म की साधना नहीं थी। शरीर और इन्द्रिय ये तो साधन हैं । इनसे पाप भी किया जा सकता है और पुण्य का उपार्जन भी किया जा सकता है। शरीर और इन्द्रियों की क्रियाओं में पुण्य-पाप नहीं रहते । वे रहते हैं—मनुष्य के मन की सही और गलत वृत्तियों में । अतः इन्द्रिय और शरीर को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें साधना है । जरा विचार तो कीजिए कि मानव को जो शरीर, इन्द्रिय और मन अनन्त पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, वे पाप-रूप कैसे हो सकते हैं ? जब अन्य प्राणी का पीड़न पाप है, तब स्वयं का उत्पीड़न भी पाप क्यों नहीं ? हिंसा क्यों नहीं ? जैनधर्म शरीर और इन्द्रिय के उद्देश्यहीन तपन को धर्म नहीं मानता है। यह तो मन के तपन को, परिमार्जन को ही धर्म मानता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org