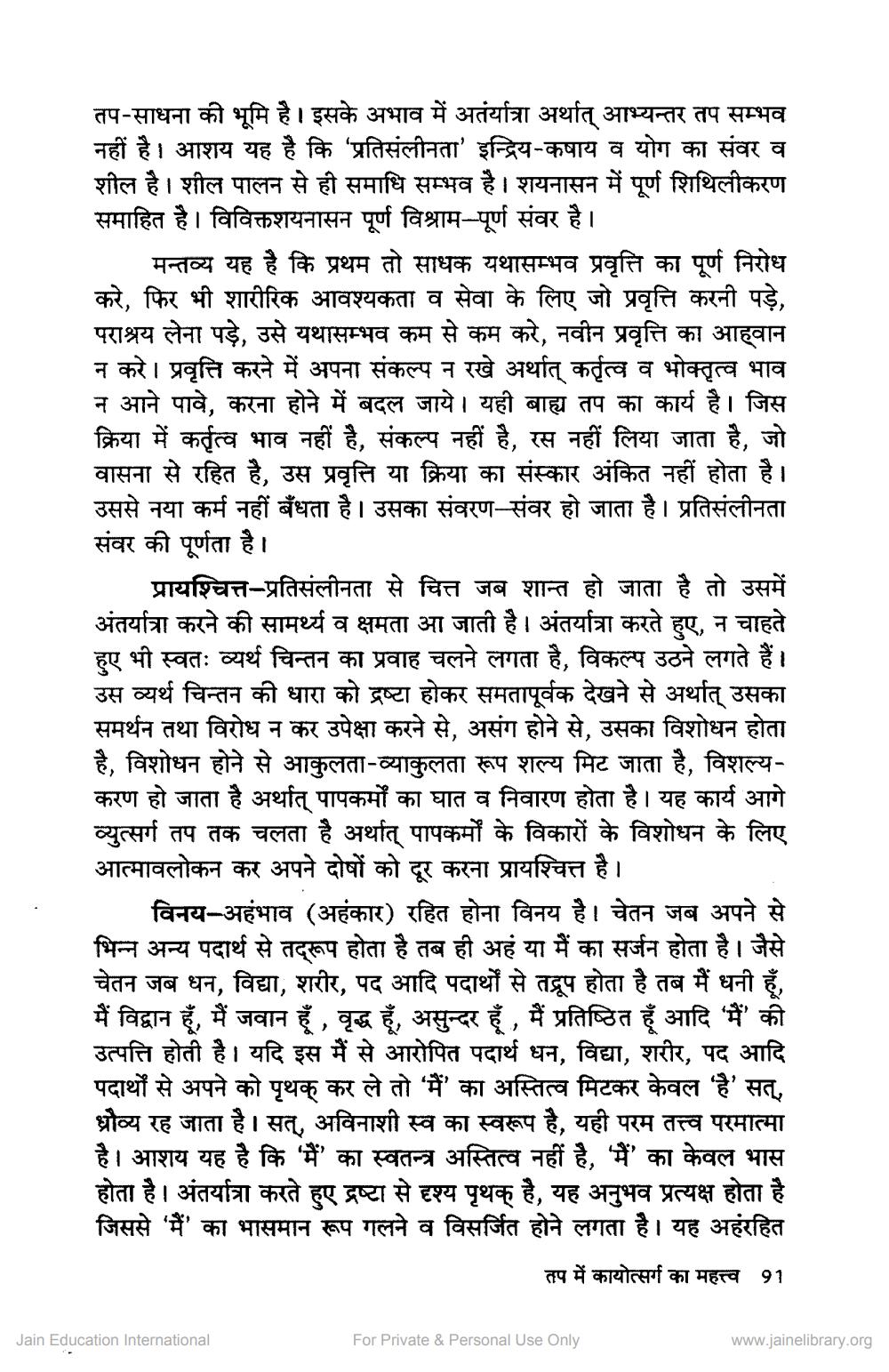________________
तप-साधना की भूमि है। इसके अभाव में अतंर्यात्रा अर्थात् आभ्यन्तर तप सम्भव नहीं है। आशय यह है कि 'प्रतिसंलीनता' इन्द्रिय-कषाय व योग का संवर व शील है। शील पालन से ही समाधि सम्भव है। शयनासन में पूर्ण शिथिलीकरण समाहित है। विविक्तशयनासन पूर्ण विश्राम-पूर्ण संवर है।
मन्तव्य यह है कि प्रथम तो साधक यथासम्भव प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध करे, फिर भी शारीरिक आवश्यकता व सेवा के लिए जो प्रवृत्ति करनी पड़े, पराश्रय लेना पड़े, उसे यथासम्भव कम से कम करे, नवीन प्रवृत्ति का आह्वान न करे। प्रवृत्ति करने में अपना संकल्प न रखे अर्थात् कर्तृत्व व भोक्तृत्व भाव न आने पावे, करना होने में बदल जाये। यही बाह्य तप का कार्य है। जिस क्रिया में कर्तृत्व भाव नहीं है, संकल्प नहीं है, रस नहीं लिया जाता है, जो वासना से रहित है, उस प्रवृत्ति या क्रिया का संस्कार अंकित नहीं होता है। उससे नया कर्म नहीं बँधता है। उसका संवरण-संवर हो जाता है। प्रतिसंलीनता संवर की पूर्णता है।
प्रायश्चित्त-प्रतिसंलीनता से चित्त जब शान्त हो जाता है तो उसमें अंतर्यात्रा करने की सामर्थ्य व क्षमता आ जाती है। अंतर्यात्रा करते हुए, न चाहते हुए भी स्वतः व्यर्थ चिन्तन का प्रवाह चलने लगता है, विकल्प उठने लगते हैं। उस व्यर्थ चिन्तन की धारा को द्रष्टा होकर समतापूर्वक देखने से अर्थात् उसका समर्थन तथा विरोध न कर उपेक्षा करने से, असंग होने से, उसका विशोधन होता है, विशोधन होने से आकुलता-व्याकुलता रूप शल्य मिट जाता है, विशल्यकरण हो जाता है अर्थात् पापकर्मों का घात व निवारण होता है। यह कार्य आगे व्युत्सर्ग तप तक चलता है अर्थात् पापकर्मों के विकारों के विशोधन के लिए आत्मावलोकन कर अपने दोषों को दूर करना प्रायश्चित्त है।
विनय-अहंभाव (अहंकार) रहित होना विनय है। चेतन जब अपने से भिन्न अन्य पदार्थ से तद्रूप होता है तब ही अहं या मैं का सर्जन होता है। जैसे चेतन जब धन, विद्या, शरीर, पद आदि पदार्थों से तद्रूप होता है तब मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जवान हूँ , वृद्ध हूँ, असुन्दर हूँ , मैं प्रतिष्ठित हूँ आदि 'मैं' की उत्पत्ति होती है। यदि इस मैं से आरोपित पदार्थ धन, विद्या, शरीर, पद आदि पदार्थों से अपने को पृथक् कर ले तो 'मैं' का अस्तित्व मिटकर केवल 'है' सत्, ध्रौव्य रह जाता है। सत्, अविनाशी स्व का स्वरूप है, यही परम तत्त्व परमात्मा है। आशय यह है कि 'मैं' का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, 'मैं' का केवल भास होता है। अंतर्यात्रा करते हुए द्रष्टा से दृश्य पृथक् है, यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है जिससे 'मैं' का भासमान रूप गलने व विसर्जित होने लगता है। यह अहंरहित
तप में कायोत्सर्ग का महत्त्व 91
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org