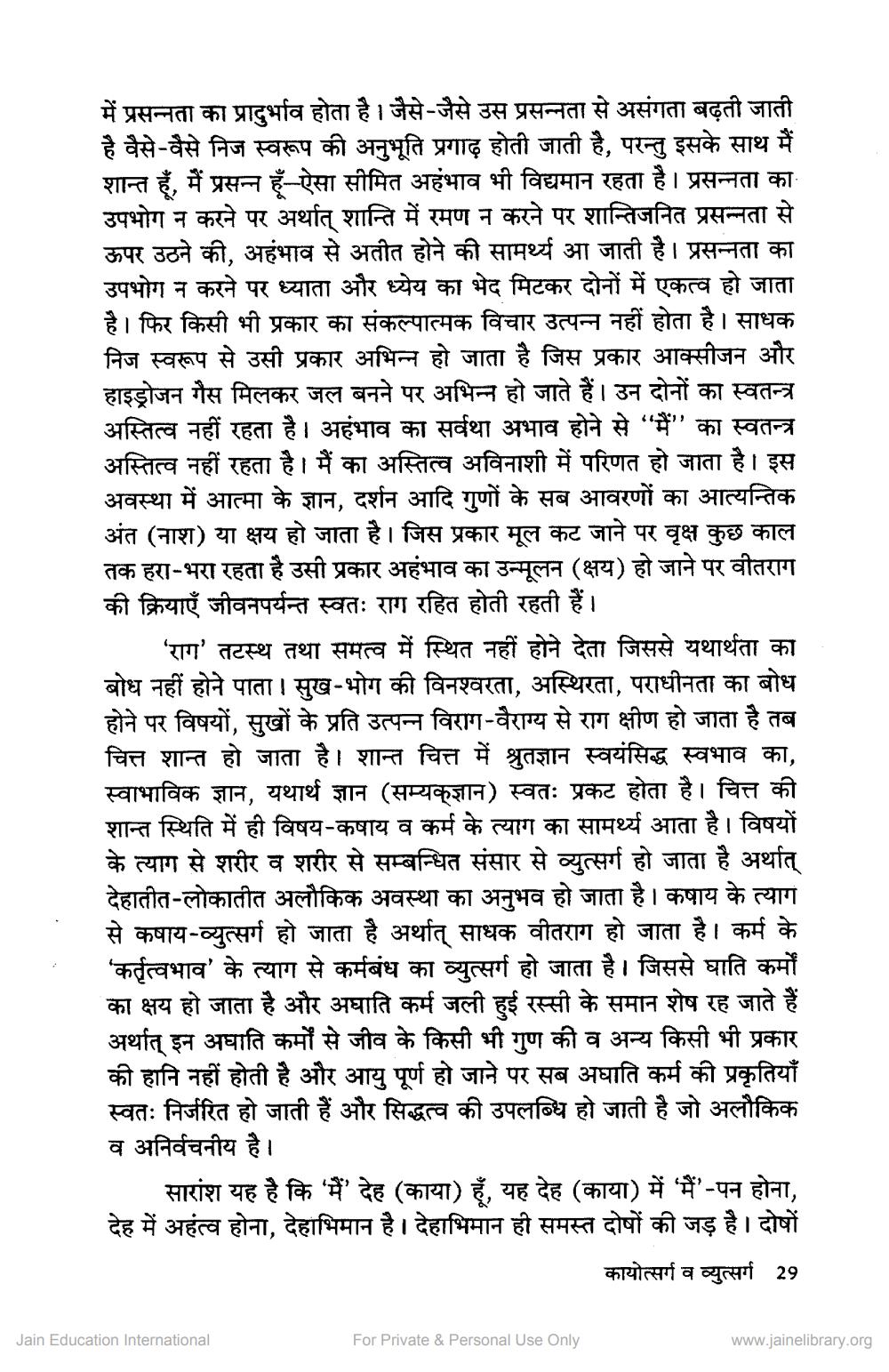________________
में प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। जैसे-जैसे उस प्रसन्नता से असंगता बढ़ती जाती है वैसे-वैसे निज स्वरूप की अनुभूति प्रगाढ़ होती जाती है, परन्तु इसके साथ मैं शान्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ-ऐसा सीमित अहंभाव भी विद्यमान रहता है। प्रसन्नता का उपभोग न करने पर अर्थात् शान्ति में रमण न करने पर शान्तिजनित प्रसन्नता से ऊपर उठने की, अहंभाव से अतीत होने की सामर्थ्य आ जाती है। प्रसन्नता का उपभोग न करने पर ध्याता और ध्येय का भेद मिटकर दोनों में एकत्व हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार का संकल्पात्मक विचार उत्पन्न नहीं होता है। साधक निज स्वरूप से उसी प्रकार अभिन्न हो जाता है जिस प्रकार आक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर जल बनने पर अभिन्न हो जाते हैं। उन दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। अहंभाव का सर्वथा अभाव होने से "मैं' का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। मैं का अस्तित्व अविनाशी में परिणत हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि गुणों के सब आवरणों का आत्यन्तिक अंत (नाश) या क्षय हो जाता है। जिस प्रकार मूल कट जाने पर वृक्ष कुछ काल तक हरा-भरा रहता है उसी प्रकार अहंभाव का उन्मूलन (क्षय) हो जाने पर वीतराग की क्रियाएँ जीवनपर्यन्त स्वतः राग रहित होती रहती हैं। ___ 'राग' तटस्थ तथा समत्व में स्थित नहीं होने देता जिससे यथार्थता का बोध नहीं होने पाता । सुख-भोग की विनश्वरता, अस्थिरता, पराधीनता का बोध होने पर विषयों, सुखों के प्रति उत्पन्न विराग-वैराग्य से राग क्षीण हो जाता है तब चित्त शान्त हो जाता है। शान्त चित्त में श्रुतज्ञान स्वयंसिद्ध स्वभाव का, स्वाभाविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान (सम्यक्ज्ञान) स्वतः प्रकट होता है। चित्त की शान्त स्थिति में ही विषय-कषाय व कर्म के त्याग का सामर्थ्य आता है। विषयों के त्याग से शरीर व शरीर से सम्बन्धित संसार से व्युत्सर्ग हो जाता है अर्थात् देहातीत-लोकातीत अलौकिक अवस्था का अनुभव हो जाता है। कषाय के त्याग से कषाय-व्युत्सर्ग हो जाता है अर्थात् साधक वीतराग हो जाता है। कर्म के 'कर्तृत्वभाव' के त्याग से कर्मबंध का व्युत्सर्ग हो जाता है। जिससे घाति कर्मों का क्षय हो जाता है और अघाति कर्म जली हुई रस्सी के समान शेष रह जाते हैं अर्थात् इन अघाति कर्मों से जीव के किसी भी गुण की व अन्य किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और आयु पूर्ण हो जाने पर सब अघाति कर्म की प्रकृतियाँ स्वतः निर्जरित हो जाती हैं और सिद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है जो अलौकिक व अनिर्वचनीय है।
सारांश यह है कि 'मैं' देह (काया) हैं, यह देह (काया) में 'मैं'-पन होना, देह में अहंत्व होना, देहाभिमान है। देहाभिमान ही समस्त दोषों की जड़ है। दोषों
कायोत्सर्ग व व्युत्सर्ग 29
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org