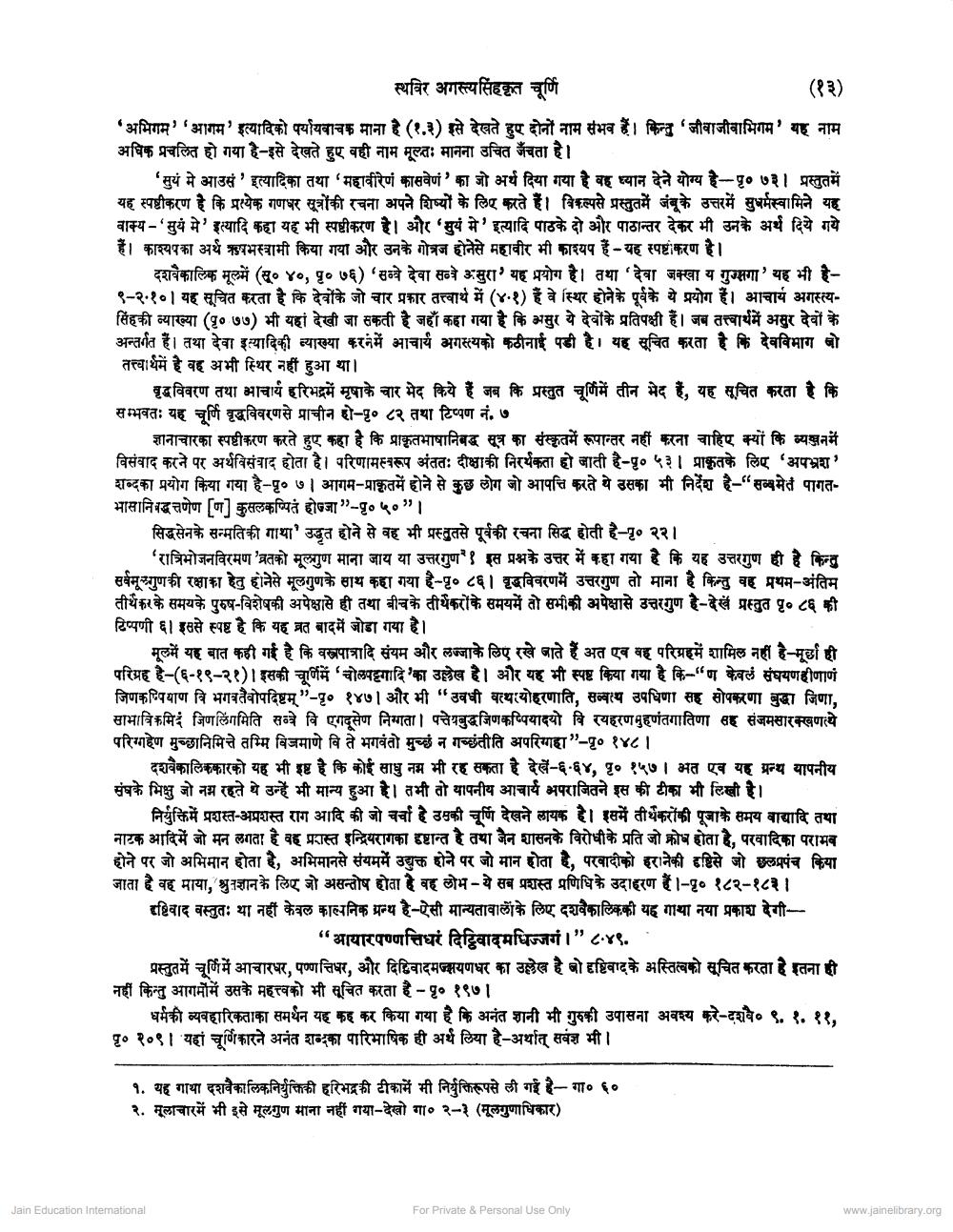________________
स्थविर अगस्त्यसिंहकृत चूर्णि
(१३) 'अभिगम' 'आगम' इत्यादिको पर्यायवाचक माना है (१.३) इसे देखते हुए दोनों नाम संभव हैं। किन्तु 'जीवाजीवाभिगम' यह नाम अधिक प्रचलित हो गया है-इसे देखते हुए वही नाम मूलतः मानना उचित ऊँचता है।
'सुयं मे आउसं ' इत्यादिका तथा 'महावीरेणं कासवेणं' का जो अर्थ दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है-पृ०७३। प्रस्तुतमें यह स्पष्टीकरण है कि प्रत्येक गणधर सूत्रोंकी रचना अपने शिष्यों के लिए करते हैं। विकल्पसे प्रस्तुतमें जंबूके उत्तर में सुधर्मस्वामिने यह वाक्य - 'सुयं मे' इत्यादि कहा यह भी स्पष्टीकरण है। और 'सुयं मे' इत्यादि पाठके दो और पाठान्तर देकर भी उनके अर्थ दिये गये हैं। काश्यपका अर्थ ऋषभस्वामी किया गया और उनके गोत्रज होनेसे महावीर भी काश्यप हैं - यह स्पष्टीकरण है।
दशवकालिक मूलमें (२०४०, पृ०७६) 'सब्वे देवा सब्वे असुरा' यह प्रयोग है। तथा 'देवा जक्खा य गुग्मगा' यह भी है९-२.१०। यह सूचित करता है कि देवोंके जो चार प्रकार तत्त्वार्थ में (४.१) हैं वे स्थिर होनेके पूर्वके ये प्रयोग हैं। आचार्य अगस्त्यसिंहकी व्याख्या (पृ०७७) भी यहां देखी जा सकती है जहाँ कहा गया है कि असुर ये देवोंके प्रतिपक्षी हैं। जब तत्त्वार्थ में असुर देवों के अन्तर्गत हैं। तथा देवा इत्यादिकी व्याख्या करने में आचार्य अगस्त्यको कठीनाई पडी है। यह सूचित करता है कि देवविमाग जो तत्त्वार्थमें है वह अभी स्थिर नहीं हुआ था।
__ वृद्धविवरण तथा भाचार्य हरिभद्रमें मृषाके चार भेद किये हैं जबकि प्रस्तुत चूर्णिमें तीन भेद है, यह सूचित करता है कि सम्भवतः यह चूर्णि वृद्धविवरणसे प्राचीन हो-पृ० ८२ तथा टिप्पण नं. ७
ज्ञानाचारका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्राकृतभाषानिबद्ध सूत्र का संस्कृतमें रूपान्तर नहीं करना चाहिए क्यों कि व्यञ्जनमें विसंवाद करने पर अर्थविसंवाद होता है। परिणामस्वरूप अंततः दीक्षाकी निरर्थकता हो जाती है-पृ० ५३ । प्राकृतके लिए 'अपभ्रश' शब्दका प्रयोग किया गया है-पृ०७। आगम-प्राकृतमें होने से कुछ लोग जो आपत्ति करते थे उसका भी निर्देश है-"सन्धमेतं पागतभासानिबद्धत्तणेण [ण] कुसलकल्पितं होज्जा"-पृ०५०"।
सिद्धसेनके सन्मतिकी गाथा' उद्धृत होने से वह भी प्रस्तुतसे पूर्वकी रचना सिद्ध होती है-गृ०२२॥
'रात्रिभोजनविरमण'व्रतको मूलगुण माना जाय या उत्तरगुण १ इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि यह उत्तरगुण ही है किन्तु सर्वमूलगुणकी रक्षाका हेतु होनेसे मूलगुणके साथ कहा गया है-पृ०८६। वृद्धविवरणमें उत्तरगुण तो माना है किन्तु वह प्रथम-अंतिम तीर्थकर के समयके पुरुष-विशेषकी अपेक्षासे ही तथा बीचके तीर्थंकरोंके समयमें तो सभीकी अपेक्षासे उत्तरगुण है-देखें प्रस्तुत पृ०८६ की टिप्पणी ६। इससे स्पष्ट है कि यह व्रत बादमें जोडा गया है।
मूलमें यह बात कही गई है कि वस्त्रपात्रादि संयम और लज्जाके लिए रखे जाते हैं अत एव वह परिग्रहमें शामिल नहीं है-मूर्छा ही परिग्रह है-(६-१९-२१)। इसकी चूर्णिमें 'चोलपट्टगादि'का उल्लेख है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि-"ण केवलं संघयणहीणाणं जिणकप्पियाण वि भगवतैवोपदिष्टम् "-पृ० १४७। और भी "उवधी वत्थायोहरणाति, सन्वस्थ उपधिणा सह सोपकरणा बुद्धा जिणा, साभाविक्रमिदं जिणलिंगमिति सम्वे वि एगदूसेण निमाता। पत्तेयबुद्धजिणकप्पियादयो वि रयहरणमुहणंतगातिणा सह संजमसारक्खणत्ये परिगाहेण मुच्छानिमित्ते तम्मि विजमाणे वि ते भगवंतो मुच्छं न गच्छंतीति अपरिगाहा"-पृ० १४८।।
दशवकालिककारको यह भी इष्ट है कि कोई साधु नम भी रह सकता है देखें-६.६४, पृ० १५७ । अत एव यह ग्रन्थ यापनीय संघके भिक्षु जो नम रहते थे उन्हें भी मान्य हुआ है। तभी तो यापनीय आचार्य अपराजितने इस की टीका भी लिखी है।
नियुक्ति में प्रशस्त-अप्रशस्त राग आदि की जो चर्चा है उसकी चूर्णि देखने लायक है। इसमें तीर्थंकरोंकी पूजाके समय वाद्यादि तथा नाटक आदिमें जो मन लगता है वह प्रास्त इन्द्रियरागका दृष्टान्त है तथा जैन शासनके विरोधीके प्रति जो क्रोध होता है, परवादिका पराभव होने पर जो अभिमान होता है, अभिमानसे संयममें उद्युक्त होने पर जो मान होता है, परवादीको हरानेकी दृष्टिसे जो छलप्रपंच किया जाता है वह माया, श्रुतज्ञान के लिए जो असन्तोष होता है वह लोभ-ये सब प्रशस्त प्रणिधिके उदाहरण हैं।-पृ० १८२-१८३ । दृष्टिवाद वस्तुतः था नहीं केवल कालनिक ग्रन्थ है-ऐसी मान्यतावालों के लिए दशवैकालिककी यह गाथा नया प्रकाश देगी
“आयारपण्णत्तिधरं दिट्टिवादमधिज्जगं।" ८.४९. . प्रस्तुतमें चूर्णिमें आचारधर, पण्णत्तिधर, और दिद्धिवादमायणधर का उल्लेख है जो दृष्टिवादके अस्तित्वको सूचित करता है इतना ही नहीं किन्तु आगोंमें उसके महत्त्वको भी सूचित करता है -पृ० १९७१
धर्मकी व्यवहारिकताका समर्थन यह कह कर किया गया है कि अनंत ज्ञानी भी गुरुकी उपासना अवश्य करे-दशवै० ९. १. ११, पृ० २०९। यहां चूर्णिकारने अनंत शब्दका पारिभाषिक ही अर्थ लिया है-अर्थात् सर्वज्ञ भी।
१. यह गाथा दशवैकालिकनियुक्तिकी हरिभद्रकी टीकामें भी नियुक्तिरूपसे ली गई है- गा०६० २. मूलाचारमें भी इसे मूलगुण माना नहीं गया-देखो गा० २-३ (मूलगुणाधिकार)
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org