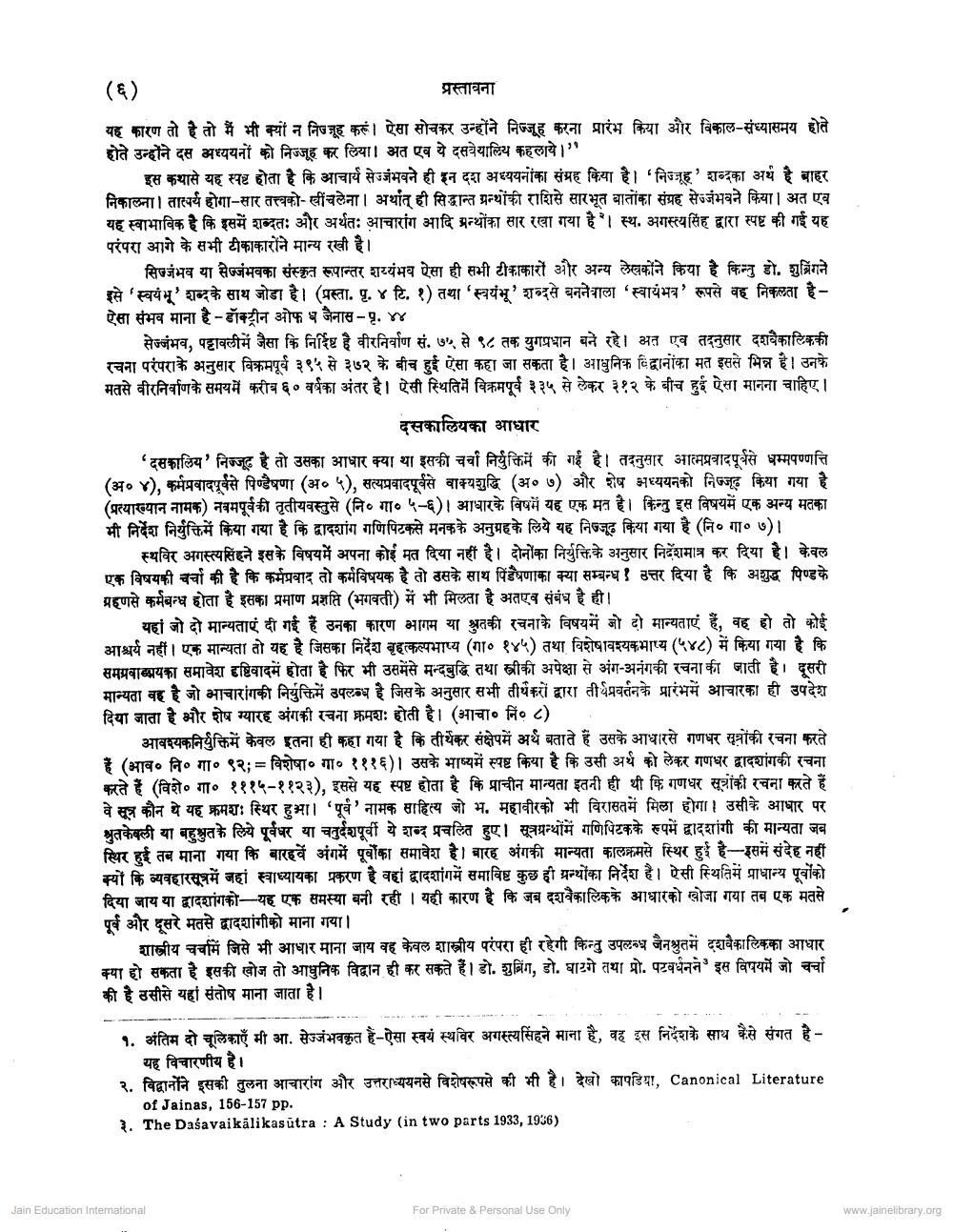________________
(६)
प्रस्तावना यह कारण तो है तो मैं भी क्यों न नितह करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने निज्जूह करना प्रारंभ किया और विकाल-संध्यासमय होते होते उन्होंने दस अध्ययनों को निज्जूह कर लिया। अत एव ये दसवेयालिय कहलाये।"
इस कथासे यह स्पष्ट होता है कि आचार्य सेज्जभवने ही इन दश अध्ययनोंका संग्रह किया है। 'निज्जूह' शब्दका अर्थ है बाहर निकालना। तात्पर्य होगा-सार तत्त्वको-खींचलेना। अर्थात् ही सिद्धान्त ग्रन्थोंकी राशिसे सारभूत बातोंका संग्रह सेज्जभवने किया। अत एव यह स्वाभाविक है कि इसमें शब्दतः और अर्थतः आचारांग आदि ग्रन्थोंका सार रखा गया है । स्थ. अगस्त्यसिंह द्वारा स्पष्ट की गई यह परंपरा आगे के सभी टीकाकारोंने मान्य रखी है।
सिज्जंभव या सज्जभवका संस्कृत रूपान्तर शय्यंभव ऐसा ही सभी टीकाकारों और अन्य लेखकोंने किया है किन्तु डो. शुब्रिगने इसे 'स्वयंभू' शब्दके साथ जोडा है। (प्रस्ता. पृ.४ टि. १) तथा 'स्वयंभू' शब्दसे बननेवाला 'स्वायंभव' रूपसे वह निकलता हैऐसा संभव माना है -डॉक्ट्रीन ओफ ध जैनास-पृ. ४४
सेज्जंभव, पट्टावलीमें जैसा कि निर्दिष्ट है वीरनिर्वाण सं. ७५ से ९८ तक युगप्रधान बने रहे। अत एव तदनुसार दशवकालिककी रचना परंपराके अनुसार विक्रमपूर्व ३९५ से ३७२ के बीच हुई ऐसा कहा जा सकता है। आधुनिक विद्वानोंका मत इससे भिन्न है। उनके मतसे वीरनिर्वाणके समयमें करीब ६० वर्षका अंतर है। ऐसी स्थिति, विक्रमपूर्व ३३५ से लेकर ३१२ के बीच हुई ऐसा मानना चाहिए ।
दसकालियका आधार 'दसकालिय' निज्जूद है तो उसका आधार क्या था इसकी चर्चा नियुक्तिमें की गई है। तदनुसार आत्मप्रवादपूर्वसे धम्मपण्णत्ति (अ. ४), कर्मप्रवादपूर्वसे पिण्डैषणा (अ०५), सत्यप्रवादपूर्वसे वाक्य शुद्धि (अ०७) और शेष अध्ययनको निज्जूद किया गया है (प्रत्याख्यान नामक) नवमपूर्वकी तृतीयवस्तुसे (नि० गा०५-६)। आधारके विषमें यह एक मत है। किन्तु इस विषयमें एक अन्य मतका भी निर्देश नियुक्तिमें किया गया है कि द्वादशांग गणिपिटकसे मनकके अनुग्रहके लिये यह निज्जूद किया गया है (नि० गा० ७)।
__ स्थविर अगस्त्यसिंहने इसके विषयमें अपना कोई मत दिया नहीं है। दोनोंका नियुक्ति के अनुसार निर्देशमात्र कर दिया है। केवल एक विषयकी चर्चा की है कि कर्मप्रवाद तो कर्मविषयक है तो उसके साथ पिंडैषणाका क्या सम्बन्ध ? उत्तर दिया है कि अशुद्ध पिण्डके ग्रहणसे कर्मबन्ध होता है इसका प्रमाण प्रज्ञप्ति (भगवती) में भी मिलता है अतएव संबंध है ही।
यहां जो दो मान्यताएं दी गई हैं उनका कारण भागम या श्रुतकी रचनाके विषयमें जो दो मान्यताएं हैं, वह हो तो कोई आश्चर्य नहीं। एक मान्यता तो यह है जिसका निर्देश बृहत्कल्पभाष्य (गा० १४५) तथा विशेषावश्यकभाष्य (५४८) में किया गया है कि समग्रवाङ्मयका समावेश दृष्टिवादमें होता है फिर भी उसमेंसे मन्दबुद्धि तथा स्त्रीकी अपेक्षा से अंग-अनंगकी रचना की जाती है। दूसरी मान्यता वह है जो भाचारांगकी नियुक्तिमें उपलब्ध है जिसके अनुसार सभी तीर्थंकरों द्वारा तीर्थप्रवर्तनके प्रारंभमें आचारका ही उपदेश दिया जाता है और शेष ग्यारह अंगकी रचना क्रमशः होती है। (आचा०नि०८)
आवश्यकनियुक्तिमें केवल इतना ही कहा गया है कि तीर्थकर संक्षेपमें अर्थ बताते हैं उसके आधारसे गणधर सूत्रोंकी रचना करते हैं (आव०नि० गा० ९२ = विशेषा. गा० १११६)। उसके भाष्यमें स्पष्ट किया है कि उसी अर्थ को लेकर गणधर द्वादशांगकी रचना करते हैं (विशे० गा० १११५-११२३), इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन मान्यता इतनी ही थी कि गणधर सूत्रोंकी रचना करते हैं वे सूत्र कौन थे यह क्रमशः स्थिर हुभा। 'पूर्व' नामक साहित्य जो भ. महावीरको भी विरासतमें मिला होगा। उसीके आधार पर श्रुतकेवली या बहुश्रुतके लिये पूर्वधर या चतुर्दशपूर्वी ये शन्द प्रचलित हुए। सूत्रग्रन्थोंमें गणिपिटकके रूपमें द्वादशांगी की मान्यता जब स्थिर हुई तब माना गया कि बारहवें अंगमें पूर्वोका समावेश है। बारह अंगकी मान्यता कालक्रमसे स्थिर हुई है-इसमें संदेह नहीं क्यों कि व्यवहारसूत्र में जहां स्वाध्यायका प्रकरण है वहां द्वादशांगमें समाविष्ट कुछ ही ग्रन्थोंका निर्देश है। ऐसी स्थितिम प्राधान्य पूर्वोको दिया जाय या द्वादशांगको-यह एक समस्या बनी रही । यही कारण है कि जब दशवैकालिकके आधारको खोजा गया तब एक मतसे पूर्व और दूसरे मतसे द्वादशांगीको माना गया।
शास्त्रीय चर्चामें जिसे भी आधार माना जाय वह केवल शास्त्रीय परंपरा ही रहेगी किन्तु उपलब्ध जैनश्रुतमें दशवैकालिकका आधार क्या हो सकता है इसकी खोज तो आधुनिक विद्वान ही कर सकते हैं। डो. शुकिंग, डो. घाटगे तथा प्रो. पटवर्धनने इस विषयमें जो चर्चा की है उसीसे यहां संतोष माना जाता है।
१. अंतिम दो चूलिकाएँ मी आ. सेज्जंभवकृत है-ऐसा स्वयं स्थविर अगस्त्यसिंहने माना है, वह इस निर्देशके साथ कैसे संगत है
यह विचारणीय है। २. विद्वानोंने इसकी तुलना आचारांग और उत्तराध्ययनसे विशेषरूपसे की भी है। देखो कापडिया, Canonical Literature
of Jainas, 156-157 pp. ३. The Dasavaikalikasutra : A Study (in two parts 1933, 1936)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org