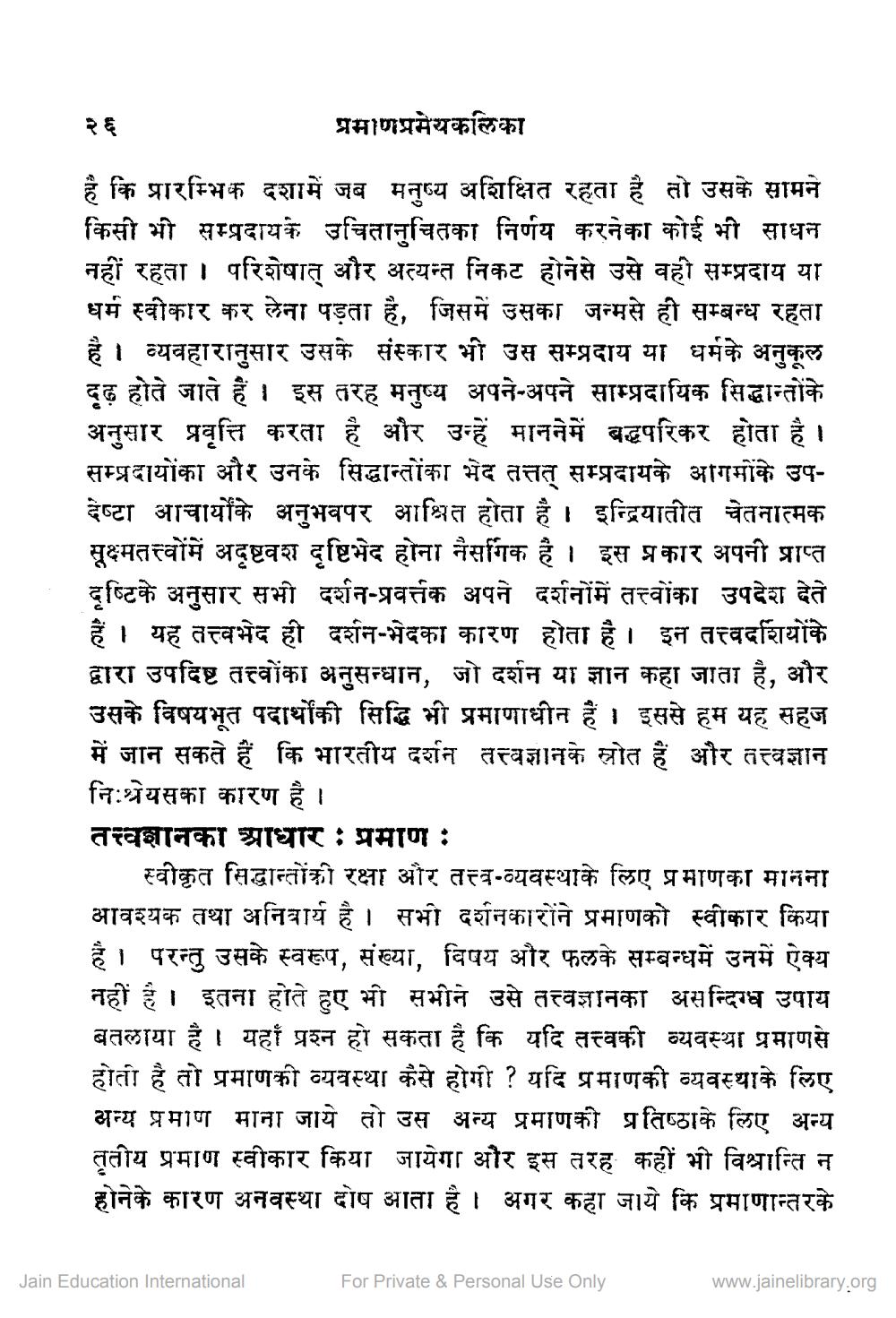________________
प्रमाणप्रमेयकलिका
है कि प्रारम्भिक दशामें जब मनुष्य अशिक्षित रहता है तो उसके सामने किसी भी सम्प्रदायके उचितानचितका निर्णय करनेका कोई भी साधन नहीं रहता। परिशेषात् और अत्यन्त निकट होनेसे उसे वही सम्प्रदाय या धर्म स्वीकार कर लेना पड़ता है, जिसमें उसका जन्मसे ही सम्बन्ध रहता है। व्यवहारानुसार उसके संस्कार भी उस सम्प्रदाय या धर्मके अनुकूल दढ़ होते जाते हैं। इस तरह मनुष्य अपने-अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तोंके अनुसार प्रवृत्ति करता है और उन्हें माननेमें बद्धपरिकर होता है । सम्प्रदायोंका और उनके सिद्धान्तोंका भेद तत्तत् सम्प्रदायके आगमोंके उपदेष्टा आचार्योंके अनुभवपर आश्रित होता है। इन्द्रियातीत चेतनात्मक सूक्ष्मतत्त्वोंमें अदृष्टवश दृष्टिभेद होना नैसर्गिक है। इस प्रकार अपनी प्राप्त दृष्टिके अनुसार सभी दर्शन-प्रवर्तक अपने दर्शनोंमें तत्त्वोंका उपदेश देते हैं । यह तत्त्वभेद ही दर्शन-भेदका कारण होता है। इन तत्त्वदर्शियोंके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंका अनुसन्धान, जो दर्शन या ज्ञान कहा जाता है, और उसके विषयभूत पदार्थोंकी सिद्धि भी प्रमाणाधीन हैं। इससे हम यह सहज में जान सकते हैं कि भारतीय दर्शन तत्त्वज्ञानके स्रोत हैं और तत्त्वज्ञान निःश्रेयसका कारण है। तत्त्वज्ञानका आधार: प्रमाण :
स्वीकृत सिद्धान्तोंकी रक्षा और तत्त्व-व्यवस्थाके लिए प्रमाणका मानना आवश्यक तथा अनिवार्य है। सभी दर्शनकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्तु उसके स्वरूप, संख्या, विषय और फलके सम्बन्धमें उनमें ऐक्य नहीं है। इतना होते हुए भी सभीने उसे तत्त्वज्ञानका असन्दिग्ध उपाय बतलाया है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि तत्त्वकी व्यवस्था प्रमाणसे होती है तो प्रमाणकी व्यवस्था कैसे होगी ? यदि प्रमाणकी व्यवस्थाके लिए अन्य प्रमाण माना जाये तो उस अन्य प्रमाणको प्रतिष्ठाके लिए अन्य तृतीय प्रमाण स्वीकार किया जायेगा और इस तरह कहीं भी विश्रान्ति न होनेके कारण अनवस्था दोष आता है। अगर कहा जाये कि प्रमाणान्तरके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org