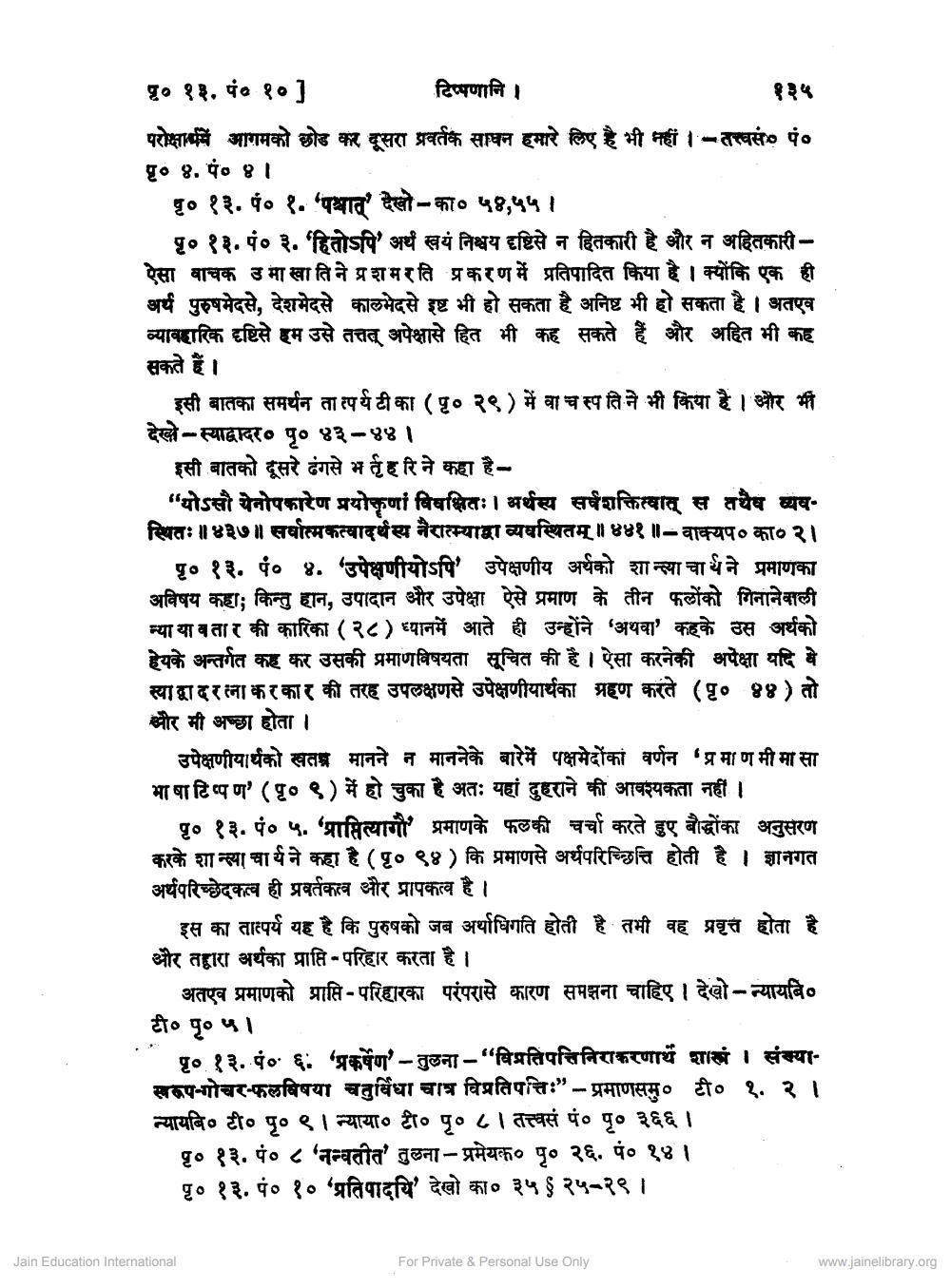________________
पृ० १३. पं० १०] टिप्पणानि । परोक्षायें आगमको छोड कर दूसरा प्रवर्तक साधन हमारे लिए है भी नहीं । - तत्त्वसं० पं० पृ० ४. पं० ४।
पृ० १३. पं० १. 'पश्चात् देखो-का० ५४,५५।
पृ० १३. पं० ३. 'हितोऽपि' अर्थ स्वयं निश्चय दृष्टिसे न हितकारी है और न अहितकारीऐसा वाचक उमा खा ति ने प्रशमरति प्रकरण में प्रतिपादित किया है । क्योंकि एक ही अर्थ पुरुषमेदसे, देशभेदसे कालभेदसे इष्ट भी हो सकता है अनिष्ट भी हो सकता है । अतएव व्यावहारिक दृष्टि से हम उसे तत्तत् अपेक्षासे हित भी कह सकते हैं और अहित भी कह सकते हैं।
इसी बातका समर्थन तात्पर्य टीका (पृ० २९) में वा च स्पति ने भी किया है । और भी देखो-स्याद्वादर० पृ० ४३-४४।।
इसी बातको दूसरे ढंगसे भर्तृहरि ने कहा है
"योऽसौ येनोपकारेण प्रयोक्तृणां विवक्षितः। अर्थस्य सर्वशक्तिस्वात् स तथैव व्यवस्थितः॥४३७॥ सर्वात्मकत्वादर्थस्य नैरात्म्यावा व्यवस्थितम् ॥४४१॥-वाक्यप० का०२।
पृ० १३. पं० ४. 'उपेक्षणीयोऽपि' उपेक्षणीय अर्थको शान्त्या चार्थ ने प्रमाणका अविषय कहा; किन्तु हान, उपादान और उपेक्षा ऐसे प्रमाण के तीन फलोंको गिनानेवाली न्या या वतार की कारिका (२८) ध्यानमें आते ही उन्होंने 'अथवा' कहके उस अर्थको हेयके अन्तर्गत कह कर उसकी प्रमाणविषयता सूचित की है । ऐसा करनेकी अपेक्षा यदि थे स्याद्वादरत्नाकर कार की तरह उपलक्षणसे उपेक्षणीयार्थका ग्रहण करते (पृ. १४) तो और भी अच्छा होता।
उपेक्षणीयार्थको खतन्त्र मानने न माननेके बारेमें पक्षमेदोंका वर्णन 'प्रमाण मी मा सा भाषा टिप्पण' (पृ०९) में हो चुका है अतः यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं ।
पृ० १३. पं० ५. 'प्राप्तित्यागौं' प्रमाणके फलकी चर्चा करते हुए बौद्धोंका अनुसरण करके शान्त्या चार्य ने कहा है (पृ० ९४) कि प्रमाणसे अर्थपरिच्छित्ति होती है । ज्ञानगत अर्थपरिच्छेदकत्व ही प्रवर्तकत्व और प्रापकत्व है ।
इस का तात्पर्य यह है कि पुरुषको जब अर्थाधिगति होती है तभी वह प्रवृत्त होता है और तहारा अर्थका प्राप्ति -परिहार करता है ।
अतएव प्रमाणको प्राप्ति - परिहारका परंपरासे कारण समझना चाहिए । देखो-न्यायबि० टी० पृ० ५।
पृ० १३. पं०. ६: 'प्रकर्षण' - तुलना- "विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थ शास्त्र । संख्याखरूप-गोचर-फलविषया चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः" - प्रमाणसमु० टी० १. २ । न्यायबि० टी० पृ० ९ । न्याया० टी० पृ० ८। तत्त्वसं पं० पृ० ३६६ ।
पृ० १३. पं० ८ 'नन्वतीत' तुलना- प्रमेयक० पृ० २६. पं० १४ । पृ० १३. पं० १० 'प्रतिपादयि' देखो का० ३५ ६ २५-२९ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org