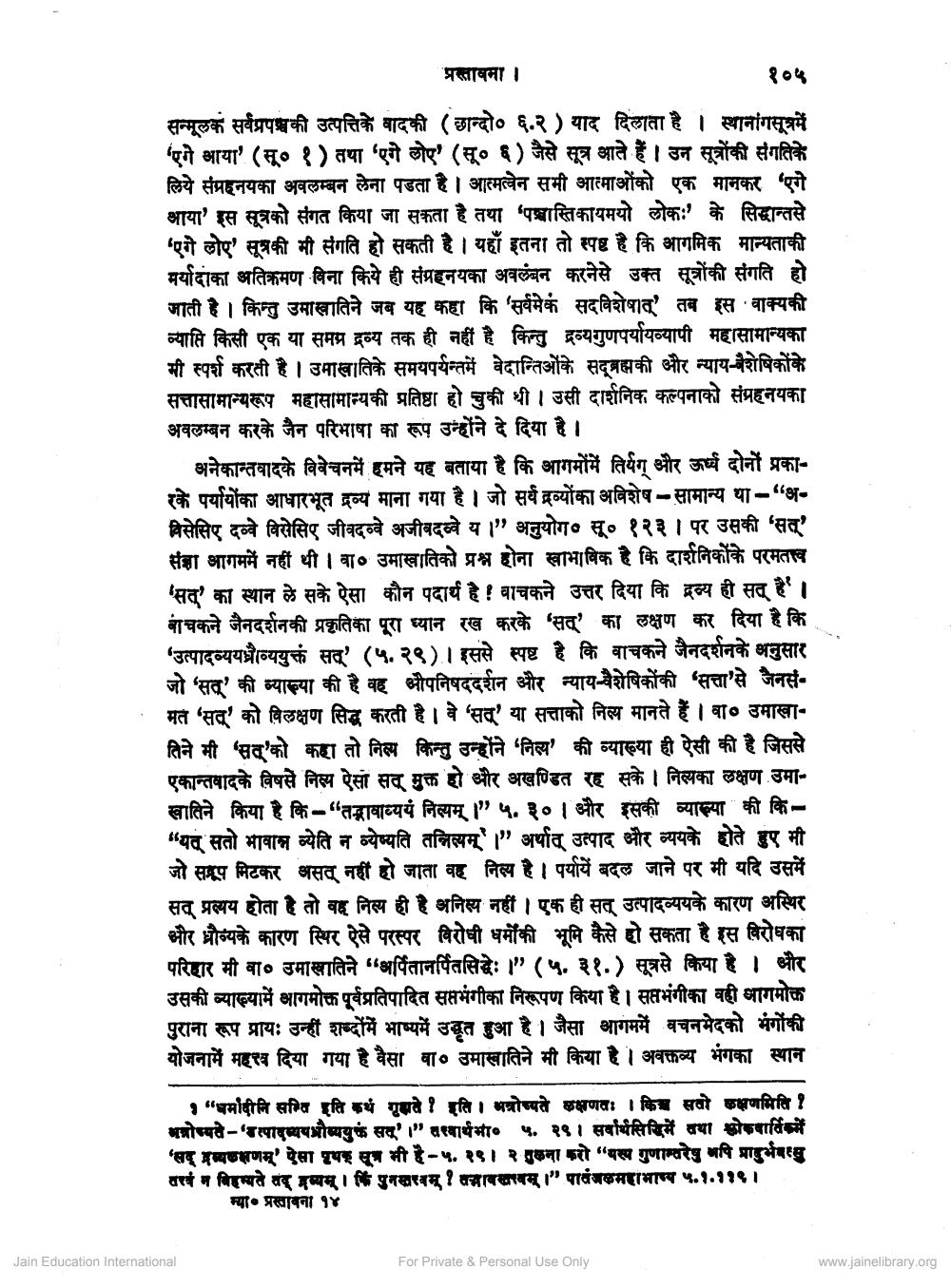________________
प्रस्तावमा।
सन्मूलकं सर्वप्रपश्चकी उत्पत्तिके वादकी (छान्दो० ६.२ ) याद दिलाता है । स्थानांगसूत्रमें 'एगे आया' (सू०१) तथा 'एगे लोए' (सू० ६) जैसे सूत्र आते हैं। उन सूत्रोंकी संगतिके लिये संग्रहनयका अवलम्बन लेना पडता है। आत्मत्वेन समी आत्माओंको एक मानकर 'एगे आया' इस सूत्रको संगत किया जा सकता है तथा 'पश्चास्तिकायमयो लोकः' के सिद्धान्तसे 'एगे लोए' सूत्रकी मी संगति हो सकती है । यहाँ इतना तो स्पष्ट है कि आगमिक मान्यताकी मर्यादाका अतिक्रमण विना किये ही संग्रहनयका अवलंबन करनेसे उक्त सूत्रोंकी संगति हो जाती है। किन्तु उमाखातिने जब यह कहा कि 'सर्वमेकं सदविशेषात्' तब इस · वाक्यकी व्याप्ति किसी एक या समग्र द्रव्य तक ही नहीं है किन्तु द्रव्यगुणपर्यायव्यापी महासामान्यका मी स्पर्श करती है । उमाखातिके समयपर्यन्तमें वेदान्तिओंके सद्ब्रह्मकी और न्याय-वैशेषिकोंके सत्तासामान्यरूप महासामान्यकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसी दार्शनिक कल्पनाको संग्रहनयका अवलम्बन करके जैन परिभाषा का रूप उन्होंने दे दिया है।
अनेकान्तवादके विवेचनमें हमने यह बताया है कि आगमोंमें तिर्यग् और ऊर्ध्व दोनों प्रकारके पर्यायोंका आधारभूत द्रव्य माना गया है । जो सर्य द्रव्योंका अविशेष- सामान्य था-"अविसेसिए दव्वे विसेसिए जीवदवे अजीबव्वे य ।" अनुयोग० सू० १२३ । पर उसकी 'सत्' संज्ञा आगममें नहीं थी । वा० उमास्त्रातिको प्रश्न होना स्वाभाविक है कि दार्शनिकोंके परमतत्त्व 'सत्' का स्थान ले सके ऐसा कौन पदार्थ है ! वाचकने उत्तर दिया कि द्रव्य ही सत् है। बाचकने जैनदर्शनकी प्रकृतिका पूरा ध्यान रख करके 'सत्' का लक्षण कर दिया है कि 'उत्पादन्ययङ्ग्रीव्ययुक्तं सत्' (५.२९) । इससे स्पष्ट है कि वाचकने जैनदर्शनके अनुसार जो 'सत्' की व्याख्या की है वह औपनिषददर्शन और न्याय-वैशेषिकोंकी 'सत्ता से जैनसंमत 'सत्' को विलक्षण सिद्ध करती है। वे 'सत्' या सत्ताको नित्य मानते हैं। वा० उमाखातिने मी 'सत्'को कहा तो निस किन्तु उन्होंने 'नित्य' की व्याख्या ही ऐसी की है जिससे एकान्तवादके विषसे नित्य ऐसा सत् मुक्त हो और अखण्डित रह सके । नित्यका लक्षण उमाखातिने किया है कि-"तदावाव्ययं नित्यम् ।" ५.३० । और इसकी व्याख्या की कि"यत् सतो भावान्न व्येति न व्येष्यति तन्नित्यम्।" अर्थात् उत्पाद और व्ययके होते हुए भी जो सप मिटकर असत् नहीं हो जाता वह नित्य है । पर्यायें बदल जाने पर मी यदि उसमें सत् प्रत्यय होता है तो वह नित्य ही है अनिस्य नहीं । एक ही सत् उत्पादव्ययके कारण अस्थिर और धौव्यके कारण स्थिर ऐसे परस्पर विरोधी धर्मोकी भूमि कैसे हो सकता है इस विरोधका परिहार मी वा० उमाखातिने "अर्पितानर्पितसिद्धेः।" (५. ३१.) सूत्रसे किया है । और उसकी व्याख्या आगमोक्त पूर्वप्रतिपादित सप्तभंगीका निरूपण किया है । सप्तभंगीका वही भागमोक्त पुराना रूप प्रायः उन्हीं शब्दोंमें भाष्यमें उबृत हुआ है। जैसा आगममें बचनभेदको भंगोंकी योजनामें महत्व दिया गया है वैसा वा० उमाखातिने भी किया है। अवक्तव्य भंगका स्थान
"धर्मादीनि सन्ति इति कथं गृह्यते इति । अत्रोच्यते लक्षणतः । किड सवो लक्षणमिति अनोग्यते-'यस्पायव्ययौव्ययुकं सत्" स्वार्थमा. ५. २९। सर्वार्थसिरिमें क्या सोकवार्तिकमें 'सद्मबक्षणम्' ऐसा पृषक सूत्र भी है-५. १९। २ तुलना करो "यस गुणान्तरेषु अपि प्रादुर्भवसु तर म बिहन्यते तद्व्य म् । किं पुनरवम् वनावखवम् ।" पातंजलमहाभाग्य ५....।
म्या. प्रस्तावना १४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org