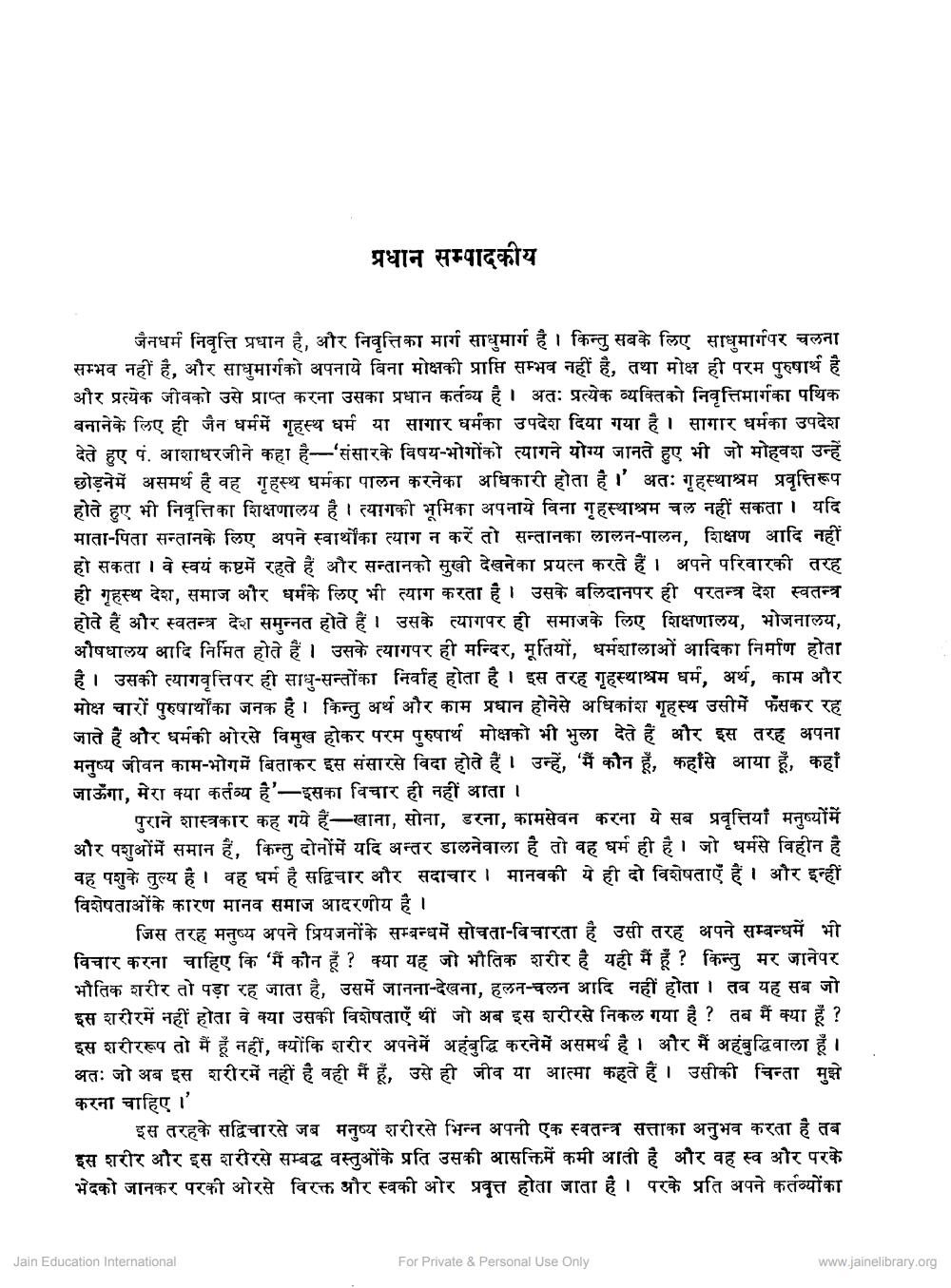________________
प्रधान सम्पादकीय
जैनधर्म निवृत्ति प्रधान है, और निवृत्तिका मार्ग साधुमार्ग है। किन्तु सबके लिए साधुमार्गपर चलना सम्भव नहीं है, और साधुमार्गको अपनाये बिना मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, तथा मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है
और प्रत्येक जीवको उसे प्राप्त करना उसका प्रधान कर्तव्य है। अतः प्रत्येक व्यक्तिको निवृत्तिमार्गका पथिक बनानेके लिए ही जैन धर्ममें गृहस्थ धर्म या सागार धर्मका उपदेश दिया गया है। सागार धर्मका उपदेश देते हए पं. आशाधरजीने कहा है-'संसारके विषय-भोगोंको त्यागने योग्य जानते हुए भी जो मोहवश उन्हें छोड़नेमें असमर्थ है वह गृहस्थ धर्मका पालन करनेका अधिकारी होता है।' अतः गृहस्थाश्रम प्रवृत्तिरूप होते हुए भी निवृत्तिका शिक्षणालय है । त्यागको भूमिका अपनाये विना गृहस्थाश्रम चल नहीं सकता। यदि माता-पिता सन्तानके लिए अपने स्वार्थोंका त्याग न करें तो सन्तानका लालन-पालन, शिक्षण आदि नहीं हो सकता। वे स्वयं कष्टमें रहते हैं और सन्तानको सुखी देखने का प्रयत्न करते हैं। अपने परिवारकी तरह ही गृहस्थ देश, समाज और धर्मके लिए भी त्याग करता है। उसके बलिदानपर ही परतन्त्र देश स्वतन्त्र होते हैं और स्वतन्त्र देश समुन्नत होते हैं। उसके त्यागपर ही समाजके लिए शिक्षणालय, भोजनालय,
औषधालय आदि निर्मित होते हैं। उसके त्यागपर ही मन्दिर, मूर्तियों, धर्मशालाओं आदिका निर्माण होता है। उसकी त्यागवृत्तिपर ही साधु-सन्तोंका निर्वाह होता है। इस तरह गृहस्थाश्रम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों परुषार्थों का जनक है। किन्तु अर्थ और काम प्रधान होनेसे अधिकांश गहस्थ उसीमें फंसकर रह जाते हैं और धर्मकी ओरसे विमुख होकर परम पुरुषार्थ मोक्षको भी भुला देते हैं और इस तरह अपना मनुष्य जीवन काम-भोगमें बिताकर इस संसारसे विदा होते हैं। उन्हें, 'मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या कर्तव्य है'-इसका विचार ही नहीं आता ।
पुराने शास्त्रकार कह गये हैं-खाना, सोना, डरना, कामसेवन करना ये सब प्रवृत्तियां मनुष्योंमें और पशुओंमें समान है, किन्तु दोनोंमें यदि अन्तर डालनेवाला है तो वह धर्म ही है। जो धर्मसे विहीन है वह पशुके तुल्य है। वह धर्म है सद्विचार और सदाचार । मानवकी ये ही दो विशेषताएँ हैं। और इन्हीं विशेषताओंके कारण मानव समाज आदरणीय है।
जिस तरह मनुष्य अपने प्रियजनों के सम्बन्धमें सोचता-विचारता है उसी तरह अपने सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि 'मैं कौन हूँ? क्या यह जो भौतिक शरीर है यही मैं हूँ ? किन्तु मर जानेपर भौतिक शरीर तो पड़ा रह जाता है, उसमें जानना-देखना, हलन-चलन आदि नहीं होता। तब यह सब जो इस शरीरमें नहीं होता वे क्या उसकी विशेषताएँ थीं जो अब इस शरीरसे निकल गया है ? तब मैं क्या हूँ ? इस शरीररूप तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि शरीर अपने में अहंबुद्धि करने में असमर्थ है। और मैं अहंबुद्धिवाला हूँ। अतः जो अब इस शरीरमें नहीं है वही मैं हूँ, उसे ही जीव या आत्मा कहते हैं। उसीकी चिन्ता मुझे करना चाहिए।'
इस तरहके सद्विचारसे जब मनुष्य शरीरसे भिन्न अपनी एक स्वतन्त्र सत्ताका अनुभव करता है तब इस शरीर और इस शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओंके प्रति उसकी आसक्तिमें कमी आती है और वह स्व और परके भेदको जानकर परकी ओरसे विरक्त और स्वकी ओर प्रवृत्त होता जाता है। परके प्रति अपने कर्तव्योंका
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org