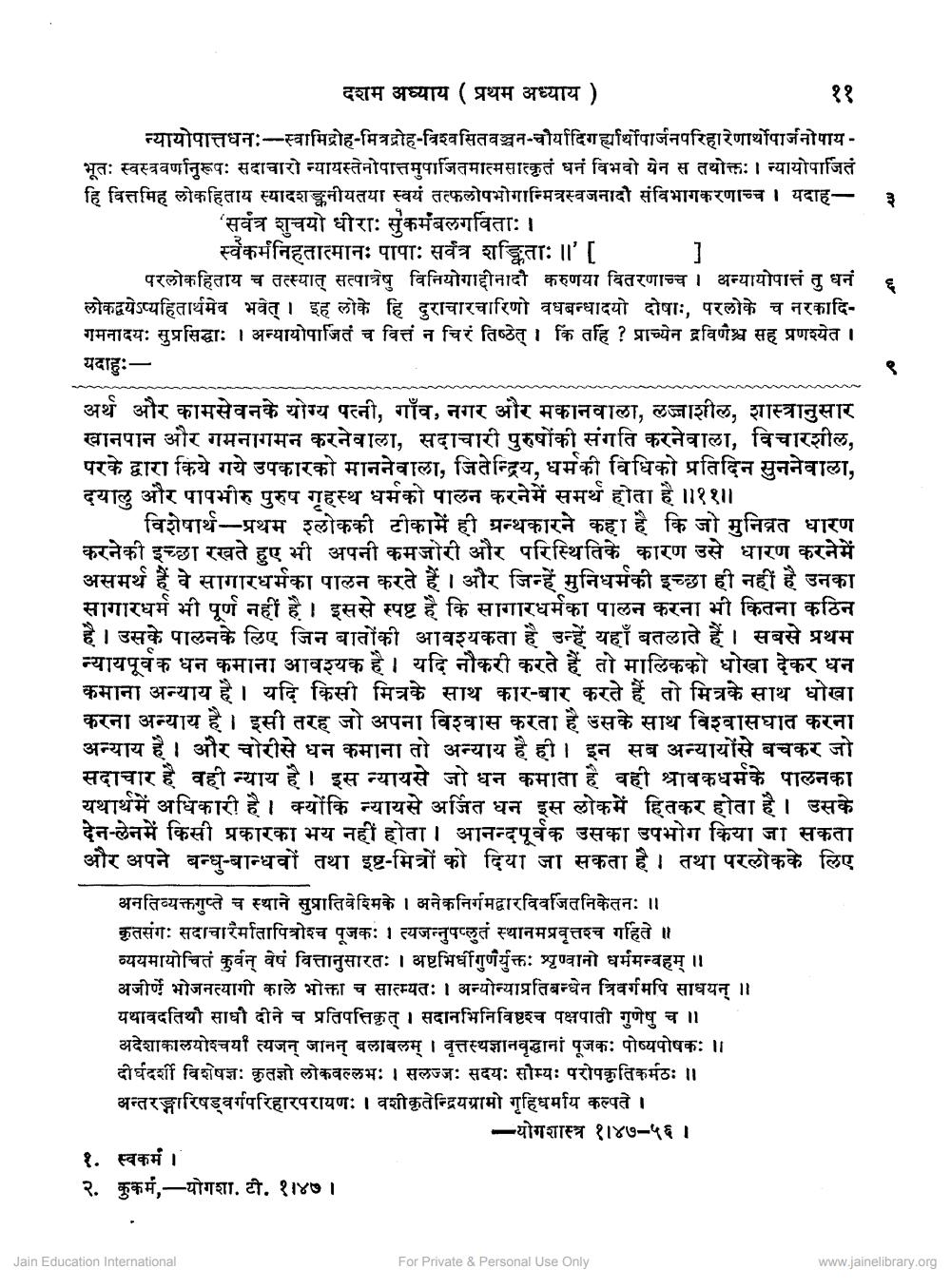________________
दशम अध्याय ( प्रथम अध्याय )
११
न्यायोपात्तधनः -- स्वामिद्रोह - मित्रद्रोह - विश्वसितवञ्चन- चौर्यादिग ह्यर्थोपार्जन परिहारेणार्थोपार्जनोपाय - भूतः स्वस्त्रवर्णानुरूपः सदाचारो न्यायस्तेनोपात्तमुपार्जितमात्मसात्कृतं धनं विभवो येन स तयोक्तः । न्यायोपार्जितं हि वित्तमिह लोकहिताय स्यादशङ्कनीयतया स्वयं तत्फलोपभोगान्मित्रस्वजनादौ संविभागकरणाच्च । यदाह— 'सर्वत्र शुचयो धीराः सुकम्बलगर्विताः ।
स्वैकर्मनिहतात्मानः पापाः सर्वत्र शङ्किताः ॥' [
]
६
परलोकहिताय च तत्स्यात् सत्पात्रेषु विनियोगाद्दीनादौ करुणया वितरणाच्च । अन्यायोपात्तं तु धनं लोकद्वयेऽप्यहितार्थमेव भवेत् । इह लोके हि दुराचारचारिणो वधबन्धादयो दोषाः, परलोके च नरकादि - गमनादयः सुप्रसिद्धाः । अन्यायोपार्जितं च वित्तं न चिरं तिष्ठेत् । किं तहि ? प्राच्येन द्रविणैश्च सह प्रणश्येत । यदाहुः -
अर्थ और कामसेवनके योग्य पत्नी, गाँव, नगर और मकानवाला, लज्जाशील, शास्त्रानुसार खानपान और गमनागमन करनेवाला, सदाचारी पुरुषोंकी संगति करनेवाला, विचारशील, परके द्वारा किये गये उपकारको माननेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मकी विधिको प्रतिदिन सुननेवाला, दयालु और पापभीरु पुरुष गृहस्थ धर्मको पालन करनेमें समर्थ होता है ॥११॥
विशेषार्थ - प्रथम श्लोककी टीकामें ही ग्रन्थकारने कहा है कि जो मुनिव्रत धारण करने की इच्छा रखते हुए भी अपनी कमजोरी और परिस्थितिके कारण उसे धारण करनेमें असमर्थ हैं वे सागारधर्मका पालन करते हैं । और जिन्हें मुनिधर्मकी इच्छा ही नहीं है उनका सागारधर्म भी पूर्ण नहीं है । इससे स्पष्ट है कि सागारधर्मका पालन करना भी कितना कठिन है | उसके पालन के लिए जिन बातोंकी आवश्यकता है उन्हें यहाँ बतलाते हैं । सबसे प्रथम न्यायपूर्वक धन कमाना आवश्यक है । यदि नौकरी करते हैं तो मालिकको धोखा देकर धन कमाना अन्याय है | यदि किसी मित्रके साथ कार-बार करते हैं तो मित्रके साथ धोखा करना अन्याय है । इसी तरह जो अपना विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करना अन्याय है । और चोरीसे धन कमाना तो अन्याय है ही । इन सब अन्यायोंसे बचकर जो सदाचार है वही न्याय है । इस न्यायसे जो धन कमाता है वही श्रावकधर्मके पालनका यथार्थ में अधिकारी है । क्योंकि न्याय से अर्जित धन इस लोक में हितकर होता है । उसके देन-लेन में किसी प्रकारका भय नहीं होता । आनन्दपूर्वक उसका उपभोग किया जा सकता और अपने बन्धुबान्धवों तथा इष्ट मित्रों को दिया जा सकता है । तथा परलोकके लिए
अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके । अनेक निर्गमद्वारविवर्जितनिकेतनः ॥ कृतसंगः सदाचारैर्मातापित्रोश्च पूजकः । त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्तश्च गर्हिते ॥
व्ययमायोचितं कुर्वन् वेषं वित्तानुसारतः । अष्टभिर्धीगुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्ममन्वहम् || अजीर्णे भोजनत्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः । अन्योन्याप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि साधयन् ॥ यथावदतिथो साधो दीने च प्रतिपत्तिकृत् । सदानभिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ अदेशाकालयोश्चर्यां त्यजन् जानन् बलाबलम् । वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ।। दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवल्लभः । सलज्जः सदयः सौम्यः परोपकृतिकर्मठः ॥ अन्तरङ्गारिषड्वर्गपरिहारपरायणः । वशीकृतेन्द्रियग्रामो गृहिधर्माय कल्पते ।
— योगशास्त्र १।४७-५६ ।
१. स्वकमं ।
२. कुकर्म, –योगशा. टी. ११४७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
३
www.jainelibrary.org