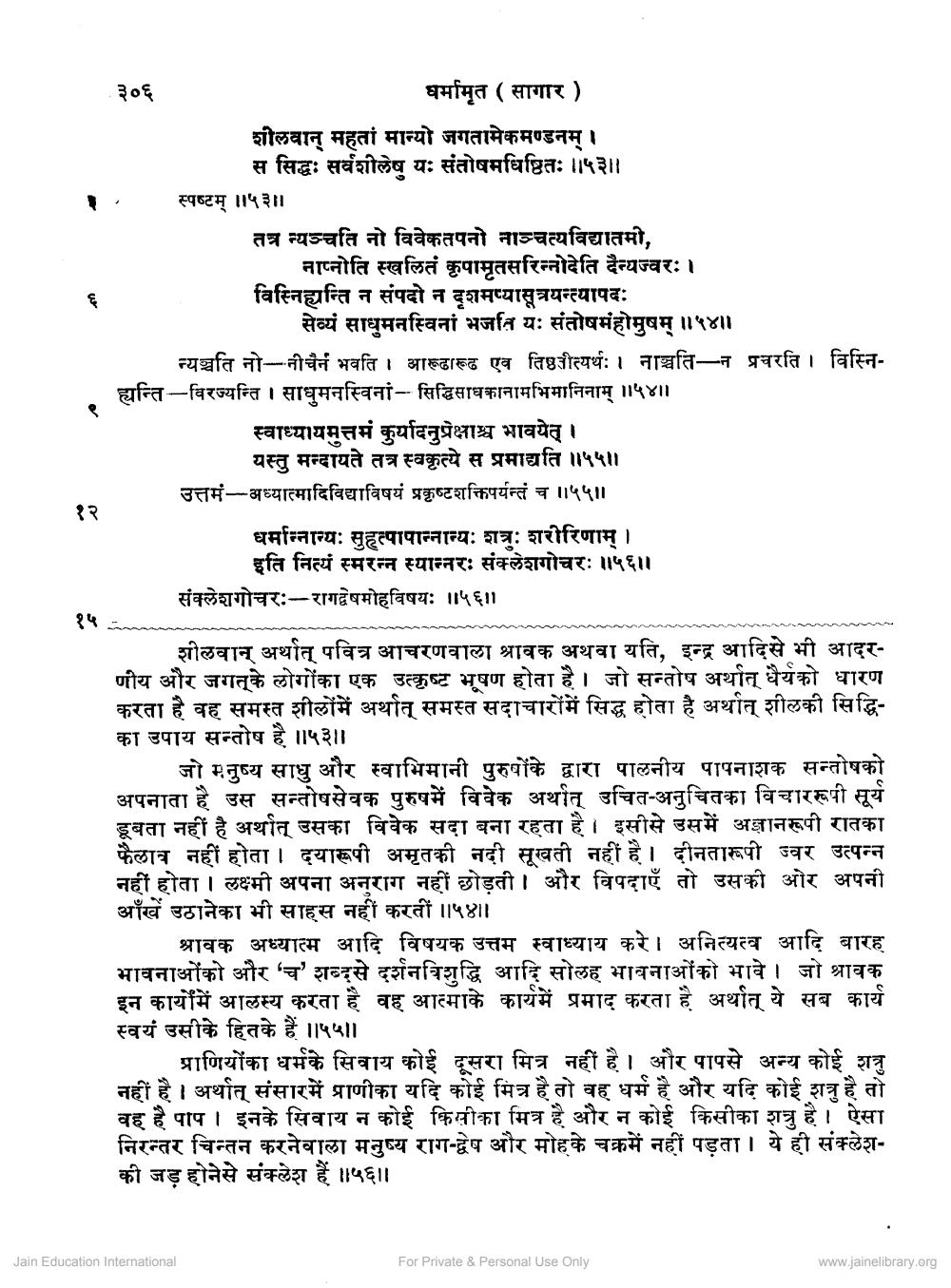________________
.३०६
धर्मामृत ( सागार ) शीलवान् महतां मान्यो जगतामेकमण्डनम् ।
स सिद्धः सर्वशीलेषु यः संतोषमधिष्ठितः ।।५३।। स्पष्टम् ॥५३॥
तत्र न्यञ्चति नो विवेकतपनो नाञ्चत्यविद्यातमी.
नाप्नोति स्खलितं कृपामृतसरिन्नोदेति दैन्यज्वरः। विस्निह्यन्ति न संपदो न दृशमप्यासूत्रयन्त्यापदः
सेव्यं साधुमनस्विनां भजति यः संतोषमंहोमुषम् ॥५४॥ न्यञ्चति नो-नीचैनं भवति । आरूढारूढ एव तिष्ठतीत्यर्थः । नाञ्चति-न प्रचरति । विस्नि. ह्यन्ति-विरज्यन्ति । साधुमनस्विनां- सिद्धिसाधकानामभिमानिनाम् ॥५४॥
स्वाध्यायमुत्तमं कुर्यादनुप्रेक्षाश्च भावयेत् ।
यस्तु मन्दायते तत्र स्वकृत्ये स प्रमाद्यति ॥५५॥ उत्तम-अध्यात्मादिविद्याविषयं प्रकृष्टशक्तिपर्यन्तं च ।।५५॥
धर्मान्नान्यः सुहृत्पापान्नान्यः शत्रः शरीरिणाम् ।
इति नित्यं स्मरन्न स्यान्नरः संक्लेशगोचरः ॥५६॥
संक्लेशगोचरः-रागद्वेषमोहविषयः ॥५६॥ १५ --~--
शीलवान अर्थात् पवित्र आचरणवाला श्रावक अथवा यति, इन्द्र आदिसे भी आदरणीय और जगत्के लोगोंका एक उत्कृष्ट भूषण होता है। जो सन्तोष अर्थात् धैय को धारण करता है वह समस्त शीलोंमें अर्थात् समस्त सदाचारोंमें सिद्ध होता है अर्थात शीलकी सिद्धिका उपाय सन्तोष है ॥५३॥
जो मनुष्य साधु और स्वाभिमानी पुरुषोंके द्वारा पालनीय पापनाशक सन्तोषको अपनाता है उस सन्तोषसेवक पुरुषमें विवेक अर्थात उचित-अनुचितका विचाररूपी सूर्य डूबता नहीं है अर्थात् उसका विवेक सदा बना रहता है। इसीसे उसमें अज्ञानरूपी रातका फैलाव नहीं होता। दयारूपी अमृतकी नदी सूखती नहीं है। दीनतारूपी ज्वर उत्पन्न नहीं होता । लक्ष्मी अपना अनुराग नहीं छोड़ती। और विपदाएँ तो उसकी ओर अपनी आँखें उठानेका भी साहस नहीं करतीं ।।५४॥
श्रावक अध्यात्म आदि विषयक उत्तम स्वाध्याय करे। अनित्यत्व आदि बारह भावनाओंको और 'च' शब्दसे दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंको भावे । जो श्रावक इन कार्यों में आलस्य करता है वह आत्माके कार्यमें प्रमाद करता है अर्थात् ये सब कार्य स्वयं उसीके हितके हैं ॥५५॥
प्राणियोंका धर्मके सिवाय कोई दूसरा मित्र नहीं है। और पापसे अन्य कोई शत्रु नहीं है। अर्थात् संसार में प्राणीका यदि कोई मित्र है तो वह धर्म है और यदि कोई शत्रु है तो वह है पाप । इनके सिवाय न कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका शत्रु है। ऐसा निरन्तर चिन्तन करनेवाला मनुष्य राग-द्वेष और मोहके चक्रमें नहीं पड़ता। ये ही संक्लेशकी जड़ होनेसे संक्लेश हैं ॥५६।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org