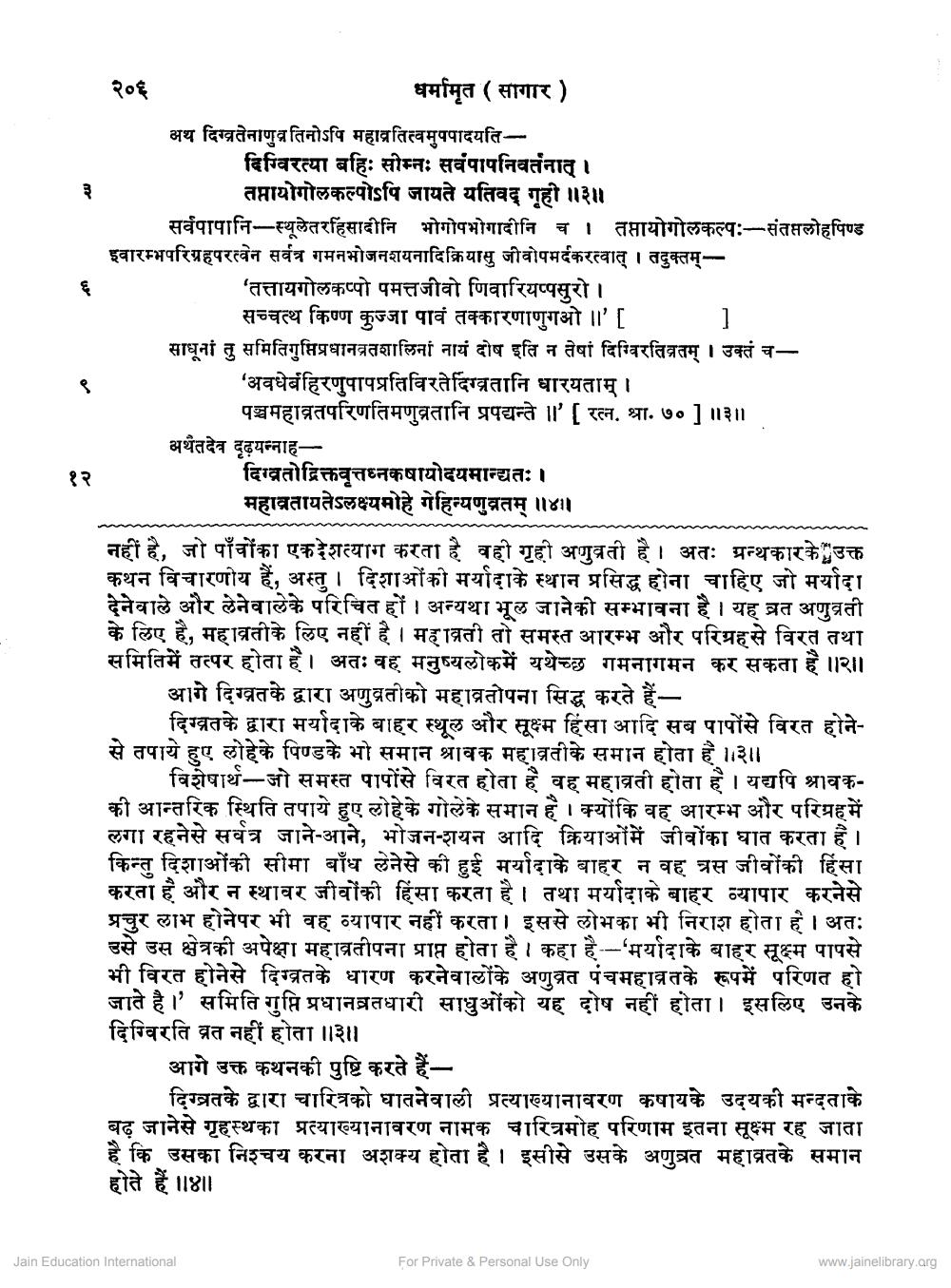________________
२०६
धर्मामृत ( सागार) अथ दिग्व्रतेनाणुन तिनोऽपि महाव्रतित्वमुपपादयति
दिग्विरत्या बहिः सोम्नः सर्वपापनिवर्तनात् ।
तप्तायोगोलकल्पोऽपि जायते यतिवद् गृही ॥३॥ सर्वपापानि-स्थूलेतरहिंसादीनि भोगोपभोगादीनि च । तप्तायोगोलकल्पः-संतप्तलोहपिण्ड इवारम्भपरिग्रहपरत्वेन सर्वत्र गमनभोजनशयनादिक्रियासु जीवोपमर्दकरत्वात् । तदुक्तम्
'तत्तायगोलकप्पो पमत्तजीवो णिवारियप्पसुरो।
सच्चत्थ किण्ण कुज्जा पावं तक्कारणाणुगओ ।' [ ] साधूनां तु समितिगुप्तिप्रधानव्रतशालिनां नायं दोष इति न तेषां दिग्विरतिव्रतम् । उक्तं च
'अवधेर्बहिरणुपापप्रतिविरतेदिग्वतानि धारयताम् ।
पञ्चमहाव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपद्यन्ते ॥' [ रत्न. श्रा. ७० ] ॥३॥ अथैतदेव दृढ़यन्नाह
दिग्वतोद्रिक्तवृत्तध्नकषायोदयमान्यतः।
महावतायतेऽलक्ष्यमोहे गेहिन्यणुव्रतम् ॥४॥ नहीं है, जो पाँचोंका एकदेशत्याग करता है वही गृही अणुव्रती है। अतः ग्रन्थकारके उक्त कथन विचारणीय हैं, अस्तु । दिशाओंको मर्यादाके स्थान प्रसिद्ध होना चाहिए जो मर्यादा देनेवाले और लेनेवालेके परिचित हों । अन्यथा भूल जाने की सम्भावना है। यह व्रत अणुव्रती के लिए है, महाव्रतीके लिए नहीं है । महाव्रती तो समस्त आरम्भ और परिग्रहसे विरत तथा समितिमें तत्पर होता है। अतः वह मनुष्यलोकमें यथेच्छ गमनागमन कर सकता है ।।२।।
आगे दिग्नतके द्वारा अणुव्रतीको महाव्रतोपना सिद्ध करते हैं
दिग्वतके द्वारा मर्यादाके बाहर स्थूल और सूक्ष्म हिंसा आदि सब पापोंसे विरत होनेसे तपाये हुए लोहेके पिण्डके भो समान श्रावक महाव्रतीके समान होता है ॥३॥
विशेषार्थ-जो समस्त पापोंसे विरत होता है वह महाव्रती होता है । यद्यपि श्रावककी आन्तरिक स्थिति तपाये हुए लोहे के गोलेके समान है । क्योंकि वह आरम्भ और परिग्रहमें लगा रहनेसे सर्वत्र जाने-आने, भोजन-शयन आदि क्रियाओंमें जीवोंका घात करता है। किन्तु दिशाओंकी सीमा बाँध लेनेसे की हुई मर्यादाके बाहर न वह त्रस जीवोंकी हिंसा करता है और न स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है। तथा मर्यादाके बाहर व्यापार करनेसे प्रचुर लाभ होनेपर भी वह व्यापार नहीं करता। इससे लोभका भी निराश होता है । अतः उसे उस क्षेत्रकी अपेक्षा महाव्रतीपना प्राप्त होता है। कहा है-'मर्यादाके बाहर सूक्ष्म पापसे भी विरत होनेसे दिग्वतके धारण करनेवालोंके अणुव्रत पंचमहाव्रतके रूपमें परिणत हो जाते है।' समिति गुप्ति प्रधानव्रतधारी साधुओंको यह दोष नहीं होता। इसलिए उनके दिग्विरति व्रत नहीं होता ॥३॥
आगे उक्त कथनकी पुष्टि करते हैं
दिग्व्रतके द्वारा चारित्रको घातनेवाली प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयकी मन्दताके बढ़ जानेसे गृहस्थका प्रत्याख्यानावरण नामक चारित्रमोह परिणाम इतना सूक्ष्म रह जाता है कि उसका निश्चय करना अशक्य होता है। इसीसे उसके अणुव्रत महाव्रतके समान होते हैं ॥४॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org