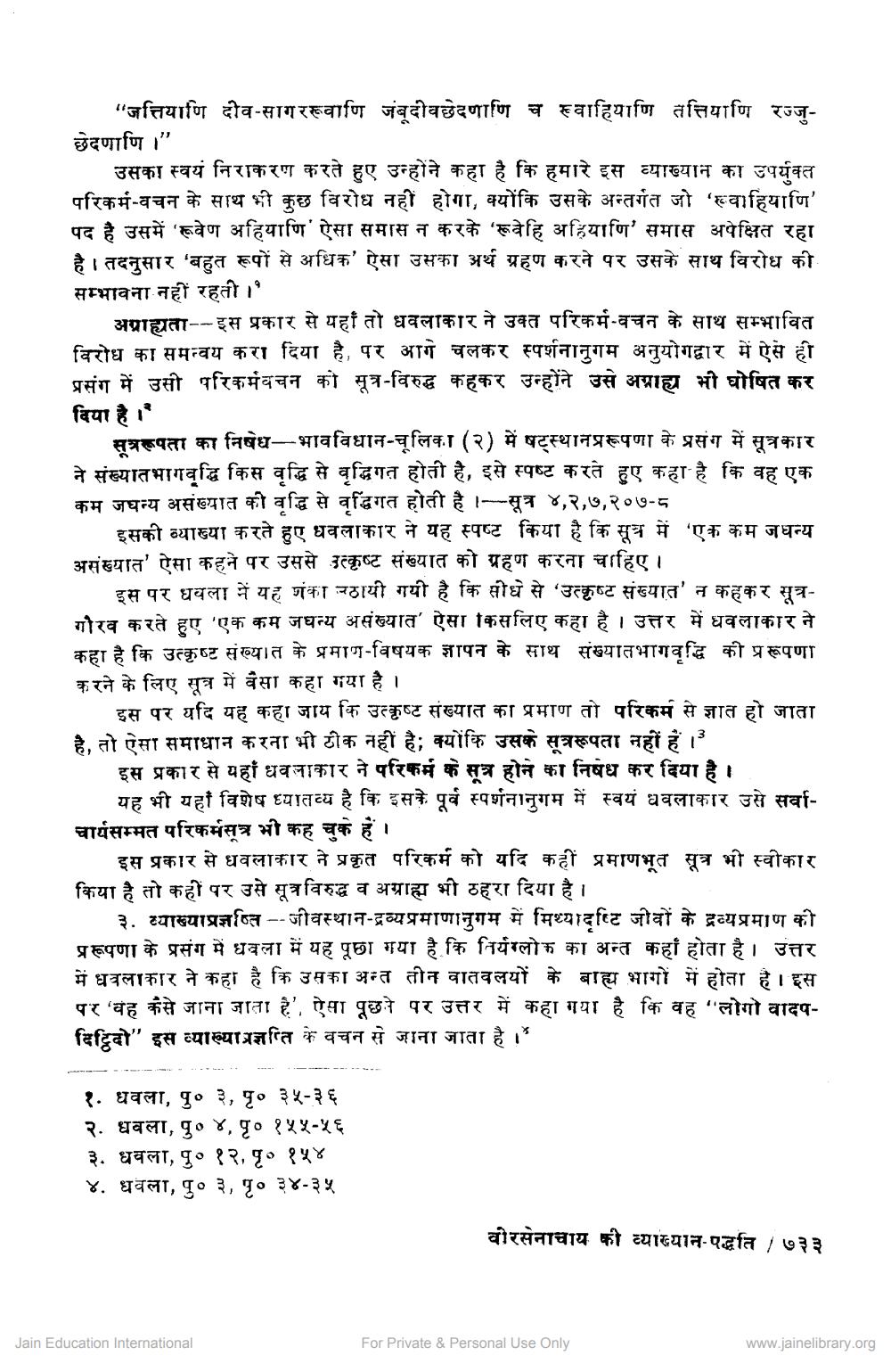________________
"जत्तियाणि दीव-सागररूवाणि जंबूदीवछेदणाणि च स्वाहियाणि तत्तियाणि रज्जुछेदणाणि ।" __उसका स्वयं निराकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे इस व्याख्यान का उपर्युक्त परिकर्म-वचन के साथ भी कुछ विरोध नहीं होगा, क्योंकि उसके अन्तर्गत जो 'रूवाहियाणि' पद है उसमें 'रूवेण अहियाणि ऐसा समास न करके 'रूवेहि अहियाणि' समास अपेक्षित रहा है। तदनुसार 'बहुत रूपों से अधिक' ऐसा उसका अर्थ ग्रहण करने पर उसके साथ विरोध की सम्भावना नहीं रहती।'
अग्राह्यता-- इस प्रकार से यहाँ तो धवलाकार ने उक्त परिकर्म-वचन के साथ सम्भावित विरोध का समन्वय करा दिया है, पर आगे चलकर स्पर्शनानुगम अनुयोगद्वार में ऐसे ही प्रसंग में उसी परिकर्मवचन को सूत्र-विरुद्ध कहकर उन्होंने उसे अग्राह्य भी घोषित कर दिया है।'
सूत्ररूपता का निषेध-भावविधान-चूलिका (२) में षट्स्थानप्ररूपणा के प्रसंग में सूत्रकार ने संख्यातभागवद्धि किस वृद्धि से वृद्धिगत होती है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह एक कम जघन्य असंख्यात की वृद्धि से वृद्धिंगत होती है ।---सूत्र ४,२,७,२०७-८
इसकी व्याख्या करते हुए धवलाकार ने यह स्पष्ट किया है कि सूत्र में एक कम जघन्य असंख्यात' ऐसा कहने पर उससे उत्कृष्ट संख्यात को ग्रहण करना चाहिए।
इस पर धवला में यह शंका ठायी गयी है कि सीधे से 'उत्कृष्ट संख्यात' न कहकर सुत्रगौरव करते हुए एक कम जघन्य असंख्यात' ऐसा किसलिए कहा है । उत्तर में धवलाकार ने कहा है कि उत्कृष्ट संख्यात के प्रमाण-विषयक ज्ञापन के साथ संख्यातभागवृद्धि की प्ररूपणा करने के लिए सूत्र में वैसा कहा गया है ।
इस पर यदि यह कहा जाय कि उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण तो परिकर्म से ज्ञात हो जाता है, तो ऐसा समाधान करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसके सूत्ररूपता नहीं हैं।
इस प्रकार से यहाँ धवलाकार ने परिकर्म के सूत्र होने का निषेध कर दिया है।
यह भी यहां विशेष ध्यातव्य है कि इसके पूर्व स्पर्शनानुगम में स्वयं धवलाकार उसे सर्वाचार्यसम्मत परिकर्मसूत्र भी कह चुके हैं।
इस प्रकार से धवलाकार ने प्रकृत परिकर्म को यदि कहीं प्रमाणभूत सूत्र भी स्वीकार किया है तो कहीं पर उसे सूत्रविरुद्ध व अग्राह्म भी ठहरा दिया है।
३. व्याख्याप्रज्ञप्ति --जीवस्थान-द्रव्यप्रमाणानुगम में मिथ्यादष्टि जीवों के द्रव्यप्रमाण की प्ररूपणा के प्रसंग में धवला में यह पूछा गया है कि तिर्यग्लोक का अन्त कहाँ होता है। उत्तर में धवलाकार ने कहा है कि उसका अन्त तीन वातवलयों के बाह्य भागों में होता है। इस पर वह कैसे जाना जाता है', ऐसा पूछने पर उत्तर में कहा गया है कि वह "लोगो वादपदिट्रिदो" इस व्याख्याज्ञप्ति के वचन से जाना जाता है ।
१. धवला, पु० ३, पृ० ३५-३६ २. धवला, पु०४, पृ० १५५-५६ ३. धवला, पु० १२, पृ० १५४ ४. धवला, पु० ३, पृ० ३४-३५
वीरसेनाचाय की व्याख्यान-पद्धति । ७३३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org