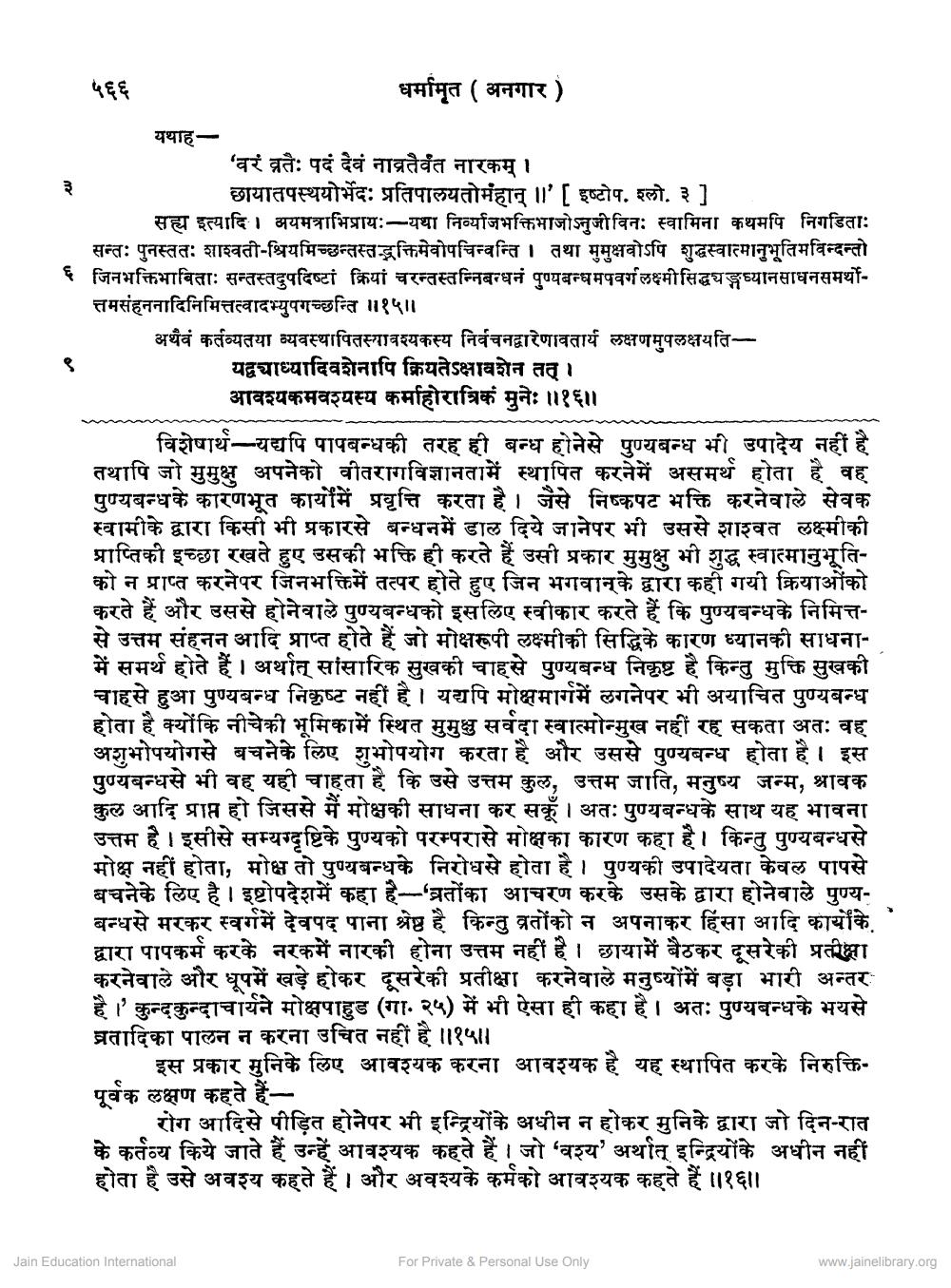________________
५६६
धर्मामृत ( अनगार)
यथाह
'वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वत नारकम् ।
छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोमहान् ।।' [ इष्टोप. श्लो. ३ ] सह्य इत्यादि। अयमत्राभिप्राय:-यथा निाजभक्तिभाजोऽनुजीविनः स्वामिना कथमपि निगडिताः ___ सन्तः पुनस्ततः शाश्वती-श्रियमिच्छन्तस्तद्भक्तिमेवोपचिन्वन्ति । तथा ममक्षवोऽपि शुद्धस्वात्मानुभूतिमविन्दन्तो जिनभक्तिभाविताः सन्तस्तदुपदिष्टां क्रियां चरन्तस्तन्निबन्धनं पुण्यबन्धमपवर्गलक्ष्मीसिद्धयङ्गध्यानसाधनसमर्थोत्तमसंहननादिनिमित्तत्वादभ्युपगच्छन्ति ॥१५॥ अथैवं कर्तव्यतया व्यवस्थापितस्यावश्यकस्य निर्वचनद्वारेणावतार्य लक्षणमुपलक्षयति
यद्वयाध्यादिवशेनापि क्रियतेऽक्षावशेन तत।
आवश्यकमवश्यस्य कर्माहोरात्रिकं मुनेः ॥१६॥ विशेषार्थ यद्यपि पापबन्धकी तरह ही बन्ध होनेसे पुण्यबन्ध भी उपादेय नहीं है तथापि जो मुमुक्षु अपनेको वीतरागविज्ञानतामें स्थापित करने में असमर्थ होता है वह पुण्यबन्धके कारणभूत कार्यों में प्रवृत्ति करता है। जैसे निष्कपट भक्ति करनेवाले सेवक स्वामीके द्वारा किसी भी प्रकारसे बन्धनमें डाल दिये जानेपर भी उससे शाश्वत लक्ष्मीकी प्राप्तिको इच्छा रखते हुए उसकी भक्ति ही करते हैं उसी प्रकार मुमुक्ष भी शुद्ध स्वात्मानुभूतिको न प्राप्त करनेपर जिनभक्तिमें तत्पर होते हुए जिन भगवानके द्वारा कही गयी क्रियाओंको करते हैं और उससे होनेवाले पुण्यबन्धको इसलिए स्वीकार करते हैं कि पुण्यबन्धके निमित्तसे उत्तम संहनन आदि प्राप्त होते हैं जो मोक्षरूपी लक्ष्मीकी सिद्धिके कारण ध्यानकी साधनामें समर्थ होते हैं । अर्थात् सांसारिक सुखकी चाहसे पुण्यबन्ध निकृष्ट है किन्तु मुक्ति सुखकी चाहसे हुआ पुण्यबन्ध निकृष्ट नहीं है। यद्यपि मोक्षमार्गमें लगनेपर भी अयाचित पुण्यबन्ध होता है क्योंकि नीचेकी भूमिकामें स्थित मुमुक्षु सर्वदा स्वात्मोन्मुख नहीं रह सकता अतः वह अशुभोपयोगसे बचनेके लिए शुभोपयोग करता है और उससे पुण्यबन्ध होता है। इस पुण्यबन्धसे भी वह यही चाहता है कि उसे उत्तम कुल, उत्तम जाति, मनुष्य जन्म, श्रावक कुल आदि प्राप्त हो जिससे मैं मोक्षकी साधना कर सकूँ । अतः पुण्यबन्धके साथ यह भावना उत्तम है। इसीसे सम्यग्दृष्टिके पुण्यको परम्परासे मोक्षका कारण कहा है। किन्तु पुण्यबन्धसे मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो पुण्यबन्धके निरोधसे होता है। पुण्यकी उपादेयता केवल पापसे बचनेके लिए है । इष्टोपदेशमें कहा है-'व्रतोंका आचरण करके उसके द्वारा होनेवाले पुण्यबन्धसे मरकर स्वर्गमें देवपद पाना श्रेष्ठ है किन्तु व्रतोंको न अपनाकर हिंसा आदि कार्योंके. द्वारा पापकर्म करके नरकमें नारकी होना उत्तम नहीं है। छायामें बैठकर दूसरेकी प्रत करनेवाले और धूपमें खड़े होकर दूसरेकी प्रतीक्षा करनेवाले मनुष्योंमें बड़ा भारी अन्तर है।' कुन्दकुन्दाचार्यने मोक्षपाहुड (गा. २५) में भी ऐसा ही कहा है। अतः पुण्यबन्धके भयसे व्रतादिका पालन न करना उचित नहीं है ॥१५॥
इस प्रकार मुनिके लिए आवश्यक करना आवश्यक है यह स्थापित करके निरुक्तिपूर्वक लक्षण कहते हैं- रोग आदिसे पीड़ित होनेपर भी इन्द्रियों के अधीन न होकर मुनिके द्वारा जो दिन-रात के कर्तव्य किये जाते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं । जो 'वश्य' अर्थात् इन्द्रियोंके अधीन नहीं होता है उसे अवश्य कहते हैं। और अवश्यके कर्मको आवश्यक कहते हैं ।।१६।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org