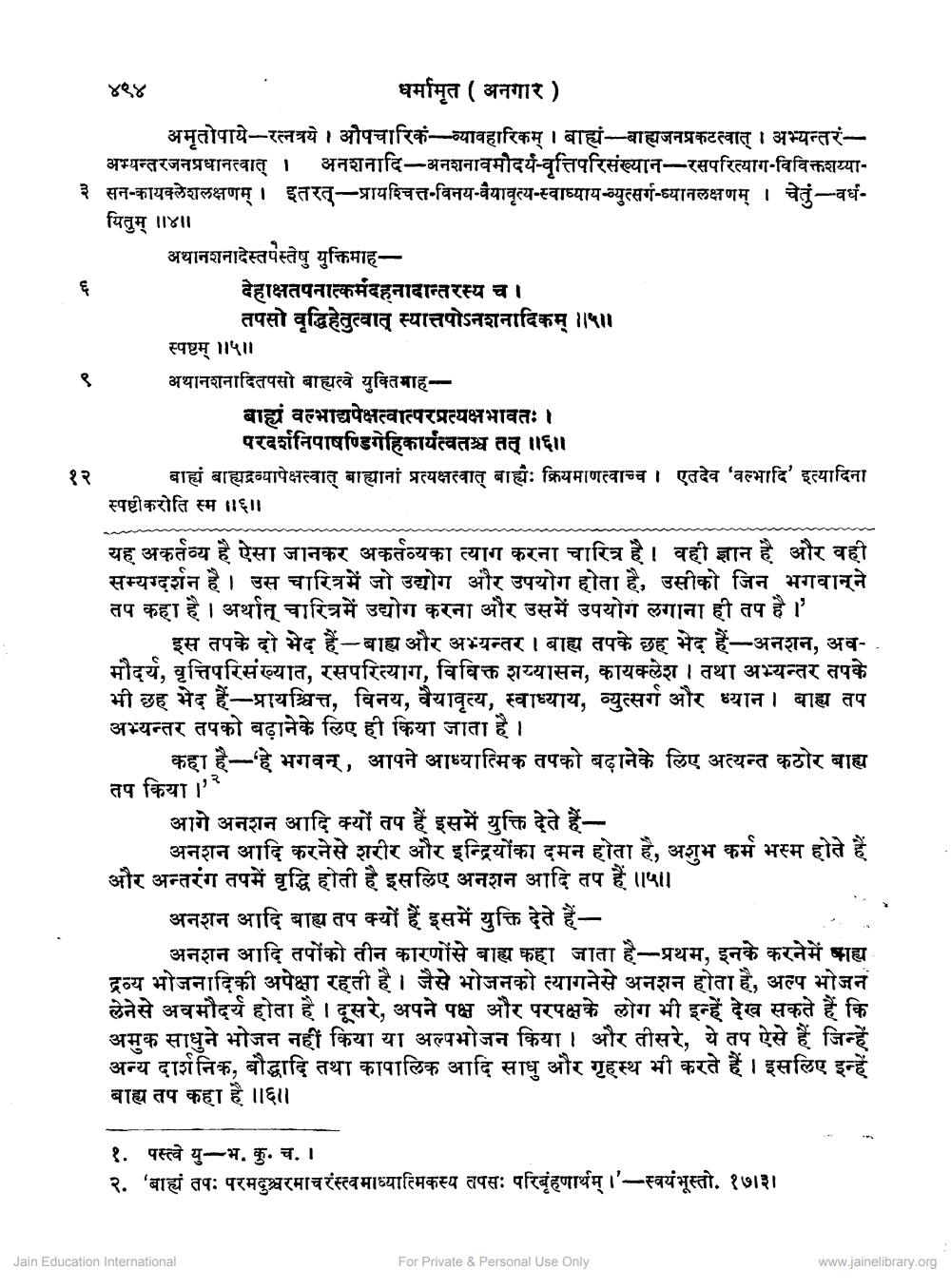________________
४९४
धर्मामृत ( अनगार) अमृतोपाये-रत्नत्रये । औपचारिक-व्यावहारिकम् । बाह्य-बाह्यजनप्रकटत्वात् । अभ्यन्तरंअभ्यन्तरजनप्रधानत्वात् । अनशनादि-अनशनावमौदर्य-वृत्तिपरिसंख्यान-रसपरित्याग-विविक्तशय्या३ सन-कायक्लेशलक्षणम् । इतरत्-प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानलक्षणम् । चेतुं-वर्धयितुम् ॥४॥ अथानशनादेस्तस्तेषु युक्तिमाह
देहाक्षतपनात्कर्मदहनादान्तरस्य च ।
तपसो वृद्धिहेतुत्वात् स्यात्तपोऽनशनादिकम् ॥५॥ स्पष्टम् ॥५॥ अथानशनादितपसो बाह्यत्वे युक्तिमाह
बाह्यं वल्भाद्यपेक्षत्वात्परप्रत्यक्षभावतः।
परदर्शनिपाषण्डिगेहिकार्यत्वतश्च तत् ॥६॥ १२ बाह्यं बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् बाह्यानां प्रत्यक्षत्वात् बाह्यः क्रियमाणत्वाच्च । एतदेव 'वल्भादि' इत्यादिना
स्पष्टीकरोति स्म ॥६॥
यह अकर्तव्य है ऐसा जानकर अकर्तव्यका त्याग करना चारित्र है। वही ज्ञान है और वही सम्यग्दर्शन है। उस चारित्रमें जो उद्योग और उपयोग होता है, उसीको जिन भगवान्ने तप कहा है । अर्थात् चारित्रमें उद्योग करना और उसमें उपयोग लगाना ही तप है।'
इस तपके दो भेद हैं-बाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य तपके छह भेद हैं-अनशन, अव- . मौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यात, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश । तथा अभ्यन्तर तपके भी छह भेद हैं-प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान । बाह्य तप अभ्यन्तर तपको बढ़ानेके लिए ही किया जाता है।
कहा है-'हे भगवन , आपने आध्यात्मिक तपको बढ़ानेके लिए अत्यन्त कठोर बाह्य तप किया।
आगे अनशन आदि क्यों तप हैं इसमें युक्ति देते हैं
अनशन आदि करनेसे शरीर और इन्द्रियोंका दमन होता है, अशुभ कर्म भस्म होते हैं और अन्तरंग तपमें वृद्धि होती है इसलिए अनशन आदि तप हैं ॥५॥
अनशन आदि बाह्य तप क्यों हैं इसमें युक्ति देते हैं
अनशन आदि तपोंको तीन कारणोंसे बाह्य कहा जाता है-प्रथम, इनके करने में बाह्य द्रव्य भोजनादिकी अपेक्षा रहती है। जैसे भोजनको त्यागनेसे अनशन होता है, अल्प भोजन लेनेसे अवमौदर्य होता है । दूसरे, अपने पक्ष और परपक्षके लोग भी इन्हें देख सकते हैं कि अमुक साधुने भोजन नहीं किया या अल्पभोजन किया। और तीसरे, ये तप ऐसे हैं जिन्हें अन्य दार्शनिक, बौद्धादि तथा कापालिक आदि साधु और गृहस्थ भी करते हैं । इसलिए इन्हें बाह्य तप कहा है ॥६॥
१. पस्त्वे यु-भ. कु. च.। २. 'बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ।'-स्वयंभूस्तो. १७३।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org