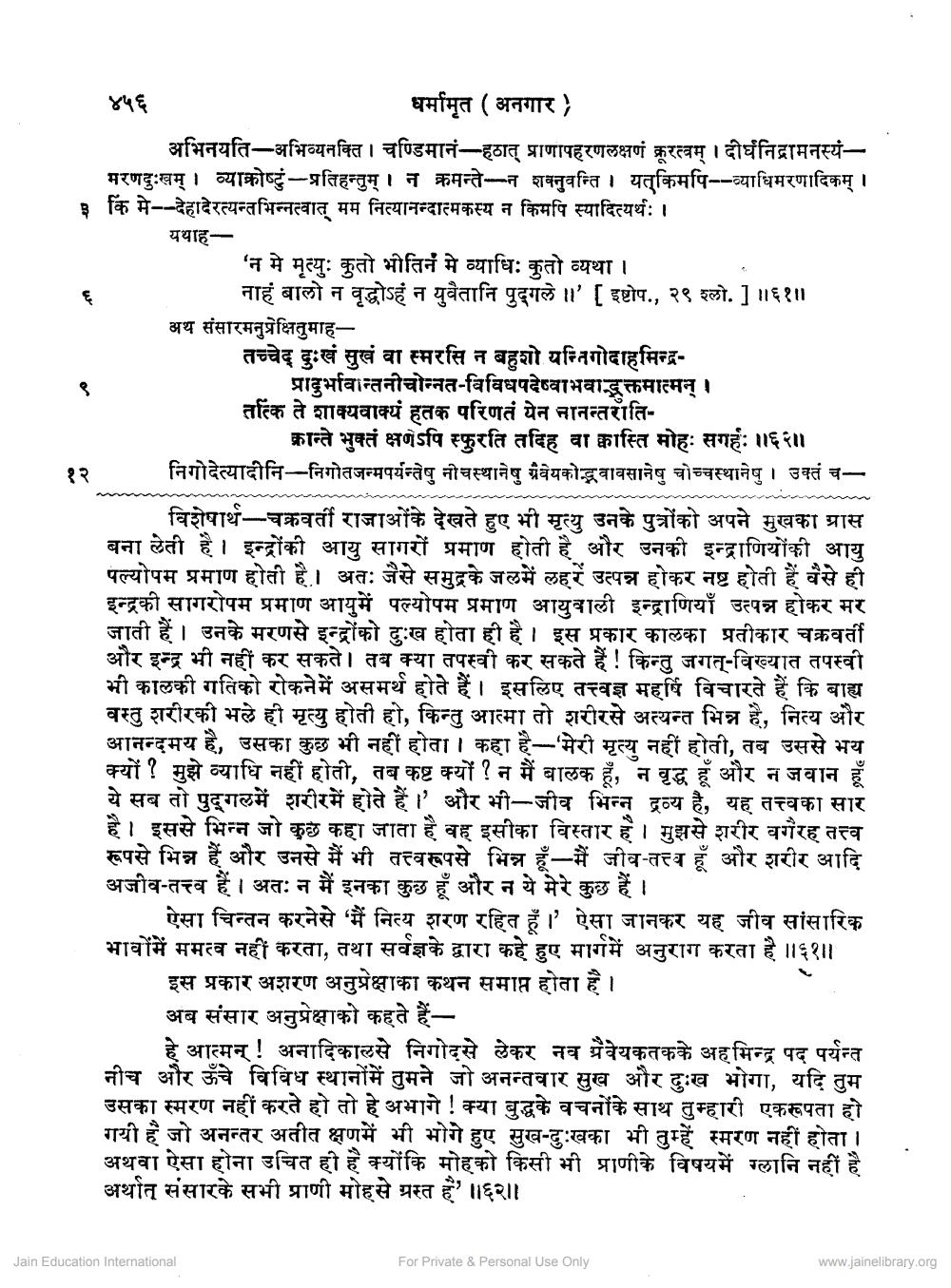________________
धर्मामृत ( अनगार) अभिनयति-अभिव्यनक्ति । चण्डिमानं-हठात् प्राणापहरणलक्षणं क्रूरत्वम् । दीर्घनिद्रामनस्यंमरणदुःखम् । व्याक्रोष्टुं-प्रतिहन्तुम् । न क्रमन्ते-न शक्नुवन्ति । यत्किमपि--व्याधिमरणादिकम् । ३ किं मे--देहादेरत्यन्तभिन्नत्वात् मम नित्यानन्दात्मकस्य न किमपि स्यादित्यर्थः । यथाह
'न मे मृत्युः कुतो भीतिनं मे व्याधिः कुतो व्यथा ।
नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥' [ इष्टोप., २९ श्लो. ] ॥६१॥ अथ संसारमनुप्रैक्षितुमाहतच्चेद् दुःखं सुखं वा स्मरसि न बहुशो यन्निगोदाहमिन्द्र
प्रादुर्भावान्तनीचोन्नत-विविधपदेष्वाभवाद्भक्तमात्मन् । तत्कि ते शाक्यवाक्यं हतक परिणतं येन नानन्तराति
___ क्रान्ते भुक्तं क्षणेऽपि स्फुरति तदिह वा क्वास्ति मोहः सगर्हः ॥६॥ निगोदेत्यादीनि-निगोतजन्मपर्यन्तेषु नीचस्थानेषु अवेयकोद्भवावसानेषु चोच्चस्थानेषु । उक्तं च
विशेषार्थ-चक्रवर्ती राजाओंके देखते हुए भी मृत्यु उनके पुत्रोंको अपने मुखका ग्रास बना लेती है। इन्द्रोंकी आयु सागरों प्रमाण होती है और उनकी इन्द्राणियोंकी आयु पल्योपम प्रमाण होती है। अतः जैसे समुद्र के जलमें लहरें उत्पन्न होकर नष्ट होती हैं वैसे ही इन्द्रकी सागरोपम प्रमाण आयुमें पल्योपम प्रमाण आयुवाली इन्द्राणियाँ उत्पन्न होकर मर जाती हैं। उनके मरणसे इन्द्रोंको दुःख होता ही है। इस प्रकार कालका प्रतीकार चक्रवर्ती और इन्द्र भी नहीं कर सकते। तब क्या तपस्वी कर सकते हैं! किन्तु जगत-विख्यात तपस्वी भी कालकी गतिको रोकने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तत्त्वज्ञ महर्षि विचारते हैं कि बाह्य वस्तु शरीरकी भले ही मृत्यु होती हो, किन्तु आत्मा तो शरीरसे अत्यन्त भिन्न है, नित्य और आनन्दमय है, उसका कुछ भी नहीं होता। कहा है-'मेरी मृत्यु नहीं होती, तब उससे भय क्यों ? मुझे व्याधि नहीं होती, तब कष्ट क्यों ? न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ और न जवान हूँ ये सब तो पुद्गलमें शरीरमें होते हैं।' और भी-जीव भिन्न द्रव्य है, यह तत्त्वका सार है। इससे भिन्न जो कुछ कहा जाता है वह इसीका विस्तार है। मुझसे शरीर वगैरह तत्त्व रूपसे भिन्न हैं और उनसे मैं भी तत्त्वरूपसे भिन्न हँ-मैं जीव-तत्त्व हूँ और शरीर आदि अजीव-तत्त्व हैं । अतः न मैं इनका कुछ हूँ और न ये मेरे कुछ हैं।
ऐसा चिन्तन करनेसे 'मैं नित्य शरण रहित हूँ।' ऐसा जानकर यह जीव सांसारिक भावोंमें ममत्व नहीं करता, तथा सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए मार्गमें अनुराग करता है ।।६।।
इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त होता है । अब संसार अनुप्रेक्षाको कहते हैं
हे आत्मन् ! अनादिकालसे निगोदसे लेकर नव अवेयकतकके अह मिन्द्र पद पर्यन्त नीच और ऊँचे विविध स्थानोंमें तुमने जो अनन्तवार सुख और दुःख भोगा, यदि तुम उसका स्मरण नहीं करते हो तो हे अभागे ! क्या बुद्धके वचनोंके साथ तुम्हारी एकरूपता हो गयी है जो अनन्तर अतीत क्षणमें भी भोगे हुए सुख-दुःखका भी तुम्हें स्मरण नहीं होता। अथवा ऐसा होना उचित ही है क्योंकि मोहको किसी भी प्राणीके विषयमें ग्लानि नहीं है अर्थात् संसारके सभी प्राणी मोहसे ग्रस्त है' ॥२॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org