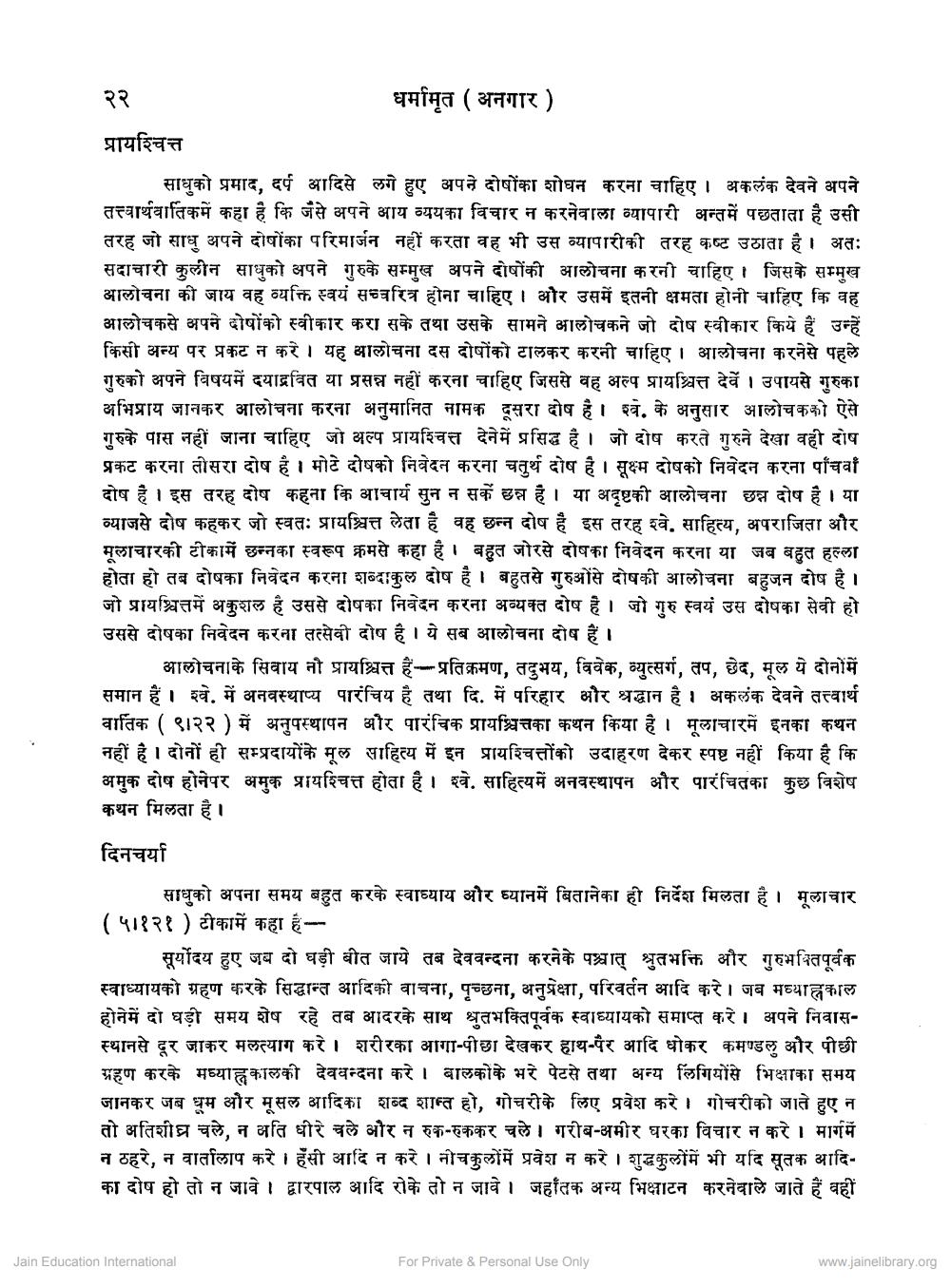________________
२२
धर्मामृत (अनगार)
प्रायश्चित्त
साधुको प्रमाद, दर्प आदिसे लगे हुए अपने दोषोंका शोधन करना चाहिए। अकलंक देवने अपने तत्त्वार्थवातिकमें कहा है कि जैसे अपने आय व्ययका विचार न करनेवाला व्यापारी अन्त में पछताता है उसी तरह जो साधु अपने दोषोंका परिमार्जन नहीं करता वह भी उस व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है। अतः सदाचारी कुलीन साधुको अपने गुरुके सम्मुख अपने दोषोंकी आलोचना करनी चाहिए। जिसके सम्मुख आलोचना की जाय वह व्यक्ति स्वयं सच्चरित्र होना चाहिए। और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह आलोचकसे अपने दोषोंको स्वीकार करा सके तथा उसके सामने आलोचकने जो दोष स्वीकार किये हैं उन्हें किसी अन्य पर प्रकट न करे। यह आलोचना दस दोषोंको टालकर करनी चाहिए। आलोचना करनेसे पहले गरुको अपने विषयमें दयाद्रवित या प्रसन्न नहीं करना चाहिए जिससे वह अल्प प्रायश्चित्त देवें । उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना अनुमानित नामक दूसरा दोष है। श्व. के अनुसार आलोचकको ऐसे गुरुके पास नहीं जाना चाहिए जो अल्प प्रायश्चित्त देने में प्रसिद्ध है। जो दोष करते गरुने देखा वही दोष प्रकट करना तीसरा दोष है । मोटे दोषको निवेदन करना चतुर्थ दोष है । सूक्ष्म दोषको निवेदन करना पाँचवाँ दोष है । इस तरह दोष कहना कि आचार्य सुन न सकें छन्न है । या अदृष्टकी आलोचना छन्न दोष है । या व्याजसे दोष कहकर जो स्वतः प्रायश्चित्त लेता है वह छन्न दोष है इस तरह श्वे. साहित्य, अपराजिता और मूलाचारकी टीका छन्नका स्वरूप क्रमसे कहा है। बहुत जोरसे दोषका निवेदन करना या जब बहुत हल्ला होता हो तब दोषका निवेदन करना शब्दाकुल दोष है। बहुतसे गुरुओंसे दोषकी आलोचना बहुजन दोष है। जो प्रायश्चित्तमें अकुशल है उससे दोषका निवेदन करना अव्यक्त दोष है। जो गुरु स्वयं उस दोषका सेवी हो उससे दोषका निवेदन करना तत्सेवी दोष है । ये सब आलोचना दोष हैं।
आलोचनाके सिवाय नौ प्रायश्चित्त हैं-प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल ये दोनों में समान हैं। श्वे. में अनवस्थाप्य पारंचिय है तथा दि. में परिहार और श्रद्धान है। अकलंक देवने तत्त्वार्थ वार्तिक ( ९।२२) में अनुपस्थापन और पारंचिक प्रायश्चित्तका कथन किया है । मूलाचारमें इनका कथन नहीं है । दोनों ही सम्प्रदायोंके मूल साहित्य में इन प्रायश्चित्तोंको उदाहरण देकर स्पष्ट नहीं किया है कि अमुक दोष होनेपर अमुक प्रायश्चित्त होता है। श्वे. साहित्यमें अनवस्थापन और पारंचितका कुछ विशेष कथन मिलता है।
दिनचर्या
साधुको अपना समय बहुत करके स्वाध्याय और ध्यानमें बितानेका ही निर्देश मिलता है। मूलाचार (५।१२१ ) टीकामें कहा है
। सूर्योदय हुए जब दो घड़ी बीत जाये तब देववन्दना करनेके पश्चात् श्रुतभक्ति और गुरुभक्तिपूर्वक स्वाध्यायको ग्रहण करके सिद्धान्त आदिकी वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन आदि करे। जब मध्याह्नकाल होने में दो घड़ी समय शेष रहे तब आदरके साथ श्रुतभक्तिपूर्वक स्वाध्यायको समाप्त करे। अपने निवासस्थानसे दूर जाकर मलत्याग करे। शरीरका आगा-पीछा देखकर हाथ-पैर आदि धोकर कमण्डलु और पीछी ग्रहण करके मध्याह्नकालकी देववन्दना करे । बालकोके भरे पेटसे तथा अन्य लिंगियोंसे भिक्षाका समय जानकर जब धूम और मूसल आदिका शब्द शान्त हो, गोचरीके लिए प्रवेश करे। गोचरीको जाते हुए न तो अतिशीघ्र चले, न अति धीरे चले और न रुक-रुककर चले। गरीब-अमीर घरका विचार न करे। मार्गमें न ठहरे, न वार्तालाप करे । हँसी आदि न करे । नोचकुलोंमें प्रवेश न करे । शुद्धकुलोंमें भी यदि सूतक आदिका दोष हो तो न जावे। द्वारपाल आदि रोके तो न जावे। जहाँतक अन्य भिक्षाटन करनेवाले जाते हैं वहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org