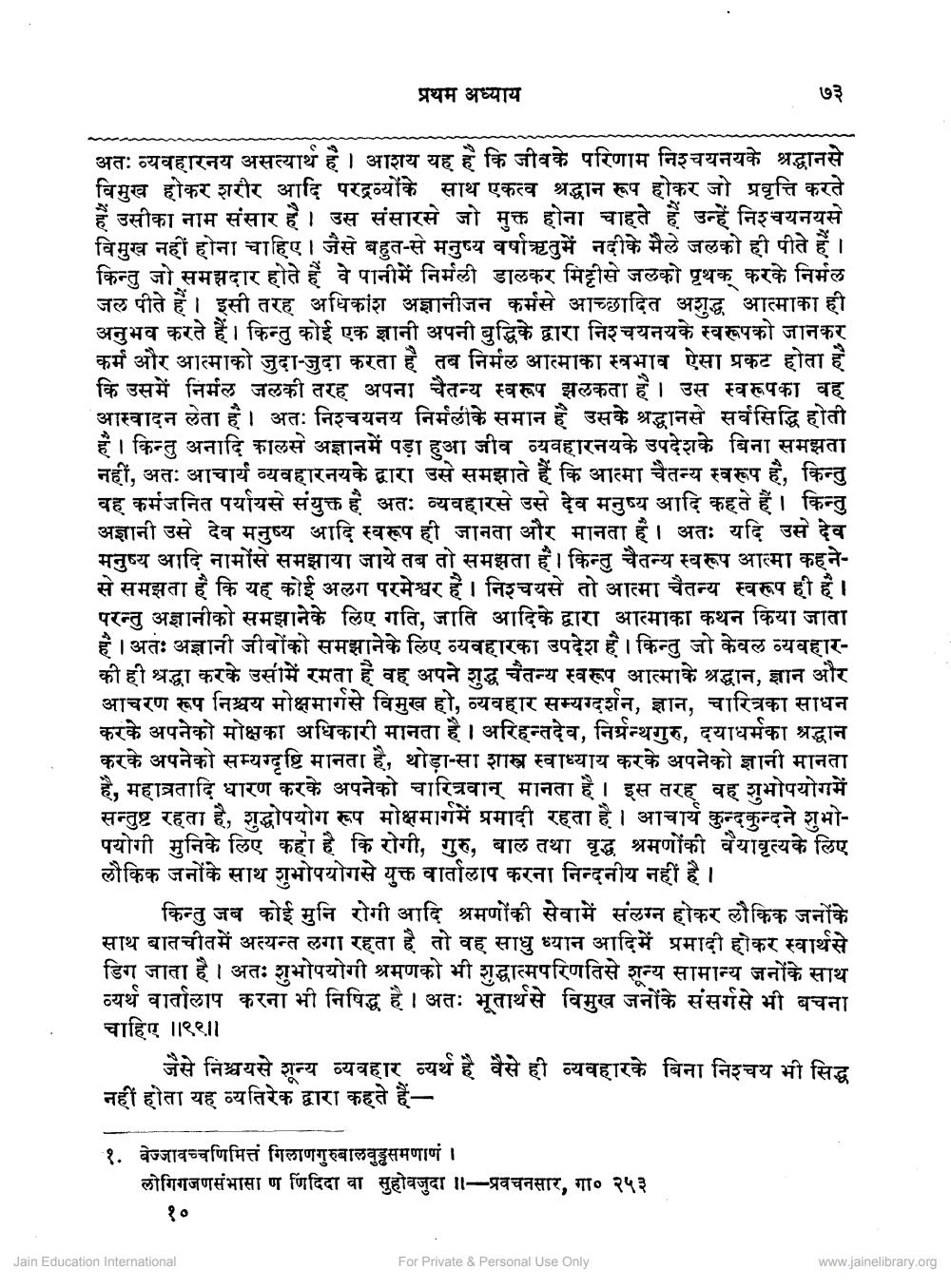________________
प्रथम अध्याय
७३
PRAKAR
अतः व्यवहारनय असत्यार्थ है। आशय यह है कि जीवके परिणाम निश्चयनयके श्रद्धानसे विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्योंके साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर जो प्रवृत्ति करते है उसीका नाम संसार है। उस संसारसे जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें निश्चयनयसे विमुख नहीं होना चाहिए । जैसे बहुत-से मनुष्य वर्षाऋतुमें नदीके मैले जलको ही पीते हैं। किन्तु जो समझदार होते हैं वे पानीमें निर्मली डालकर मिट्टीसे जलको पृथक् करके निर्मल जल पीते हैं। इसी तरह अधिकांश अज्ञानीजन कर्मसे आच्छादित अशुद्ध आत्माका ही अनुभव करते हैं। किन्तु कोई एक ज्ञानी अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चयनयके स्वरूपको जानकर कर्म और आत्माको जुदा-जुदा करता है तब निर्मल आत्माका स्वभाव ऐसा प्रकट होता है कि उसमें निर्मल जलकी तरह अपना चैतन्य स्वरूप झलकता है। उस स्वरूपका वह आस्वादन लेता है। अतः निश्चयनय निर्मलीके समान है उसके श्रद्धानसे सर्वसिद्धि होती है। किन्तु अनादि कालसे अज्ञानमें पड़ा हुआ जीव व्यवहारनयके उपदेशके बिना समझता नहीं, अतः आचार्य व्यवहारनयके द्वारा उसे समझाते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, किन्तु वह कर्मजनित पर्यायसे संयुक्त है, अतः व्यवहारसे उसे देव मनुष्य आदि कहते हैं। किन्तु अज्ञानी उसे देव मनुष्य आदि स्वरूप ही जानता और मानता है। अतः यदि उसे देव मनुष्य आदि नामोंसे समझाया जाये तब तो समझता है। किन्तु चैतन्य स्वरूप आत्मा कहनेसे समझता है कि यह कोई अलग परमेश्वर है । निश्चयसे तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। परन्तु अज्ञानीको समझानेके लिए गति, जाति आदिके द्वारा आत्माका कथन किया जाता है । अतः अज्ञानी जीवोंको समझानेके लिए व्यवहारका उपदेश है। किन्तु जो केवल व्यवहारकी ही श्रद्धा करके उसीमें रमता है वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप निश्चय मोक्षमार्गसे विमुख हो, व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रका साधन करके अपनेको मोक्षका अधिकारी मानता है । अरिहन्तदेव, निम्रन्थगुरु, दयाधर्मका श्रद्धान करके अपनेको सम्यग्दृष्टि मानता है, थोड़ा-सा शास्त्र स्वाध्याय करके अपनेको ज्ञानी मानता है, महाव्रतादि धारण करके अपनेको चारित्रवान् मानता है । इस तरह वह शुभोपयोगमें सन्तुष्ट रहता है, शुद्धोपयोग रूप मोक्षमागमें प्रमादी रहता है। आचार्य कुन्दकुन्दने शुभोपयोगी मुनिके लिए कहा है कि रोगी, गुरु, बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी वैयावृत्यके लिए लौकिक जनों के साथ शुभोपयोगसे युक्त वातोलाप करना निन्दनीय नहीं है।
किन्तु जब कोई मुनि रोगी आदि श्रमणोंकी सेवामें संलग्न होकर लौकिक जनोंके साथ बातचीतमें अत्यन्त लगा रहता है तो वह साधु ध्यान आदिमें प्रमादी होकर स्वार्थसे डिग जाता है । अतः शुभोपयोगी श्रमणको भी शुद्धात्मपरिणतिसे शून्य सामान्य जनोंके साथ व्यर्थ वार्तालाप करना भी निषिद्ध है । अतः भूतार्थसे विमुख जनोंके संसर्गसे भी बचना चाहिए ।।९९॥
जैसे निश्चयसे शून्य व्यवहार व्यर्थ है वैसे ही व्यवहारके बिना निश्चय भी सिद्ध नहीं होता यह व्यतिरेक द्वारा कहते हैं
१
बेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुबालवुड्समणाणं । लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ।।-प्रवचनसार, गा० २५३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org