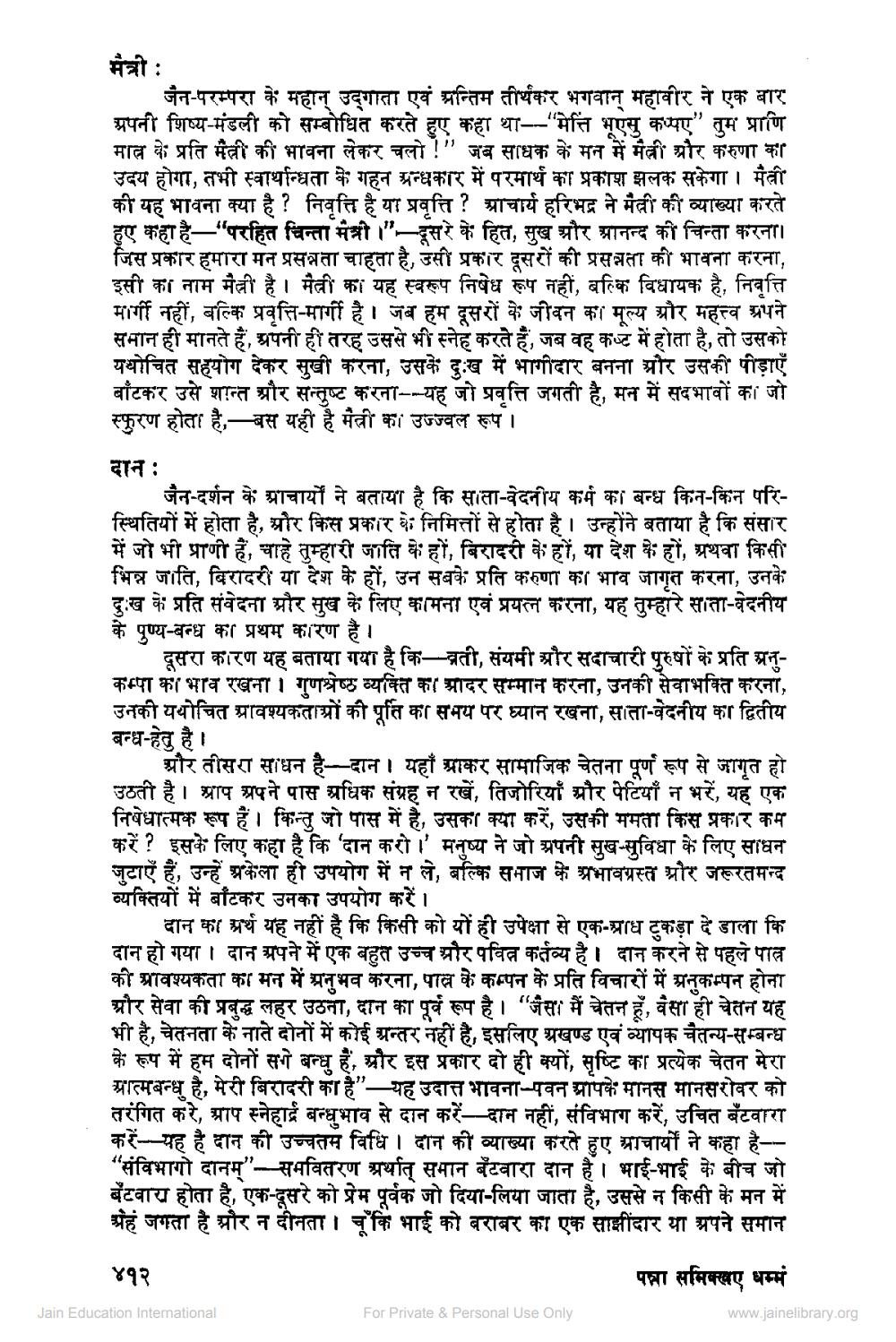Book Title: Yug Yug Ki Mang Samanta Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 6
________________ मैत्री: __ जैन-परम्परा के महान् उद्गाता एवं अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक बार अपनी शिष्य-मंडली को सम्बोधित करते हुए कहा था--"मेत्ति भूएसु कप्पए" तुम प्राणि मात्र के प्रति मैत्री की भावना लेकर चलो!" जब साधक के मन में मंत्री और करुणा का उदय होगा, तभी स्वार्थान्धता के गहन अन्धकार में परमार्थ का प्रकाश झलक सकेगा। मैत्री की यह भावना क्या है ? निवृत्ति है या प्रवृत्ति ? आचार्य हरिभद्र ने मंत्री की व्याख्या करते हुए कहा है—"परहित चिन्ता मंत्री।"-दूसरे के हित, सुख और आनन्द की चिन्ता करना। जिस प्रकार हमारा मन प्रसन्नता चाहता है, उसी प्रकार दूसरों की प्रसन्नता की भावना करना, इसी का नाम मैत्री है। मैत्री का यह स्वरूप निषेध रूप नहीं, बल्कि विधायक है, निवृत्ति मार्गी नहीं, बल्कि प्रवृत्ति-मार्गी है। जब हम दूसरों के जीवन का मूल्य और महत्त्व अपने समान ही मानते हैं, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते हैं, जब वह कष्ट में होता है, तो उसको यथोचित सहयोग देकर सुखी करना, उसके दुःख में भागीदार बनना और उसकी पीड़ाएँ बाँटकर उसे शान्त और सन्तुष्ट करना--यह जो प्रवृत्ति जगती है, मन में सदभावों का जो स्फुरण होता है, बस यही है मैत्री का उज्ज्वल रूप । दान: जैन-दर्शन के प्राचार्यों ने बताया है कि साता-वेदनीय कर्म का बन्ध किन-किन परिस्थितियों में होता है, और किस प्रकार के निमित्तों से होता है। उन्होंने बताया है कि संसार में जो भी प्राणी है, चाहे तुम्हारी जाति के हों, बिरादरी के हों, या देश के हों, अथवा किसी भिन्न जाति, बिरादरी या देश के हों, उन सबके प्रति करुणा का भाव जागृत करना, उनके दुःख के प्रति संवेदना और सुख के लिए कामना एवं प्रयत्न करना, यह तुम्हारे साता-वेदनीय के पुण्य-बन्ध का प्रथम कारण है। दूसरा कारण यह बताया गया है कि-व्रती, संयमी और सदाचारी पुरुषों के प्रति अनुकम्पा का भाव रखना । गुणश्रेष्ठ व्यक्ति का आदर सम्मान करना, उनकी सेवाभक्ति करना, उनकी यथोचित आवश्यकताओं की पूर्ति का समय पर ध्यान रखना, साता-वेदनीय का द्वितीय बन्ध-हेतु है। __ और तीसरा साधन है-दान। यहाँ प्राकर सामाजिक चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो उठती है। आप अपने पास अधिक संग्रह न रखें, तिजोरियाँ और पेटियाँ न भरें, यह एक निषेधात्मक रूप हैं। किन्तु जो पास में है, उसका क्या करें, उसकी ममता किस प्रकार कम करें? इसके लिए कहा है कि 'दान करो।' मनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा के लिए साधन जुटाएँ हैं, उन्हें अकेला ही उपयोग में न ले, बल्कि समाज के अभावग्रस्त और जरूरतमन्द व्यक्तियों में बाँटकर उनका उपयोग करें। दान का अर्थ यह नहीं है कि किसी को यों ही उपेक्षा से एक-प्राध टुकड़ा दे डाला कि दान हो गया। दान अपने में एक बहुत उच्च और पवित्न कर्तव्य है। दान करने से पहले पात्र की आवश्यकता का मन में अनुभव करना, पान के कम्पन के प्रति विचारों में अनुकम्पन होना और सेवा की प्रबुद्ध लहर उठना, दान का पूर्व रूप है। "जैसा मैं चेतन हूँ, वैसा ही चेतन यह भी है, चेतनता के नाते दोनों में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए अखण्ड एवं व्यापक चैतन्य-सम्बन्ध के रूप में हम दोनों सगे बन्धु हैं, और इस प्रकार दो ही क्यों, सृष्टि का प्रत्येक चेतन मेरा आत्मबन्धु है, मेरी बिरादरी का है”—यह उदात्त भावना-पवन आपके मानस मानसरोवर को तरंगित करे, आप स्नेहार्द्र बन्धुभाव से दान करें-दान नहीं, संविभाग करें, उचित बँटवारा करें-यह है दान की उच्चतम विधि । दान की व्याख्या करते हुए प्राचार्यों ने कहा है-- “संविभागो दानम्"--समवितरण अर्थात समान बँटवारा दान है। भाई-भाई के बीच जो बँटवारा होता है, एक-दूसरे को प्रेम पूर्वक जो दिया-लिया जाता है, उससे न किसी के मन में अहं जगता है और न दीनता। चूँकि भाई को बराबर का एक साझीदार या अपने समान ४१२ पन्ना समिक्खए धम्म Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7