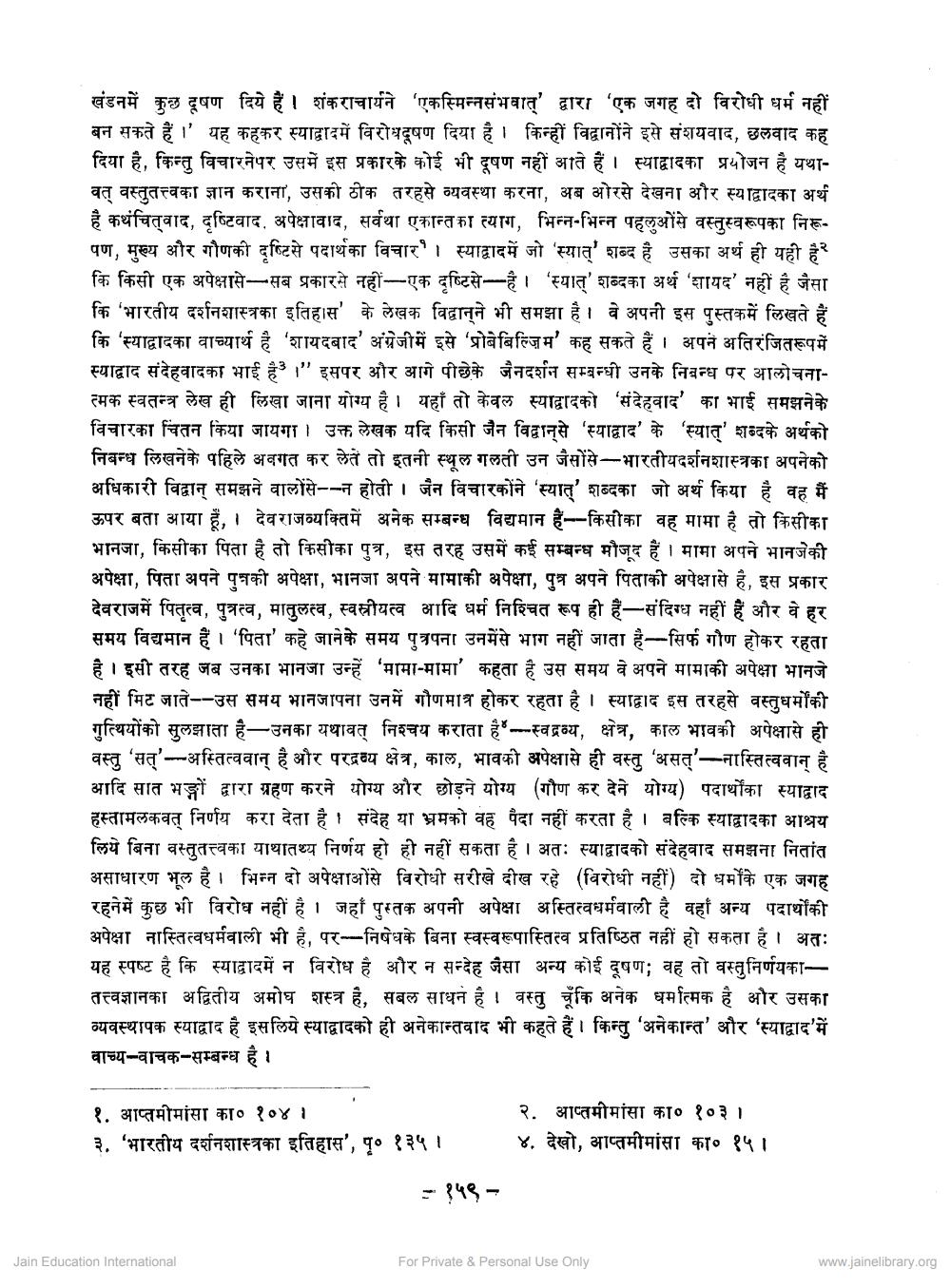Book Title: Veer Shasan aur uska Mahattva Author(s): Darbarilal Kothiya Publisher: Z_Darbarilal_Kothiya_Abhinandan_Granth_012020.pdf View full book textPage 5
________________ खंड में कुछ दूषण दिये हैं । शंकराचार्यने 'एकस्मिन्नसंभवात् ' द्वारा 'एक जगह दो विरोधी धर्म नहीं बन सकते हैं ।' यह कहकर स्याद्वाद में विरोधदूषण दिया है । किन्हीं विद्वानोंने इसे संशयवाद, छलवाद कह दिया है, किन्तु विचारनेपर उसमें इस प्रकारके कोई भी दूषण नहीं आते हैं । स्याद्वादका प्रयोजन है यथावत् वस्तुतत्त्वका ज्ञान कराना, उसकी ठीक तरहसे व्यवस्था करना, अब ओरसे देखना और स्याद्वादका अर्थ है कथंचित्वाद, दृष्टिवाद, अपेक्षावाद, सर्वथा एकान्तका त्याग, भिन्न-भिन्न पहलुओं से वस्तुस्वरूपका निरूपण, मुख्य और गौणकी दृष्टिसे पदार्थका विचार' । स्याद्वाद में जो 'स्यात्' शब्द है उसका अर्थ ही यही है कि किसी एक अपेक्षासे --- सब प्रकार से नहीं - एक दृष्टि से ― है । 'स्यात् ' शब्दका अर्थ 'शायद' नहीं है जैसा कि 'भारतीय दर्शनशास्त्रका इतिहास' के लेखक विद्वान्ने भी समझा है । वे अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि 'स्याद्वादका वाच्यार्थ है 'शायदबाद' अंग्रेजी में इसे 'प्रोबेबिल्ज़िम' कह सकते हैं । अपने अतिरंजितरूप में स्याद्वाद संदेहवादका भाई है ।" इसपर और आगे पीछेके जैनदर्शन सम्बन्धी उनके निबन्ध पर आलोचनात्मक स्वतन्त्र लेख ही लिखा जाना योग्य है । यहाँ तो केवल स्याद्वादको 'संदेहवाद' का भाई समझने के विचारका चिंतन किया जायगा । उक्त लेखक यदि किसी जैन विद्वान्से 'स्याद्वाद' के 'स्यात्' शब्द के अर्थको निबन्ध लिखनेके पहिले अवगत कर लेते तो इतनी स्थूल गलती उन जैसोंसे - भारतीयदर्शनशास्त्रका अपनेको अधिकारी विद्वान् समझने वालोंसे न होती । जैन विचारकोंने 'स्यात्' शब्दका जो अर्थ किया है वह मैं ऊपर बता आया हूँ, । देवराजव्यक्ति में अनेक सम्बन्ध विद्यमान हैं -- किसीका वह मामा है तो किसीका भानजा, किसीका पिता है तो किसीका पुत्र, इस तरह उसमें कई सम्बन्ध मौजूद हैं। मामा अपने भानजेकी अपेक्षा, पिता अपने पुत्र की अपेक्षा, भानजा अपने मामाकी अपेक्षा, पुत्र अपने पिताकी अपेक्षासे है, इस प्रकार देवराज में पितृत्व, पुत्रत्व, मातुलत्व, स्वस्त्रीयत्व आदि धर्म निश्चित रूप ही हैं - संदिग्ध नहीं हैं और वे हर समय विद्यमान हैं । 'पिता' कहे जाने के समय पुत्रपना उनमेंसे भाग नहीं जाता है - सिर्फ गौण होकर रहता है । इसी तरह जब उनका भानजा उन्हें 'मामा-मामा' कहता है उस समय वे अपने मामाकी अपेक्षा भानजे नहीं मिट जाते -- उस समय भानजापना उनमें गौणमात्र होकर रहता है । स्याद्वाद इस तरहसे वस्तुधर्मोकी गुत्थियों को सुलझाता है— उनका यथावत् निश्चय कराता है - स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भावकी अपेक्षा ही वस्तु 'सत्'---अस्तित्ववान् है और परद्रव्य क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा से ही वस्तु 'असत्' - नास्तित्ववान् है आदि सात भङ्गों द्वारा ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य ( गौण कर देने योग्य) पदार्थोंका स्याद्वाद हस्तामलकवत् निर्णय करा देता है । संदेह या भ्रमको वह पैदा नहीं करता है। बल्कि स्याद्वादका आश्रय लिये बिना वस्तुतत्त्वका याथातथ्य निर्णय हो ही नहीं सकता है । अतः स्याद्वादको संदेहवाद समझना नितांत असाधारण भूल है । भिन्न दो अपेक्षाओंसे विरोधी सरीखे दीख रहे ( विरोधी नहीं) दो धर्मोके एक जगह रहने में कुछ भी विरोध नहीं है । जहाँ पुस्तक अपनी अपेक्षा अस्तित्वधर्मवाली है वहाँ अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा नास्तित्वधर्मवाली भी है, पर -- निषेधके बिना स्वस्वरूपास्तित्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है । अतः यह स्पष्ट है कि स्याद्वाद में न विरोध है और न सन्देह जैसा अन्य कोई दूषण; वह तो वस्तुनिर्णयकातत्त्वज्ञानका अद्वितीय अमोघ शस्त्र है, सबल साधन है । वस्तु चूँकि अनेक धर्मात्मक है और उसका व्यवस्थापक स्याद्वाद है इसलिये स्याद्वादको ही अनेकान्तवाद भी कहते हैं । किन्तु 'अनेकान्त' और 'स्याद्वाद' में वाच्य - वाचक - सम्बन्ध है | १. आप्तमीमांसा का० १०४ । ३. 'भारतीय दर्शनशास्त्रका इतिहास', पृ० १३५ । Jain Education International - १५९ - २. आप्तमीमांसा का० १०३ । ४. देखो, आप्तमीमांसा का० १५ । For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6