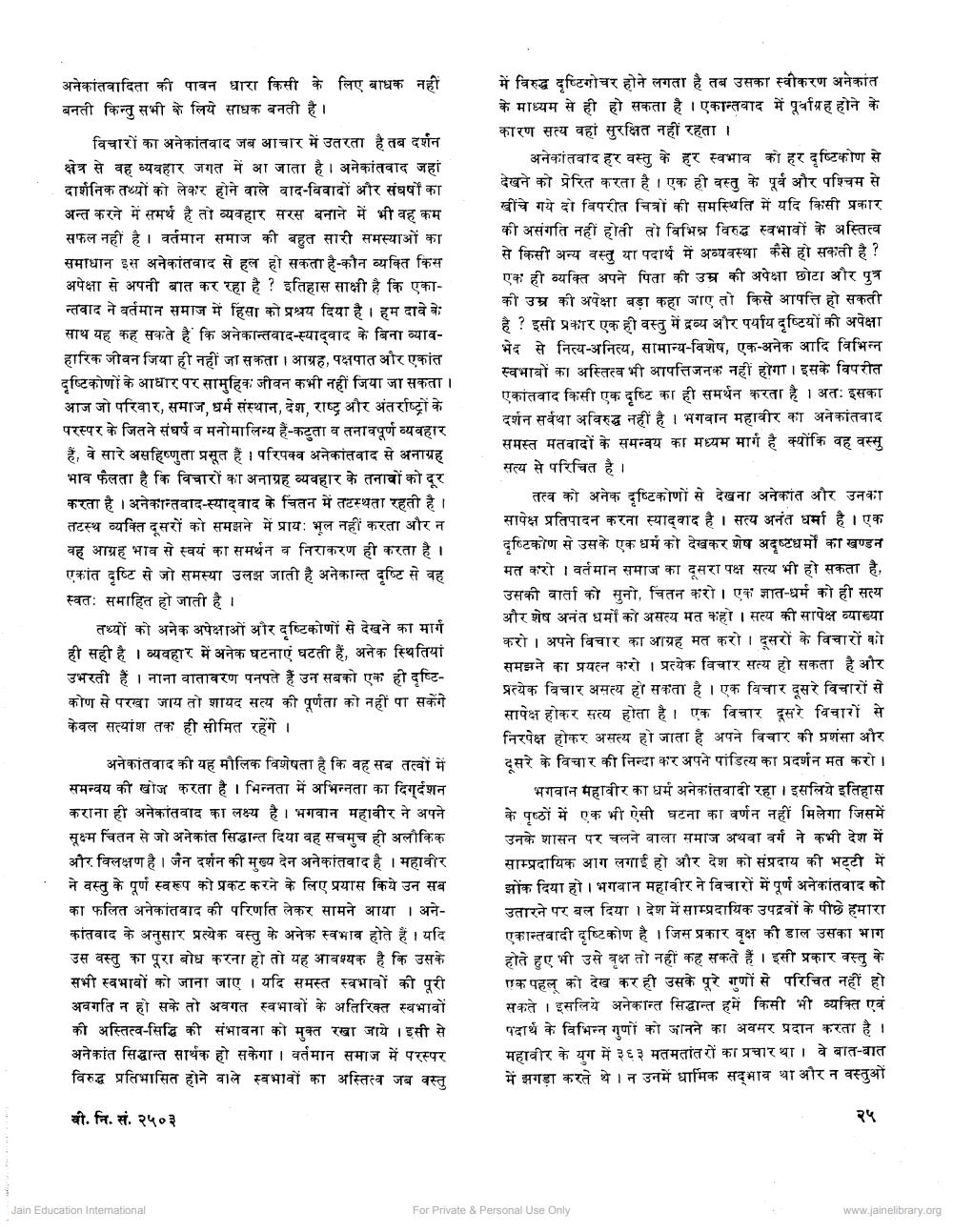Book Title: Vartaman Samaj aur Bhagavan Mahavir ka Anekant Siddhant Author(s): Shrichand Choradiya Publisher: Z_Rajendrasuri_Janma_Sardh_Shatabdi_Granth_012039.pdf View full book textPage 2
________________ अनेकांतवादिता की पावन धारा किसी के लिए बाधक नहीं बनती किन्तु सभी के लिये साधक बनती है। विचारों का अनेकांतवाद जब आचार में उतरता है तब दर्शन क्षेत्र से वह व्यवहार जगत में आ जाता है। अनेकांतवाद जहां दार्शनिक तथ्यों को लेकर होने वाले वाद-विवादों और संघर्षों का अन्त करने में समर्थ है तो व्यवहार सरस बनाने में भी वह कम सफल नहीं है। वर्तमान समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस अनेकांतवाद से हल हो सकता है-कौन व्यक्ति किस अपेक्षा से अपनी बात कर रहा है ? इतिहास साक्षी है कि एकान्तवाद ने वर्तमान समाज में हिंसा को प्रश्रय दिया है । हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि अनेकान्तवाद-स्याद्वाद के बिना व्यावहारिक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। आग्रह, पक्षपात और एकांत दृष्टिकोणों के आधार पर सामुहिक जीवन कभी नहीं जिया जा सकता। आज जो परिवार, समाज,धर्म संस्थान, देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रों के परस्पर के जितने संघर्ष व मनोमालिन्य हैं-कटुता व तनावपूर्ण व्यवहार हैं, वे सारे असहिष्णुता प्रसूत हैं । परिपक्व अनेकांतवाद से अनाग्रह भाव फैलता है कि विचारों का अनाग्रह व्यवहार के तनावों को दूर करता है । अनेकान्तवाद-स्याद्वाद के चिंतन में तटस्थता रहती है। तटस्थ व्यक्ति दूसरों को समझने में प्रायः भूल नहीं करता और न वह आग्रह भाव से स्वयं का समर्थन व निराकरण ही करता है । एकांत दृष्टि से जो समस्या उलझ जाती है अनेकान्त दृष्टि से वह स्वत: समाहित हो जाती है। तथ्यों को अनेक अपेक्षाओं और दृष्टिकोणों से देखने का मार्ग ही सही है । व्यवहार में अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक स्थितियां उभरती हैं । नाना वातावरण पनपते हैं उन सबको एक ही दृष्टिकोण से परखा जाय तो शायद सत्य की पूर्णता को नहीं पा सकेंगे केवल सत्यांश तक ही सीमित रहेंगे । ___ अनेकांतवाद की यह मौलिक विशेषता है कि वह सब तत्वों में समन्वय की खोज करता है । भिन्नता में अभिन्नता का दिग्रर्दशन कराना ही अनेकांतवाद का लक्ष्य है। भगवान महावीर ने अपने सूक्ष्म चिंतन से जो अनेकांत सिद्धान्त दिया वह सचमुच ही अलौकिक और विलक्षण है । जैन दर्शन की मुख्य देन अनेकांतवाद है । महावीर ने वस्तु के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रयास किये उन सब का फलित अनेकांतवाद की परिणति लेकर सामने आया । अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक स्वभाव होते हैं । यदि उस वस्तु का पूरा बोध करना हो तो यह आवश्यक है कि उसके सभी स्वभावों को जाना जाए । यदि समस्त स्वभावों की पूरी अवगति न हो सके तो अवगत स्वभावों के अतिरिक्त स्वभावों की अस्तित्व-सिद्धि की संभावना को मुक्त रखा जाये । इसी से अनेकांत सिद्धान्त सार्थक हो सकेगा। वर्तमान समाज में परस्पर विरुद्ध प्रतिभासित होने वाले स्वभावों का अस्तित्व जब वस्तु में विरुद्ध दृष्टिगोचर होने लगता है तब उसका स्वीकरण अनेकांत के माध्यम से ही हो सकता है । एकान्तवाद में पूर्वाग्रह होने के कारण सत्य वहां सुरक्षित नहीं रहता । अनेकांतवाद हर वस्तु के हर स्वभाव को हर दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित करता है । एक ही वस्तु के पूर्व और पश्चिम से खींचे गये दो विपरीत चित्रों की समस्थिति में यदि किसी प्रकार की असंगति नहीं होती तो विभिन्न विरुद्ध स्वभावों के अस्तित्व से किसी अन्य वस्तु या पदार्थ में अव्यवस्था कैसे हो सकती है ? एक ही व्यक्ति अपने पिता की उम्र की अपेक्षा छोटा और पुत्र की उम्र की अपेक्षा बड़ा कहा जाए तो किसे आपत्ति हो सकती है ? इसी प्रकार एक ही वस्तु में द्रव्य और पर्याय दृष्टियों की अपेक्षा भेद से नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, एक-अनेक आदि विभिन्न स्वभावों का अस्तित्व भी आपत्तिजनक नहीं होगा। इसके विपरीत एकांतवाद किसी एक दृष्टि का ही समर्थन करता है । अतः इसका दर्शन सर्वथा अविरुद्ध नहीं है। भगवान महावीर का अनेकांतवाद समस्त मतवादों के समन्वय का मध्यम मार्ग है क्योंकि वह वस्सु सत्य से परिचित है। तत्व को अनेक दृष्टिकोणों से देखना अनेकांत और उनका सापेक्ष प्रतिपादन करना स्याद्वाद है । सत्य अनंत धर्मा है । एक दृष्टिकोण से उसके एक धर्म को देखकर शेष अदृष्टधर्मों का खण्डन मत करो । वर्तमान समाज का दूसरा पक्ष सत्य भी हो सकता है, उसकी वार्ता को सुनो, चिंतन करो। एक ज्ञात-धर्म को ही सत्य और शेष अनंत धर्मों को असत्य मत कहो । सत्य की सापेक्ष व्याख्या करो। अपने विचार का आग्रह मत करो। दूसरों के विचारों को समझने का प्रयत्न करो । प्रत्येक विचार सत्य हो सकता है और प्रत्येक विचार असत्य हो सकता है । एक विचार दूसरे विचारों से सापेक्ष होकर सत्य होता है। एक विचार दूसरे विचारों से निरपेक्ष होकर असत्य हो जाता है अपने विचार की प्रशंसा और दूसरे के विचार की निन्दा कर अपने पांडित्य का प्रदर्शन मत करो। भगवान महावीर का धर्म अनेकांतवादी रहा । इसलिये इतिहास के पृष्ठों में एक भी ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलेगा जिसमें उनके शासन पर चलने वाला समाज अथवा वर्ग ने कभी देश में साम्प्रदायिक आग लगाई हो और देश को संप्रदाय की भट्टी में झोंक दिया हो । भगवान महावीर ने विचारों में पूर्ण अनेकांतवाद को उतारने पर बल दिया । देश में साम्प्रदायिक उपद्रवों के पीछे हमारा एकान्तवादी दृष्टिकोण है । जिस प्रकार वृक्ष की डाल उसका भाग होते हुए भी उसे वृक्ष तो नहीं कह सकते हैं । इसी प्रकार वस्तु के एक पहल को देख कर ही उसके पूरे गुणों से परिचित नहीं हो सकते । इसलिये अनेकान्त सिद्धान्त हमें किसी भी व्यक्ति एवं पदार्थ के विभिन्न गुणों को जानने का अवसर प्रदान करता है । महावीर के युग में ३६३ मतमतांतरों का प्रचार था। वे बात-बात में झगड़ा करते थे। न उनमें धार्मिक सद्भाव था और न वस्तुओं वी.नि.सं. २५०३ २५ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4