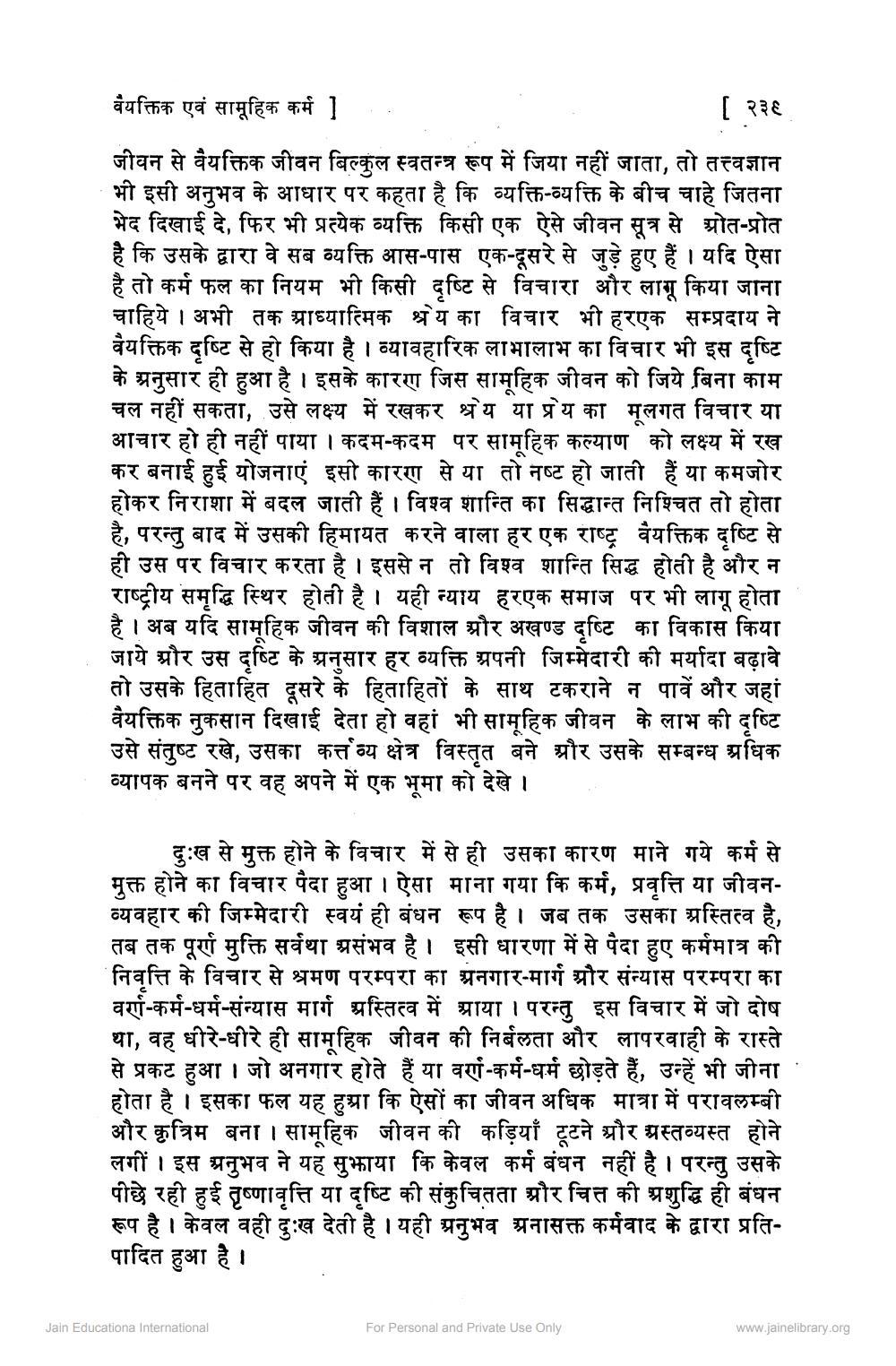Book Title: Vaiyaktik evam Samuhik Karm Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 3
________________ वैयक्तिक एवं सामूहिक कर्म ] [ २३६ जीवन से वैयक्तिक जीवन बिल्कुल स्वतन्त्र रूप में जिया नहीं जाता, तो तत्त्वज्ञान भी इसी अनुभव के आधार पर कहता है कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच चाहे जितना भेद दिखाई दे, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति किसी एक ऐसे जीवन सूत्र से ओत-प्रोत है कि उसके द्वारा वे सब व्यक्ति आस-पास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । यदि ऐसा है तो कर्म फल का नियम भी किसी दृष्टि से विचारा और लागू किया जाना चाहिये । अभी तक आध्यात्मिक श्रेय का विचार भी हरएक सम्प्रदाय ने वैयक्तिक दृष्टि से हो किया है । व्यावहारिक लाभालाभ का विचार भी इस दृष्टि के अनुसार ही हुआ है । इसके कारण जिस सामूहिक जीवन को जिये बिना काम चल नहीं सकता, उसे लक्ष्य में रखकर श्रेय या प्रेय का मूलगत विचार या आचार हो ही नहीं पाया । कदम-कदम पर सामूहिक कल्याण को लक्ष्य में रख कर बनाई हुई योजनाएं इसी कारण से या तो नष्ट हो जाती हैं या कमजोर होकर निराशा में बदल जाती हैं। विश्व शान्ति का सिद्धान्त निश्चित तो होता है, परन्तु बाद में उसकी हिमायत करने वाला हर एक राष्ट्र वैयक्तिक दृष्टि से ही उस पर विचार करता है । इससे न तो विश्व शान्ति सिद्ध होती है और न राष्ट्रीय समृद्धि स्थिर होती है। यही न्याय हरएक समाज पर भी लागू होता है । अब यदि सामूहिक जीवन की विशाल और अखण्ड दृष्टि का विकास किया जाये और उस दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी की मर्यादा बढ़ावे तो उसके हिताहित दूसरे के हिताहितों के साथ टकराने न पावें और जहां वैयक्तिक नुकसान दिखाई देता हो वहां भी सामूहिक जीवन के लाभ की दृष्टि उसे संतुष्ट रखे, उसका कर्तव्य क्षेत्र विस्तृत बने और उसके सम्बन्ध अधिक व्यापक बनने पर वह अपने में एक भूमा को देखे । दुःख से मुक्त होने के विचार में से ही उसका कारण माने गये कर्म से मुक्त होने का विचार पैदा हुआ। ऐसा माना गया कि कर्म, प्रवृत्ति या जीवनव्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ही बंधन रूप है। जब तक उसका अस्तित्व है, तब तक पूर्ण मुक्ति सर्वथा असंभव है। इसी धारणा में से पैदा हुए कर्ममात्र की निवृत्ति के विचार से श्रमण परम्परा का अनगार-मार्ग और संन्यास परम्परा का वर्ण-कर्म-धर्म-संन्यास मार्ग अस्तित्व में आया । परन्तु इस विचार में जो दोष था, वह धीरे-धीरे ही सामूहिक जीवन की निर्बलता और लापरवाही के रास्ते से प्रकट हुआ । जो अनगार होते हैं या वर्ण-कर्म-धर्म छोड़ते हैं, उन्हें भी जीना होता है । इसका फल यह हुआ कि ऐसों का जीवन अधिक मात्रा में परावलम्बी और कृत्रिम बना । सामूहिक जीवन की कड़ियाँ टूटने और अस्तव्यस्त होने लगीं। इस अनुभव ने यह सुझाया कि केवल कर्म बंधन नहीं है । परन्तु उसके पीछे रही हुई तृष्णावृत्ति या दृष्टि की संकुचितता और चित्त की अशुद्धि ही बंधन रूप है। केवल वही दुःख देती है । यही अनुभव अनासक्त कर्मवाद के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5