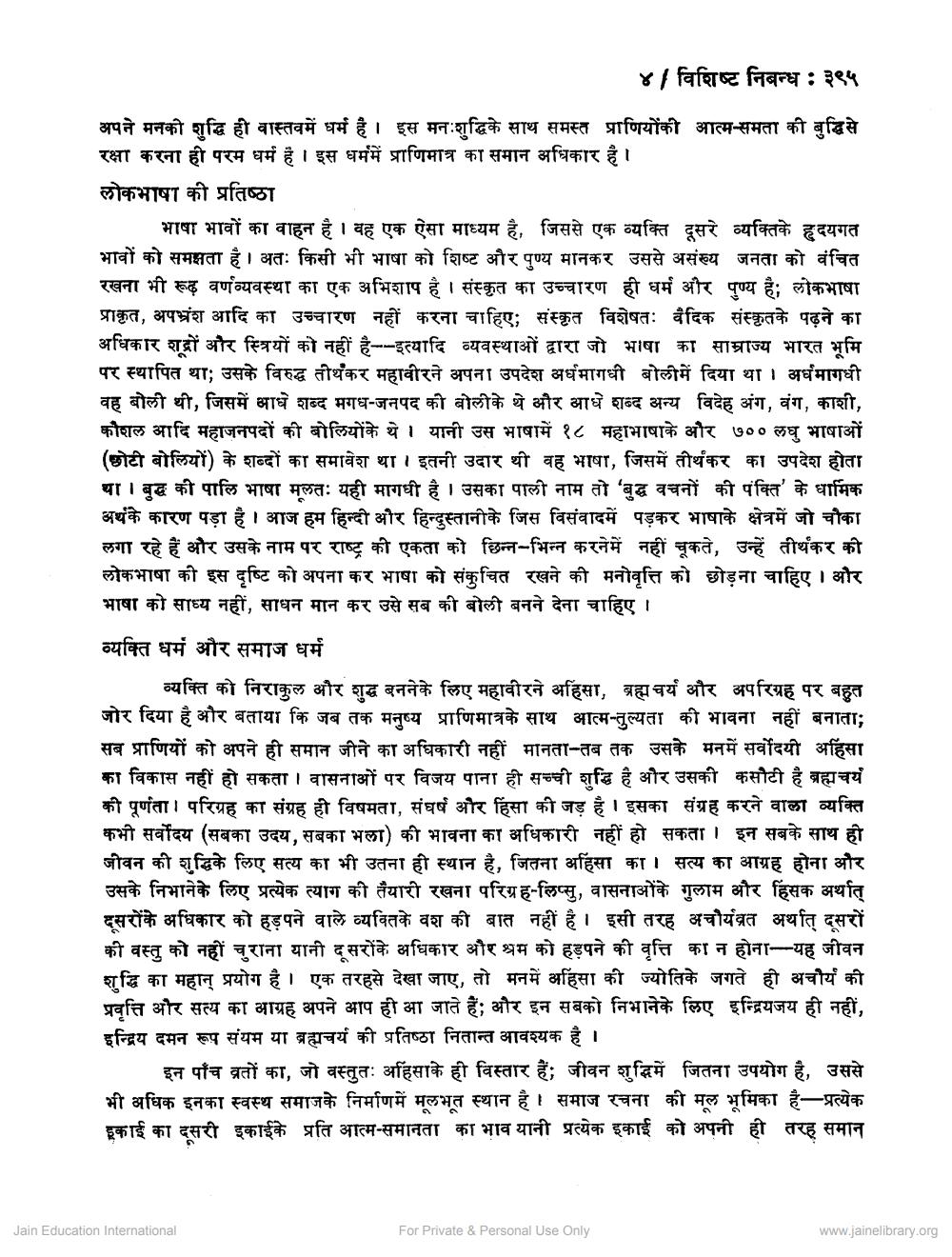Book Title: Tirthankar Mahavir Author(s): Publisher: Z_Mahendrakumar_Jain_Nyayacharya_Smruti_Granth_012005.pdf View full book textPage 3
________________ ४ / विशिष्ट निबन्ध : ३९५ अपने मनको शुद्धि ही वास्तवमें धर्म है। इस मनःशुद्धिके साथ समस्त प्राणियोंकी आत्म-समता की बुद्धिसे रक्षा करना ही परम धर्म है । इस धर्म में प्राणिमात्र का समान अधिकार है। लोकभाषा की प्रतिष्ठा भाषा भावों का वाहन है । वह एक ऐसा माध्यम है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके हृदयगत भावों को समझता है। अतः किसी भी भाषा को शिष्ट और पुण्य मानकर उससे असंख्य जनता को वंचित रखना भी रूढ़ वर्णव्यवस्था का एक अभिशाप है । संस्कृत का उच्चारण ही धर्म और पुण्य है; लोकभाषा प्राकृत, अपभ्रंश आदि का उच्चारण नहीं करना चाहिए; संस्कृत विशेषतः वैदिक संस्कृतके पढ़ने का अधिकार शद्रों और स्त्रियों को नहीं है--इत्यादि व्यवस्थाओं द्वारा जो भाषा का साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित था; उसके विरुद्ध तीर्थंकर महावीरने अपना उपदेश अर्धमागधी बोलीमें दिया था। अर्धमागधी वह बोली थी, जिसमें आधे शब्द मगध-जनपद की बोलीके थे और आधे शब्द अन्य विदेह अंग, वंग, काशी, कौशल आदि महाजनपदों की बोलियोंके थे। यानी उस भाषामें १८ महाभाषाके और ७०० लघु भाषाओं (छोटी बोलियों) के शब्दों का समावेश था। इतनी उदार थी वह भाषा, जिसमें तीर्थंकर का उपदेश होता था। बुद्ध की पालि भाषा मूलतः यही मागधी है । उसका पाली नाम तो 'बुद्ध वचनों की पंक्ति' के धार्मिक अर्थके कारण पड़ा है। आज हम हिन्दी और हिन्दुस्तानीके जिस विसंवादमें पड़कर भाषाके क्षेत्र में जो चौका लगा रहे हैं और उसके नाम पर राष्ट्र की एकता को छिन्न-भिन्न करने में नहीं चूकते, उन्हें तीर्थंकर की लोकभाषा की इस दृष्टि को अपना कर भाषा को संकुचित रखने की मनोवृत्ति को छोड़ना चाहिए । और भाषा को साध्य नहीं, साधन मान कर उसे सब की बोली बनने देना चाहिए । व्यक्ति धर्म और समाज धर्म व्यक्ति को निराकूल और शद्ध बननेके लिए महावीरने अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर बहुत जोर दिया है और बताया कि जब तक मनुष्य प्राणिमात्रके साथ आत्म-तुल्यता की भावना नहीं बनाता; सब प्राणियों को अपने ही समान जीने का अधिकारी नहीं मानता-तब तक उसके मनमें सर्वोदयी अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। वासनाओं पर विजय पाना ही सच्ची शुद्धि है और उसकी कसौटी है ब्रह्मचर्य की पूर्णता। परिग्रह का संग्रह ही विषमता, संघर्ष और हिंसा की जड़ है। इसका संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी सर्वोदय (सबका उदय, सबका भला) की भावना का अधिकारी नहीं हो सकता। इन सबके साथ ही जीवन की शुद्धिके लिए सत्य का भी उतना ही स्थान है, जितना अहिंसा का। सत्य का आग्रह होना और उसके निभानेके लिए प्रत्येक त्याग की तैयारी रखना परिग्रह-लिप्सु, वासनाओंके गुलाम और हिंसक अर्थात् दूसरोंके अधिकार को हड़पने वाले व्यक्तिके वश की बात नहीं है। इसी तरह अचौर्यव्रत अर्थात् दूसरों की वस्तु को नहीं चुराना यानी दूसरोंके अधिकार और श्रम को हड़पने की वृत्ति का न होना--यह जीवन शुद्धि का महान् प्रयोग है। एक तरहसे देखा जाए, तो मनमें अहिंसा की ज्योतिके जगते ही अचौर्य की प्रवृत्ति और सत्य का आग्रह अपने आप ही आ जाते हैं। और इन सबको निभानेके लिए इन्द्रियजय ही नहीं, इन्द्रिय दमन रूप संयम या ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नितान्त आवश्यक है। इन पाँच व्रतों का, जो वस्तुतः अहिंसाके ही विस्तार हैं; जीवन शुद्धिमें जितना उपयोग है, उससे भी अधिक इनका स्वस्थ समाजके निर्माणमें मलभत स्थान है। समाज रचना की मल भूमिका है-प्रत्येक इकाई का दूसरी इकाईके प्रति आत्म-समानता का भाव यानी प्रत्येक इकाई को अपनी ही तरह समान Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4