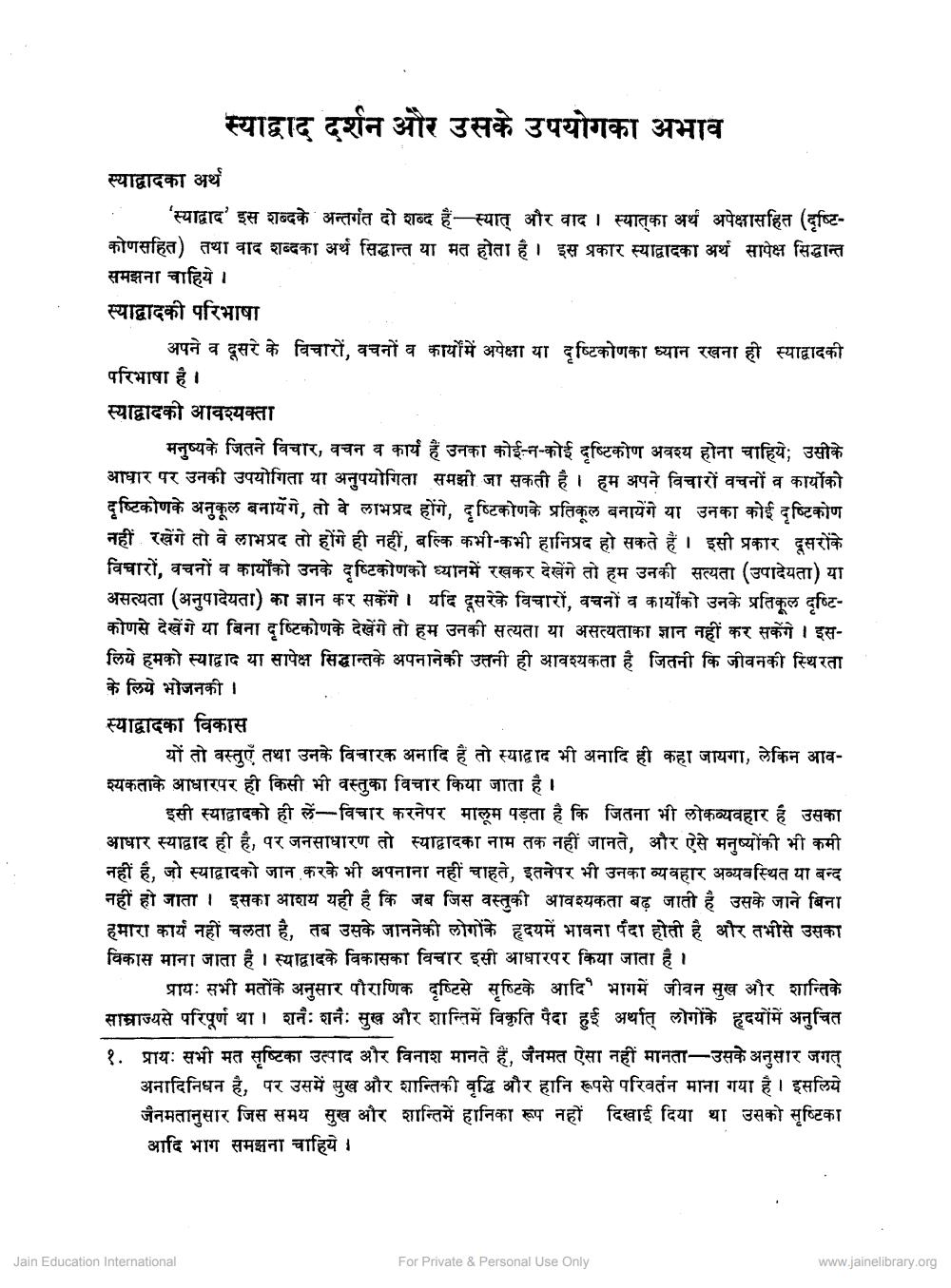Book Title: Syadwad Darshan aur uske upyogka Abhav Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 1
________________ स्याद्वाद दर्शन और उसके उपयोगका अभाव स्याद्वादका अर्थ - 'स्याद्वाद' इस शब्दके अन्तर्गत दो शब्द हैं-स्यात् और वाद । स्यातका अर्थ अपेक्षासहित (दृष्टिकोणसहित) तथा वाद शब्दका अर्थ सिद्धान्त या मत होता है। इस प्रकार स्याद्वादका अर्थ सापेक्ष सिद्धान्त समझना चाहिये। स्याद्वादकी परिभाषा अपने व दूसरे के विचारों, वचनों व कार्यों में अपेक्षा या दृष्टिकोणका ध्यान रखना ही स्याद्वादकी परिभाषा है। स्याद्वादको आवश्यक्ता मनुष्यके जितने विचार, वचन व कार्य हैं उनका कोई-न-कोई दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिये; उसीके आधार पर उनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता समझी जा सकती है। हम अपने विचारों वचनों व कार्योको दृष्टिकोणके अनुकूल बनायेंगे, तो वे लाभप्रद होंगे, दृष्टिकोणके प्रतिकूल बनायेंगे या उनका कोई दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो वे लाभप्रद तो होंगे ही नहीं, बल्कि कभी-कभी हानिप्रद हो सकते हैं। इसी प्रकार दूसरोंके विचारों, वचनों व कार्योंको उनके दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर देखेंगे तो हम उनकी सत्यता (उपादेयता) या मा (अनुपादेयता) का ज्ञान कर सकेंगे। यदि दूसरेके विचारों, वचनों व कार्योंको उनके प्रतिकूल दृष्टिकोणसे देखेंगे या बिना दृष्टिकोणके देखेंगे तो हम उनकी सत्यता या असत्यताका ज्ञान नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमको स्याद्वाद या सापेक्ष सिद्धान्तके अपनानेकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जीवनकी स्थिरता के लिये भोजनकी। स्याद्वादका विकास यों तो वस्तुएँ तथा उनके विचारक अनादि है तो स्याद्वाद भी अनादि ही कहा जायगा, लेकिन आवश्यकताके आधारपर ही किसी भी वस्तुका विचार किया जाता है। इसी स्याद्वादको ही लें-विचार करनेपर मालूम पड़ता है कि जितना भी लोकव्यवहार है उसका आधार स्याद्वाद ही है, पर जनसाधारण तो स्याद्वादका नाम तक नहीं जानते, और ऐसे मनुष्योंकी भी कमी नहीं है, जो स्याद्वादको जान करके भी अपनाना नहीं चाहते, इतनेपर भी उनका व्यवहार अव्यवस्थित या बन्द नहीं हो जाता। इसका आशय यही है कि जब जिस वस्तुकी आवश्यकता बढ़ जाती है उसके जाने बिना हमारा कार्य नहीं चलता है, तब उसके जाननेकी लोगोंके हृदयमें भावना पैदा होती है और तभीसे उसका विकास माना जाता है । स्याद्वादके विकासका विचार इसी आधारपर किया जाता है। प्रायः सभी मतोंके अनुसार पौराणिक दृष्टिसे सृष्टिके आदि' भागमें जीवन सुख और शान्तिके साम्राज्यसे परिपूर्ण था। शनैः शनैः सुख और शान्तिमें विकृति पैदा हुई अर्थात् लोगोंके हृदयोंमें अनुचित १. प्रायः सभी मत सृष्टिका उत्पाद और विनाश मानते हैं, जैनमत ऐसा नहीं मानता-उसके अनुसार जगत् अनादिनिधन है, पर उसमें सुख और शान्तिकी वृद्धि और हानि रूपसे परिवर्तन माना गया है। इसलिये जैनमतानुसार जिस समय सुख और शान्तिमें हानिका रूप नहीं दिखाई दिया था उसको सृष्टिका आदि भाग समझना चाहिये। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4