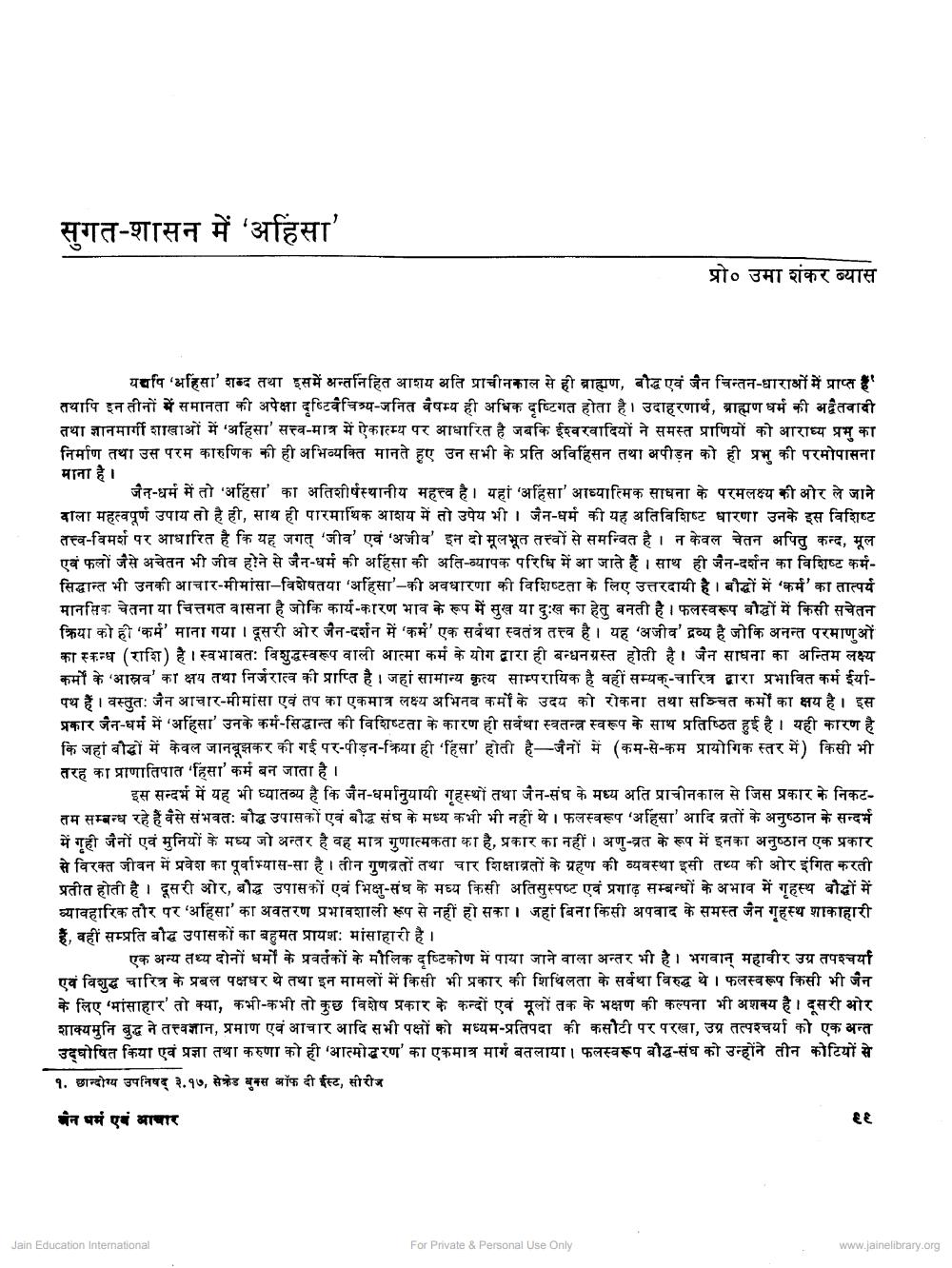Book Title: Sugat Shasan me Ahimsa Author(s): Umashankar Vyas Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 1
________________ सुगत-शासन में 'अहिंसा' प्रो० उमा शंकर ब्यास यद्यपि अहिंसा' शब्द तथा इसमें अन्तनिहित आशय अति प्राचीनकाल से ही ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन चिन्तन-धाराओं में प्राप्त है। तथापि इन तीनों में समानता की अपेक्षा दृष्टिवैचित्र्य-जनित वैषम्य ही अधिक दृष्टिगत होता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण धर्म की अद्वैतवादी तथा ज्ञानमार्गी शाखाओं में 'अहिंसा' सत्त्व-मात्र में एकात्म्य पर आधारित है जबकि ईश्वरवादियों ने समस्त प्राणियों को आराध्य प्रभु का निर्माण तथा उस परम कारुणिक की ही अभिव्यक्ति मानते हुए उन सभी के प्रति अविहिंसन तथा अपीड़न को ही प्रभु की परमोपासना माना है। जैन-धर्म में तो 'अहिंसा' का अतिशीर्षस्थानीय महत्त्व है। यहां 'अहिंसा' आध्यात्मिक साधना के परमलक्ष्य की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण उपाय तो है ही, साथ ही पारमार्थिक आशय में तो उपेय भी। जैन-धर्म की यह अतिविशिष्ट धारणा उनके इस विशिष्ट तत्त्व-विमर्श पर आधारित है कि यह जगत् 'जीव' एवं 'अजीव' इन दो मूलभूत तत्त्वों से समन्वित है। न केवल चेतन अपितु कन्द, मूल एवं फलों जैसे अचेतन भी जीव होने से जैन-धर्म की अहिंसा की अति-व्यापक परिधि में आ जाते हैं । साथ ही जैन-दर्शन का विशिष्ट कर्मसिद्धान्त भी उनकी आचार-मीमांसा-विशेषतया 'अहिंसा' की अवधारणा की विशिष्टता के लिए उत्तरदायी है । बौद्धों में 'कर्म' का तात्पर्य मानसिक चेतना या चित्तगत वासना है जोकि कार्य-कारण भाव के रूप में सुख या दुःख का हेतु बनती है । फलस्वरूप बौद्धों में किसी सचेतन क्रिया को ही 'कर्म' माना गया । दूसरी ओर जैन-दर्शन में 'कर्म' एक सर्वथा स्वतंत्र तत्त्व है। यह 'अजीव' द्रव्य है जोकि अनन्त परमाणुओं का स्कन्ध (राशि) है । स्वभावत: विशुद्धस्वरूप वाली आत्मा कर्म के योग द्वारा ही बन्धन ग्रस्त होती है। जैन साधना का अन्तिम लक्ष्य कर्मों के 'आस्रव' का क्षय तथा निर्जरात्व की प्राप्ति है। जहां सामान्य कृत्य साम्परायिक है वहीं सम्यक्-चारित्र द्वारा प्रभावित कर्म ईर्यापथ हैं । वस्तुतः जैन आचार-मीमांसा एवं तप का एकमात्र लक्ष्य अभिनव कर्मों के उदय को रोकना तथा सञ्चित कर्मों का क्षय है। इस प्रकार जैन-धर्म में 'अहिंसा' उनके कर्म-सिद्धान्त की विशिष्टता के कारण ही सर्वथा स्वतन्त्र स्वरूप के साथ प्रतिष्ठित हुई है। यही कारण है कि जहां बौद्धों में केवल जानबूझकर की गई पर-पीड़न-क्रिया ही 'हिंसा' होती है-जैनों में (कम-से-कम प्रायोगिक स्तर में) किसी भी तरह का प्राणातिपात 'हिंसा' कर्म बन जाता है । इस सन्दर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि जैन-धर्मानुयायी गृहस्थों तथा जैन-संघ के मध्य अति प्राचीनकाल से जिस प्रकार के निकटतम सम्बन्ध रहे हैं वैसे संभवत: बौद्ध उपासकों एवं बौद्ध संघ के मध्य कभी भी नहीं थे। फलस्वरूप 'अहिंसा' आदि व्रतों के अनुष्ठान के सन्दर्भ में गृही जैनों एवं मुनियों के मध्य जो अन्तर है वह मात्र गुणात्मकता का है, प्रकार का नहीं। अणु-व्रत के रूप में इनका अनुष्ठान एक प्रकार से विरक्त जीवन में प्रवेश का पूर्वाभ्यास-सा है । तीन गुणवतों तथा चार शिक्षाव्रतों के ग्रहण की व्यवस्था इसी तथ्य की ओर इंगित करती प्रतीत होती है। दूसरी ओर, बौद्ध उपासकों एवं भिक्षु-संघ के मध्य किसी अतिसुस्पष्ट एवं प्रगाढ़ सम्बन्धों के अभाव में गृहस्थ बौद्धों में व्यावहारिक तौर पर 'अहिंसा' का अवतरण प्रभावशाली रूप से नहीं हो सका। जहां बिना किसी अपवाद के समस्त जैन गृहस्थ शाकाहारी हैं, वहीं सम्प्रति बौद्ध उपासकों का बहुमत प्रायशः मांसाहारी है। एक अन्य तथ्य दोनों धर्मों के प्रवर्तकों के मौलिक दृष्टिकोण में पाया जाने वाला अन्तर भी है। भगवान् महावीर उग्र तपश्चर्या एवं विशुद्ध चारित्र के प्रबल पक्षधर थे तथा इन मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता के सर्वथा विरुद्ध थे। फलस्वरूप किसी भी जैन के लिए 'मांसाहार' तो क्या, कभी-कभी तो कुछ विशेष प्रकार के कन्दों एवं मूलों तक के भक्षण की कल्पना भी अशक्य है। दूसरी ओर शाक्यमुनि बुद्ध ने तत्त्वज्ञान, प्रमाण एवं आचार आदि सभी पक्षों को मध्यम-प्रतिपदा की कसौटी पर परखा, उग्र तत्पश्चर्या को एक अन्त उद्घोषित किया एवं प्रज्ञा तथा करुणा को ही 'आत्मोद्धरण' का एकमात्र मार्ग बतलाया। फलस्वरूप बौद्ध-संघ को उन्होंने तीन कोटियों से १. छान्दोग्य उपनिषद् ३.१७, सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट, सीरीज जैन धर्म एवं आचार Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4