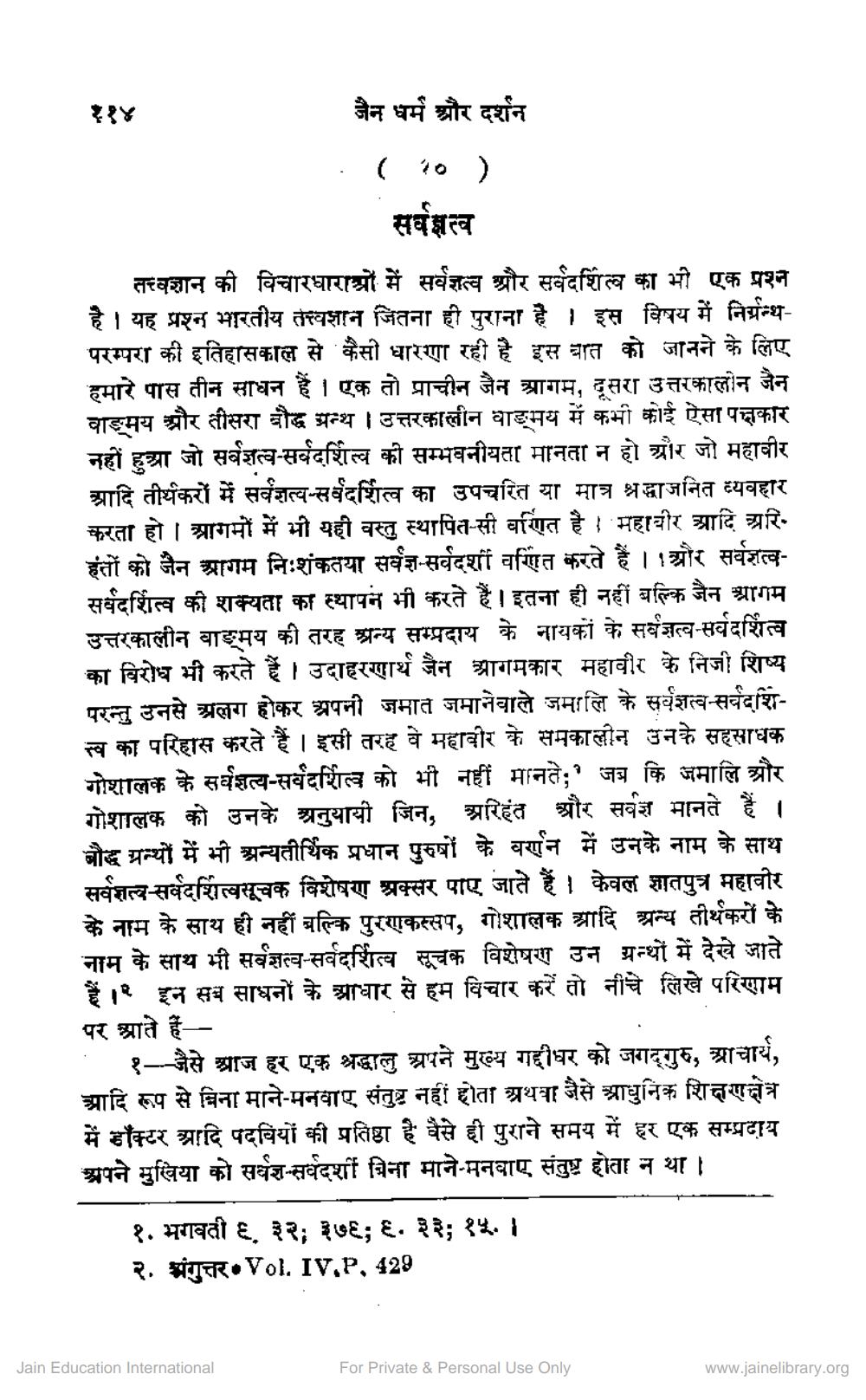Book Title: Sarvagnatva Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Darshan_aur_Chintan_Part_1_2_002661.pdf View full book textPage 1
________________ ११४ जैन धर्म और दर्शन ( 10 ) सर्वज्ञत्व तत्वज्ञान की विचारधाराओं में सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व का भी एक प्रश्न है । यह प्रश्न भारतीय तत्त्वज्ञान जितना ही पुराना है । इस विषय में निर्ग्रन्थपरम्परा की इतिहासकाल से कैसी धारणा रही है इस बात को जानने के लिए हमारे पास तीन साधन हैं। एक तो प्राचीन जैन श्रागम, दूसरा उत्तरकालीन जैन वाङ्मय और तीसरा बौद्ध ग्रन्थ । उत्तरकालीन वाङ्मय में कभी कोई ऐसा पक्षकार नहीं हुआ जो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व की सम्भवनीयता मानता न हो और जो महावीर आदि तीर्थकरों में सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व का उपचरित या मात्र श्रद्धाजनित व्यवहार करता हो । श्रागमों में भी यही वस्तु स्थापित-सी वर्णित है। महावीर आदि रि हंतों को जैन आगम निःशंकतया सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वर्णित करते हैं । 1 और सर्वज्ञत्वसर्वदर्शित्व की शक्यता का स्थापन भी करते हैं । इतना ही नहीं बल्कि जैन श्रागम उत्तरकालीन वाङ्मय की तरह अन्य सम्प्रदाय के नायकों के सर्वज्ञत्व- सर्व दर्शित्व का विरोध भी करते हैं । उदाहरणार्थ जैन श्रागमकार महावीर के निजी शिष्य परन्तु उनसे अलग होकर अपनी जमात जमानेवाले जमालि के सर्वशत्व- सर्वदर्शिस्व का परिहास करते हैं। इसी तरह वे महावीर के समकालीन उनके सहसाधक गोशालक के सर्वशत्य- सर्वदर्शित्व को भी नहीं मानते; ' जब कि जमालि और गोशालक को उनके अनुयायी जिन, अरिहंत और सर्वज्ञ मानते हैं । बौद्ध ग्रन्थों में भी अन्यतीर्थिक प्रधान पुरुषों के वर्णन में उनके नाम के साथ सर्वशत्व सर्वदर्शित्वसूचक विशेषण अक्सर पाए जाते हैं। केवल ज्ञातपुत्र महावीर के नाम के साथ ही नहीं बल्कि पुरणकस्सप, गोशालक आदि अन्य तीर्थकरों के नाम के साथ भी सर्वज्ञत्व- सर्वदर्शित्व सूचक विशेषण उन ग्रन्थों में देखे जाते हैं । इन सब साधनों के आधार से हम विचार करें तो नीचे लिखे परिणाम पराते हैं १ - जैसे आज हर एक श्रद्धालु अपने मुख्य गद्दीधर को जगद्गुरु, प्राचार्य, आदि रूप से बिना माने- मनवाए संतुष्ट नहीं होता अथवा जैसे आधुनिक शिक्षणक्षेत्र में डॉक्टर आदि पदवियों की प्रतिष्ठा है वैसे ही पुराने समय में हर एक सम्प्रदाय अपने मुखिया को सर्वज्ञ - सर्वदर्शी बिना माने- मनवाए संतुष्ट होता न था । १. भगवती ६, ३२, ३७६; ६.३३; १५. । २. अंगुत्तर• Vol. IV. P. 429 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2