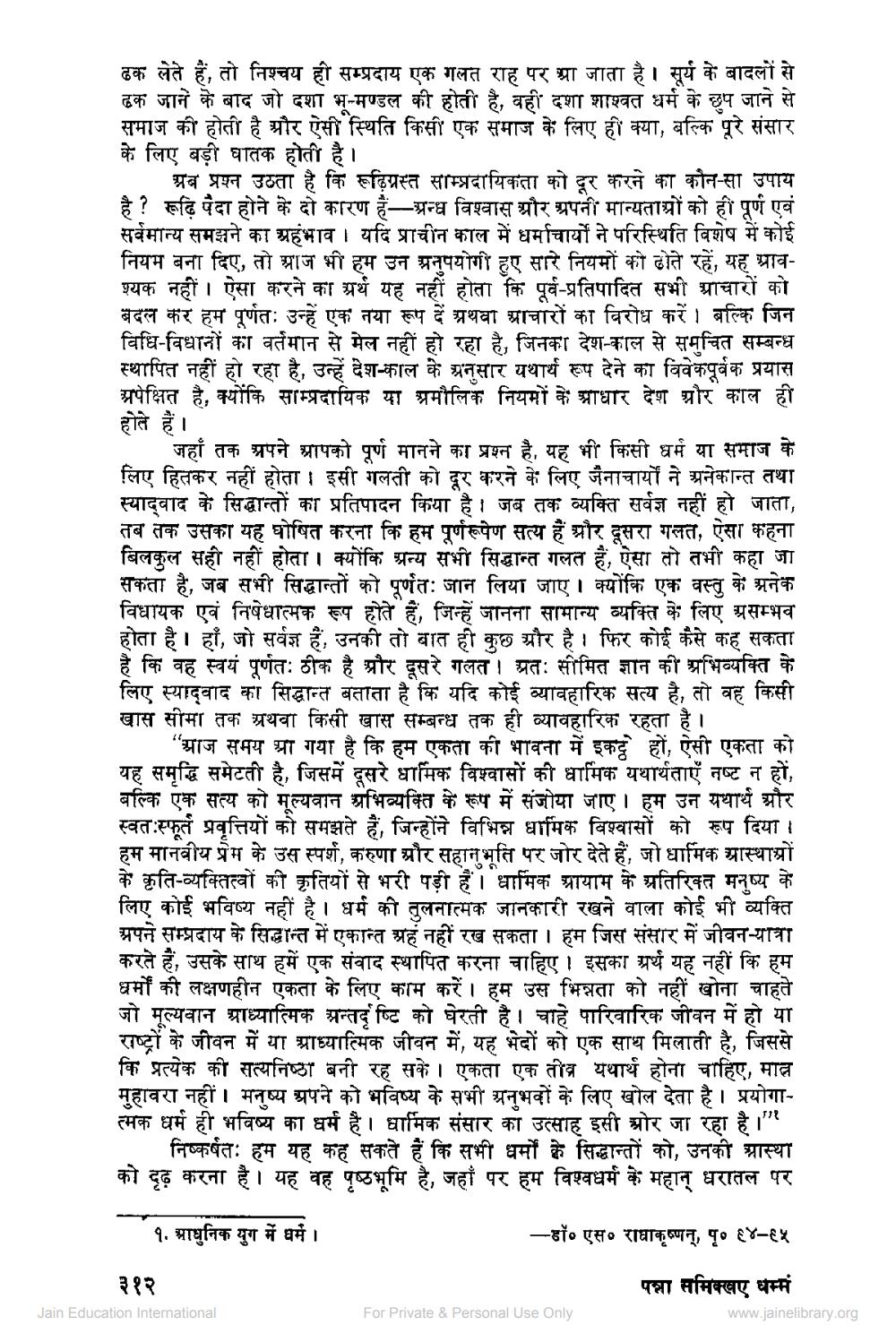Book Title: Sarv Dharm Samanvay Anagrah Drushti Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 2
________________ ढक लेते हैं, तो निश्चय ही सम्प्रदाय एक गलत राह पर आ जाता है। सूर्य के बादलों से ढक जाने के बाद जो दशा भू-मण्डल की होती है, वहीं दशा शाश्वत धर्म के छुप जाने से समाज की होती है और ऐसी स्थिति किसी एक समाज के लिए ही क्या, बल्कि पूरे संसार के लिए बड़ी घातक होती है। अब प्रश्न उठता है कि रूढ़िग्रस्त साम्प्रदायिकता को दूर करने का कौन-सा उपाय है ? रूढ़ि पैदा होने के दो कारण है-अन्ध विश्वास और अपनी मान्यतानों को ही पूर्ण एवं सर्वमान्य समझने का अहंभाव । यदि प्राचीन काल में धर्माचार्यों ने परिस्थिति विशेष में कोई नियम बना दिए, तो आज भी हम उन अनुपयोगी हुए सारे नियमों को ढोते रहें, यह प्रावश्यक नहीं। ऐसा करने का अर्थ यह नहीं होता कि पूर्व-प्रतिपादित सभी प्राचारों को बदल कर हम पूर्णतः उन्हें एक नया रूप दें अथवा आचारों का विरोध करें। बल्कि जिन विधि-विधानों का वर्तमान से मेल नहीं हो रहा है, जिनका देश-काल से समुचित सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है, उन्हें देश-काल के अनुसार यथार्थ रूप देने का विवेकपूर्वक प्रयास अपेक्षित है, क्योंकि साम्प्रदायिक या अमौलिक नियमों के आधार देश और काल ही होते हैं। जहाँ तक अपने आपको पूर्ण मानने का प्रश्न है, यह भी किसी धर्म या समाज के लिए हितकर नहीं होता। इसी गलती को दूर करने के लिए जैनाचार्यों ने अनेकान्त तथा स्याद्वाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जब तक व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो जाता, तब तक उसका यह घोषित करना कि हम पूर्णरूपेण सत्य है और दूसरा गलत, ऐसा कहना बिलकुल सही नहीं होता। क्योंकि अन्य सभी सिद्धान्त गलत है, ऐसा तो तभी कहा जा सकता है, जब सभी सिद्धान्तों को पूर्णतः जान लिया जाए। क्योंकि एक वस्तु के अनेक विधायक एवं निषेधात्मक रूप होते हैं, जिन्हें जानना सामान्य व्यक्ति के लिए असम्भव होता है। हाँ, जो सर्वज्ञ हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि वह स्वयं पूर्णत: ठीक है और दसरे गलत। अतः सीमित ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए स्याद्वाद का सिद्धान्त बताता है कि यदि कोई व्यावहारिक सत्य है, तो वह किसी खास सीमा तक अथवा किसी खास सम्बन्ध तक ही व्यावहारिक रहता है। "आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में इकट्ठे हों, ऐसी एकता को यह समृद्धि समेटती है, जिसमें दूसरे धार्मिक विश्वासों की धार्मिक यथार्थताएँ नष्ट न हों, बल्कि एक सत्य को मूल्यवान अभिव्यक्ति के रूप में संजोया जाए। हम उन यथार्थ और स्वतःस्फूर्त प्रवृत्तियों को समझते हैं, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक विश्वासों को रूप दिया । हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं, जो धार्मिक आस्थाओं के कृति-व्यक्तित्वों की कृतियों से भरी पड़ी है। धार्मिक अायाम के अतिरिक्त मनष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धर्म की तुलनात्मक जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में एकान्त अहं नहीं रख सकता। हम जिस संसार में जीवन-यात्रा करते हैं, उसके साथ हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम उस भिन्नता को नहीं खोना चाहते जो मूल्यवान आध्यात्मिक अन्तर्दष्टि को घेरती है। चाहे पारिवारिक जीवन में हो या राष्ट्रों के जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक की सत्यनिष्ठा बनी रह सके। एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मान्न मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धर्म ही भविष्य का धर्म है। धार्मिक संसार का उत्साह इसी ओर जा रहा है।" निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सभी धर्मों के सिद्धान्तों को, उनकी आस्था को दृढ़ करना है। यह वह पृष्ठभूमि है, जहाँ पर हम विश्वधर्म के महान् धरातल पर १. आधुनिक युग में धर्म। -डॉ. एस. राधाकृष्णन्, पृ० ६४-६५ पन्ना समिक्खए धम्म Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3