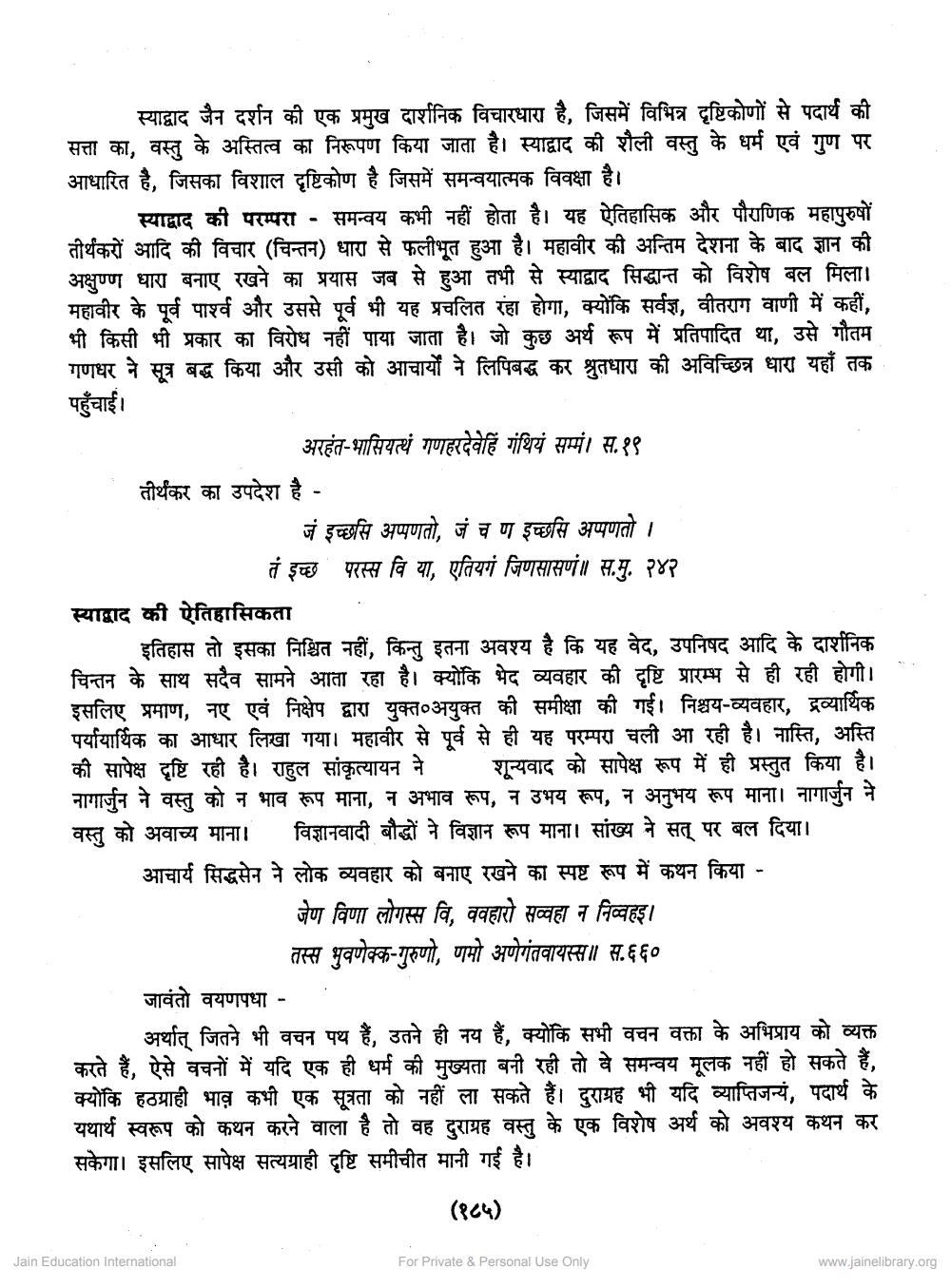Book Title: Samanvaya ka Marg Syadwad Author(s): Udaychandra Jain Publisher: Z_Mahasati_Dway_Smruti_Granth_012025.pdf View full book textPage 2
________________ स्याद्वाद जैन दर्शन की एक प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थ की सत्ता का, वस्तु के अस्तित्व का निरूपण किया जाता है। स्याद्वाद की शैली वस्तु के धर्म एवं गुण पर आधारित है, जिसका विशाल दृष्टिकोण है जिसमें समन्वयात्मक विवक्षा है। स्यावाद की परम्परा - समन्वय कभी नहीं होता है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों तीर्थंकरों आदि की विचार (चिन्तन) धारा से फलीभूत हुआ है। महावीर की अन्तिम देशना के बाद ज्ञान की अक्षुण्ण धारा बनाए रखने का प्रयास जब से हुआ तभी से स्याद्वाद सिद्धान्त को विशेष बल मिला। महावीर के पूर्व पार्श्व और उससे पूर्व भी यह प्रचलित रहा होगा, क्योंकि सर्वज्ञ, वीतराग वाणी में कहीं, भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं पाया जाता है। जो कुछ अर्थ रूप में प्रतिपादित था, उसे गौतम गणधर ने सूत्र बद्ध किया और उसी को आचार्यों ने लिपिबद्ध कर श्रुतधारा की अविच्छिन्न धारा यहाँ तक पहुँचाई। अरहंत-भासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्म। स.१९ तीर्थंकर का उपदेश है - जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणतो । तं इच्छ परस्स वि या, एतियगं जिणसासणं॥ स.मु. २४२ स्यावाद की ऐतिहासिकता इतिहास तो इसका निश्चित नहीं, किन्तु इतना अवश्य है कि यह वेद, उपनिषद आदि के दार्शनिक चिन्तन के साथ सदैव सामने आता रहा है। क्योंकि भेद व्यवहार की दष्टि प्रारम्भ से ही रही होगी। इसलिए प्रमाण, नए एवं निक्षेप द्वारा युक्त०अयुक्त की समीक्षा की गई। निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का आधार लिखा गया। महावीर से पूर्व से ही यह परम्परा चली आ रही है। नास्ति, अस्ति की सापेक्ष दृष्टि रही है। राहुल सांकृत्यायन ने शून्यवाद को सापेक्ष रूप में ही प्रस्तुत किया है। नागार्जुन ने वस्तु को न भाव रूप माना, न अभाव रूप, न उभय रूप, न अनुभय रूप माना। नागार्जुन ने वस्तु को अवाच्य माना। विज्ञानवादी बौद्धों ने विज्ञान रूप माना। सांख्य ने सत् पर बल दिया। आचार्य सिद्धसेन ने लोक व्यवहार को बनाए रखने का स्पष्ट रूप में कथन किया - जेण विणा लोगस्स वि, ववहारो सव्वहा न निव्वहइ। तस्स भुवणेक्क-गुरुणो, णमो अणेगंतवायस्स॥ स.६६० जावंतो वयणपधा - अर्थात् जितने भी वचन पथ हैं, उतने ही नय हैं, क्योंकि सभी वचन वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं, ऐसे वचनों में यदि एक ही धर्म की मुख्यता बनी रही तो वे समन्वय मूलक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हठयाही भाव कभी एक सूत्रता को नहीं ला सकते हैं। दुराग्रह भी यदि व्याप्तिजन्यं, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कथन करने वाला है तो वह दुराग्रह वस्तु के एक विशेष अर्थ को अवश्य कथन कर सकेगा। इसलिए सापेक्ष सत्यग्राही दृष्टि समीचीत मानी गई है। (१८५) Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5