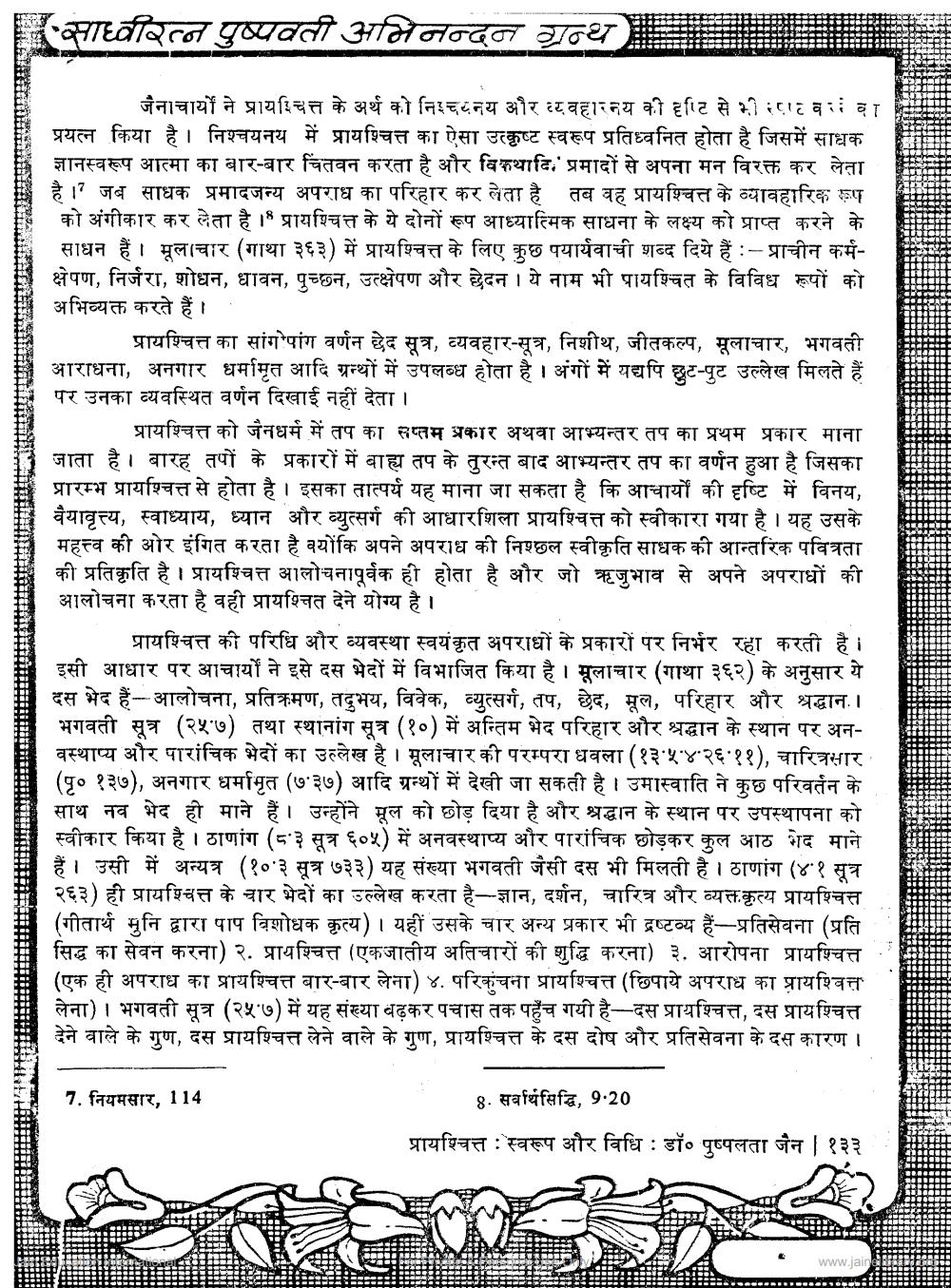Book Title: Prayaschitta swarup aur Vidhi Author(s): Pushpalata Jain Publisher: Z_Sadhviratna_Pushpvati_Abhinandan_Granth_012024.pdf View full book textPage 2
________________ 1. साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ जैनाचार्यों ने प्रायश्चित्त के अर्थ को निश्चयनय और व्यवहारनय की दृष्टि से भी पटवा प्रयत्न किया है । निश्चयनय में प्रायश्चित्त का ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिध्वनित होता है जिसमें साधक ज्ञानस्वरूप आत्मा का बार-बार चितवन करता है और विरुथादि प्रमादों से अपना मन विरक्त कर लेता 17 जब साधक प्रमादजन्य अपराध का परिहार कर लेता है तब वह प्रायश्चित्त के व्यावहारिक रूप को अंगीकार कर लेता है ।" प्रायश्चित्त के ये दोनों रूप आध्यात्मिक साधना के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं। मूल(चार (गाथा ३६३) में प्रायश्चित्त के लिए कुछ पयार्यवाची शब्द दिये हैं :- प्राचीन कर्मक्षेपण, निर्जरा, शोधन, धावन, पुच्छन, उत्क्षेपण और छेदन । ये नाम भी प्रायश्चित के विविध रूपों को अभिव्यक्त करते हैं । प्रायश्चित्त का सांगोपांग वर्णन छेद सूत्र, व्यवहार-सूत्र, निशीथ, जीतकल्प, मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । अंगों में यद्यपि छुट-पुट उल्लेख मिलते हैं पर उनका व्यवस्थित वर्णन दिखाई नहीं देता । प्रायश्चित्त को जैनधर्म में तप का सप्तम प्रकार अथवा आभ्यन्तर तप का प्रथम प्रकार माना जाता है । बारह तपों के प्रकारों में बाह्य तप के तुरन्त बाद आभ्यन्तर तप का वर्णन हुआ है जिसका प्रारम्भ प्रायश्चित्त से होता है। इसका तात्पर्य यह माना जा सकता है कि आचार्यों की दृष्टि में विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग की आधारशिला प्रायश्चित्त को स्वीकारा गया है । यह उसके महत्त्व की ओर इंगित करता है क्योंकि अपने अपराध की निश्छल स्वीकृति साधक की आन्तरिक पवित्रता की प्रतिकृति है । प्रायश्चित्त आलोचनापूर्वक ही होता है और जो ऋजुभाव से अपने अपराधों की आलोचना करता है वही प्रायश्चित देने योग्य है । प्रायश्चित्त की परिधि और व्यवस्था स्वयंकृत अपराधों के प्रकारों पर निर्भर रहा करती है । इसी आधार पर आचार्यों ने इसे दस भेदों में विभाजित किया है । मूलाचार ( गाथा ३६२ ) के अनुसार ये दस भेद हैं- आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । भगवती सूत्र ( २५७) तथा स्थानांग सूत्र (१०) में अन्तिम भेद परिहार और श्रद्धान के स्थान पर अनवस्थाप्य और पारांचिक भेदों का उल्लेख है । मूलाचार की परम्परा धवला (१३५४ २६ ११), चारित्रसार (पृ० १३७), अनगार धर्मामृत (७३७) आदि ग्रन्थों में देखी जा सकती है । उमास्वाति ने कुछ परिवर्तन के साथ नव भेद ही माने हैं। उन्होंने मूल को छोड़ दिया है और श्रद्धान के स्थान पर उपस्थापना को स्वीकार किया है । ठाणांग (८३ सूत्र ६०५ ) में अनवस्थाप्य और पारांचिक छोड़कर कुल आठ भेद माने हैं । उसी में अन्यत्र ( १० ३ सूत्र ७३३ ) यह संख्या भगवती जैसी दस भी मिलती है। ठाणांग (४१ सूत्र २६३) ही प्रायश्चित्त के चार भेदों का उल्लेख करता है - ज्ञान, दर्शन, चारित्र और व्यक्तकृत्य प्रायश्चित्त ( गीतार्थ मुनि द्वारा पाप विशोधक कृत्य ) । यहीं उसके चार अन्य प्रकार भी द्रष्टव्य हैं - प्रतिसेवना ( प्रति सिद्ध का सेवन करना) २. प्रायश्चित्त ( एकजातीय अतिचारों की शुद्धि करना) ३. आरोपना प्रायश्चित्त ( एक ही अपराध का प्रायश्चित्त बार-बार लेना ) ४. परिकुंचना प्रायश्चित्त ( छिपाये अपराध का प्रायश्वित्त लेना) | भगवती सूत्र ( २५७) में यह संख्या बढ़कर पचास तक पहुँच गयी है - दस प्रायश्चित्त, दस प्रायश्चित्त देने वाले के गुण, दस प्रायश्चित्त लेने वाले के गुण, प्रायश्चित्त के दस दोष और प्रतिसेवना के दस कारण । 7. नियमसार, 114 8. aafafafa, 9.20 प्रायश्चित्त: स्वरूप और विधि : डॉ० पुष्पलता जैन | १३३ www.jaindPage Navigation
1 2 3 4 5 6