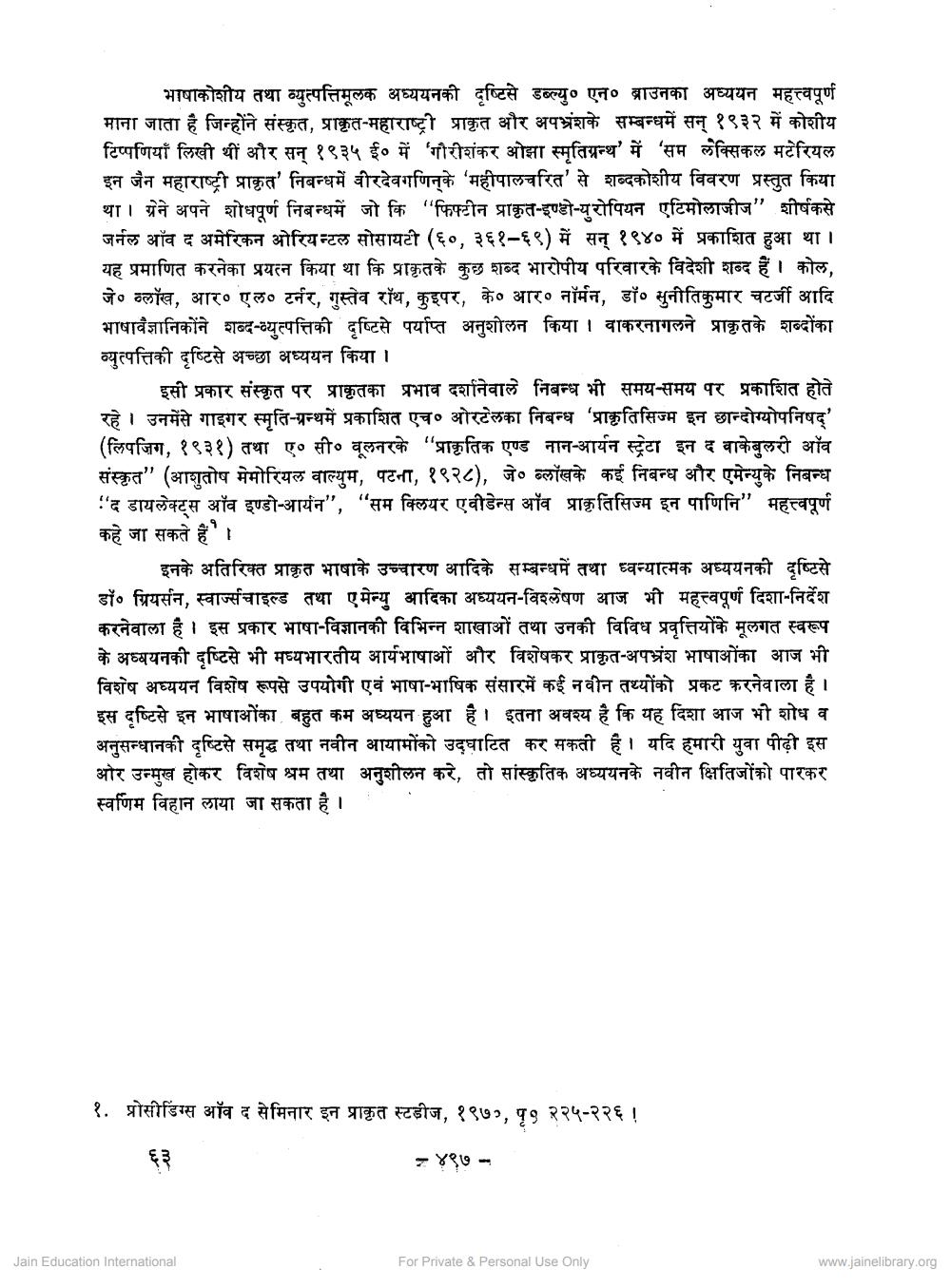Book Title: Prakrit tatha Apbhramsa Shodh me Karya ki Dishaye Author(s): Devendra Kumar Jain Publisher: Z_Kailashchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012048.pdf View full book textPage 7
________________ भाषाकोशीय तथा व्युत्पत्तिमूलक अध्ययनकी दृष्टिसे डब्ल्यु० एन० ब्राउनका अध्ययन महत्त्वपूर्ण माना जाता है जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत-महाराष्ट्री प्राकृत और अपभ्रंशके सम्बन्धमें सन् 1932 में कोशीय टिप्पणियाँ लिखी थीं और सन् 1935 ई० में 'गौरीशंकर ओझा स्मृतिग्रन्थ' में 'सम लेक्सिकल मटेरियल इन जैन महाराष्ट्री प्राकृत' निबन्धमें वीरदेवगणिन्के 'महीपालचरित' से शब्दकोशीय विवरण प्रस्तुत किया था। ग्रेने अपने शोधपूर्ण निबन्धमें जो कि "फिफ्टीन प्राकृत-इण्डो-युरोपियन एटिमोलाजीज" शीर्षकसे जर्नल ऑव द अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी (60, 361-69) में सन् 1940 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया था कि प्राकृतके कुछ शब्द भारोपीय परिवारके विदेशी शब्द हैं / कोल, जे० लाख, आर० एल० टर्नर, गुस्तेव रॉथ, कुइपर, के० आर० नॉर्मन, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी आदि जानिकोंने शब्द-व्यत्पत्तिकी दष्टिसे पर्याप्त अनुशीलन किया। वाकरनागलने प्राकृतके शब्दोंका व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अच्छा अध्ययन किया / इसी प्रकार संस्कृत पर प्राकृतका प्रभाव दर्शानेवाले निबन्ध भी समय-समय पर प्रकाशित होते रहे। उनमेंसे गाइगर स्मृति-ग्रन्थमें प्रकाशित एच० ओरटेलका निबन्ध 'प्राकृतिसिज्म इन छान्दोग्योपनिषद्' (लिपजिग, 1931) तथा ए० सी० वूलनरके "प्राकृतिक एण्ड नान-आर्यन स्ट्रेटा इन द वाकेबुलरी ऑव संस्कृत" (आशुतोष मेमोरियल वाल्युम, पटना, 1928), जे. ब्लॉखके कई निबन्ध और एमेन्युके निबन्ध :"द डायलेक्टस ऑव इण्डो-आर्यन", "सम क्लियर एवीडेन्स ऑव प्राकृतिसिज्म इन पाणिनि" महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृत भाषाके उच्चारण आदिके सम्बन्धमें तथा ध्वन्यात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे डॉ० ग्रियर्सन, स्वार्क्सचाइल्ड तथा एमेन्यु आदिका अध्ययन-विश्लेषण आज भी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश करनेवाला है। इस प्रकार भाषा-विज्ञानकी विभिन्न शाखाओं तथा उनकी विविध प्रवृत्तियोंके मूलगत स्वरूप के अध्ययनकी दृष्टिसे भी मध्यभारतीय आर्यभाषाओं और विशेषकर प्राकृत-अपभ्रंश भाषाओंका आज भी विशेष अध्ययन विशेष रूपसे उपयोगी एवं भाषा-भाषिक संसारमें कई नवीन तथ्योंको प्रकट करनेवाला है। इस दृष्टिसे इन भाषाओंका बहुत कम अध्ययन हुआ है। इतना अवश्य है कि यह दिशा आज भी शोध व अनुसन्धानकी दृष्टिसे समृद्ध तथा नवीन आयामोंको उद्घाटित कर सकती है। यदि हमारी युवा पीढ़ी इस ओर उन्मुख होकर विशेष श्रम तथा अनुशीलन करे, तो सांस्कृतिक अध्ययनके नवीन क्षितिजोंको पारकर स्वर्णिम विहान लाया जा सकता है। 1. प्रोसीडिंग्स ऑव द सेमिनार इन प्राकृत स्टडीज, 1970, 19225-226 / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7