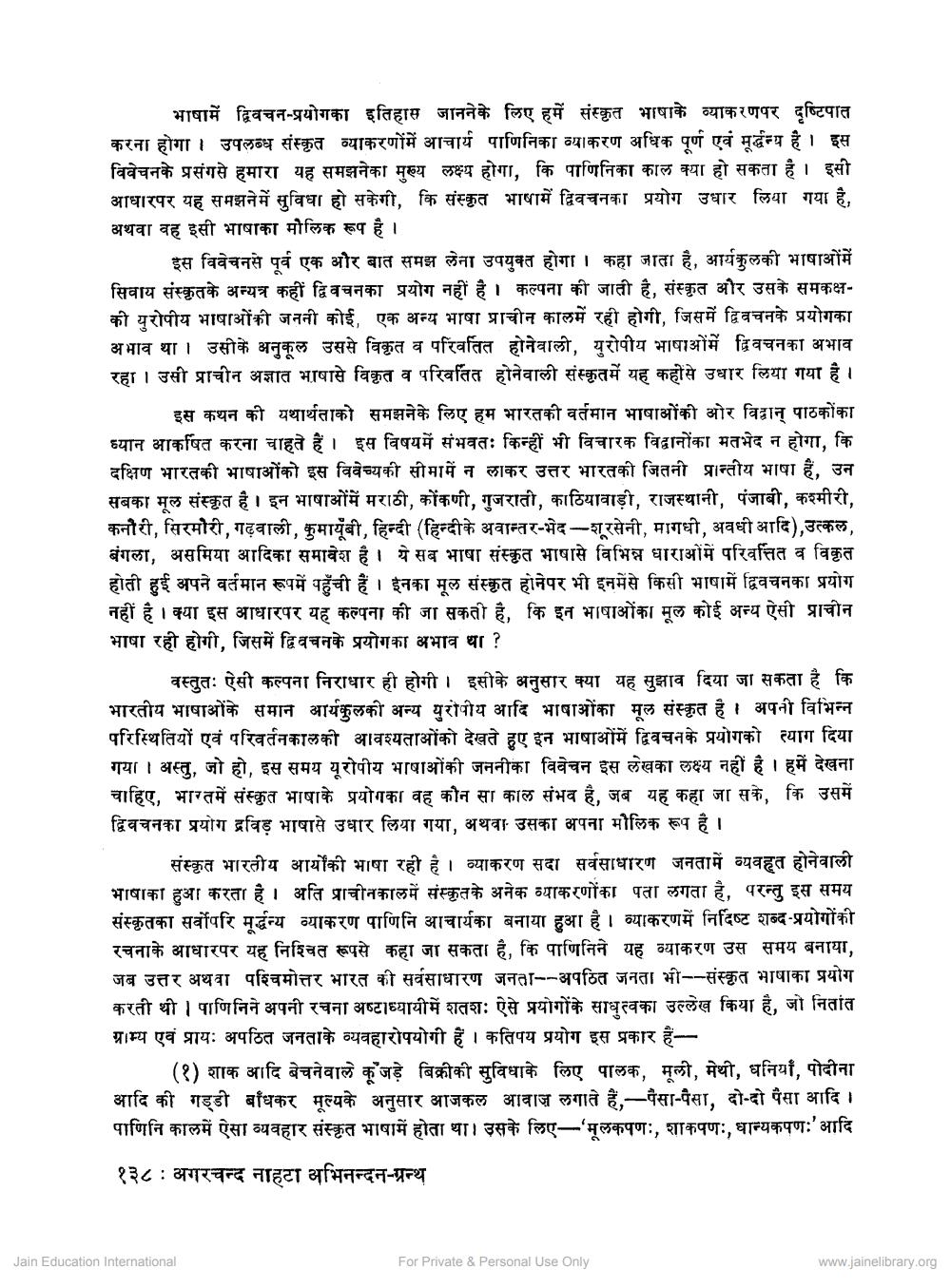Book Title: Paninikal evam Sanskrut me Dwivachan Author(s): Udayvir Shastri Publisher: Z_Nahta_Bandhu_Abhinandan_Granth_012007.pdf View full book textPage 2
________________ भाषा में द्विवचन प्रयोगका इतिहास जाननेके लिए हमें संस्कृत भाषाके व्याकरणपर दृष्टिपात करना होगा । उपलब्ध संस्कृत व्याकरणोंमें आचार्य पाणिनिका व्याकरण अधिक पूर्ण एवं मूव है। इस विवेचनके प्रसंगसे हमारा यह समझनेका मुख्य लक्ष्य होगा, कि पाणिनिका काल क्या हो सकता है । इसी आधारपर यह समझने में सुविधा हो सकेगी, कि संस्कृत भाषामें द्विवचनका प्रयोग उधार लिया गया है, अथवा वह इसी भाषाका मौलिक रूप है । इस विवेचनसे पूर्व एक और बात समझ लेना उपयुक्त होगा। कहा जाता है, आर्यकुलकी भाषाओं में सिवाय संस्कृतके अन्यत्र कहीं द्विवचनका प्रयोग नहीं है । कल्पना की जाती है, संस्कृत और उसके समकक्षकी युरोपीय भाषाओं की जननी कोई एक अन्य भाषा प्राचीन कालमें रही होगी, जिसमें द्विवचनके प्रयोगका अभाव था। उसी के अनुकूल उससे विकृत व परिवर्तित होनेवाली यूरोपीय भाषाओं में द्विवचनका अभाव रहा । उसी प्राचीन अज्ञात भाषासे विकृत व परिवर्तित होनेवाली संस्कृत में यह कहीं से उधार लिया गया है । इस कथन की यथार्थताको समझने के लिए हम भारतकी वर्तमान भाषाओंकी ओर विद्वान् पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । इस विषय में संभवतः किन्हीं भी विचारक विद्वानोंका मतभेद न होगा, कि दक्षिण भारतकी भाषाओंको इस विवेच्य की सीमा में न लाकर उत्तर भारतकी जितनी प्रान्तीय भाषा हैं, उन सबका मूल संस्कृत है। इन भाषाओं में मराठी, कोंकणी, गुजराती, काठियावाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी, कनौरी, सिरमौरी, गढ़वाली, कुमायूँबी, हिन्दी (हिन्दी के अवान्तर भेव शूरसेनी, मागधी, अवधी आदि), उत्कल, बंगला, असमिया आदिका समावेश है। ये सब भाषा संस्कृत भाषासे विभिन्न धाराओं में परिवर्तित व विकृत होती हुई अपने वर्तमान रूपमें पहुँची हैं। इनका मूल संस्कृत होनेपर भी इनमें से किसी भाषा में द्विवचनका प्रयोग नहीं है । क्या इस आधारपर यह कल्पना की जा सकती है, कि इन भाषाओंका मूल कोई अन्य ऐसी प्राचीन भाषा रही होगी, जिसमें द्विवचनके प्रयोगका अभाव था ? वस्तुतः ऐसी कल्पना निराधार ही होगी । इसीके अनुसार क्या यह सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय भाषाओं के समान आर्यकुलकी अन्य युरोपीय आदि भाषाओंका मूल संस्कृत है । अपनी विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवर्तनकालकी आवश्यताओंको देखते हुए इन भाषाओंमें द्विवचनके प्रयोगको त्याग दिया गया। अस्तु, जो हो, इस समय यूरोपीय भाषाओंकी जननीका विवेचन इस लेखका लक्ष्य नहीं है। हमें देखना चाहिए, भारतमें संस्कृत भाषाके प्रयोगका वह कौन सा काल संभव है, जब यह कहा जा सके, कि उसमें द्विवचनका प्रयोग द्रविड़ भाषासे उधार लिया गया, अथवा उसका अपना मौलिक रूप है । संस्कृत भारतीय आर्योंकी भाषा रही है । व्याकरण सदा सर्वसाधारण जनता में व्यवहृत होनेवाली भाषाका हुआ करता है। अति प्राचीनकालने संस्कृतके अनेक व्याकरणोंका पता लगता है, परन्तु इस समय संस्कृतका सर्वोपरि मूर्द्धन्य व्याकरण पाणिनि आचार्यका बनाया हुआ है। व्याकरण में निर्दिष्ट शब्द प्रयोगों की रचना के आधारपर यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, कि पाणिनिने यह व्याकरण उस समय बनाया, जब उत्तर अथवा पश्चिमोत्तर भारत की सर्वसाधारण जनता अपठित जनता भी संस्कृत भाषाका प्रयोग करती थी । पाणिनिने अपनी रचना अष्टाध्यायी में शतशः ऐसे प्रयोगों के साधुत्वका उल्लेख किया है, जो नितांत ग्राम्य एवं प्रायः अपठित जनताके व्यवहारोपयोगी हैं । कतिपय प्रयोग इस प्रकार हैं ― (१) शाक आदि बेचनेवाले कूंजड़े बिक्रीकी सुविधाके लिए पालक, मूली, मेथी, धनियाँ, पोदीना आदि की गड्डी बांधकर मूल्यके अनुसार आजकल आवाज लगाते हैं, पैसा-पैसा, दो-दो पैसा आदि । पाणिनि कालमें ऐसा व्यवहार संस्कृत भाषामें होता था। उसके लिए - 'मूलकपणः, शाकपणः, धान्यकपणः ' आदि १३८ अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6