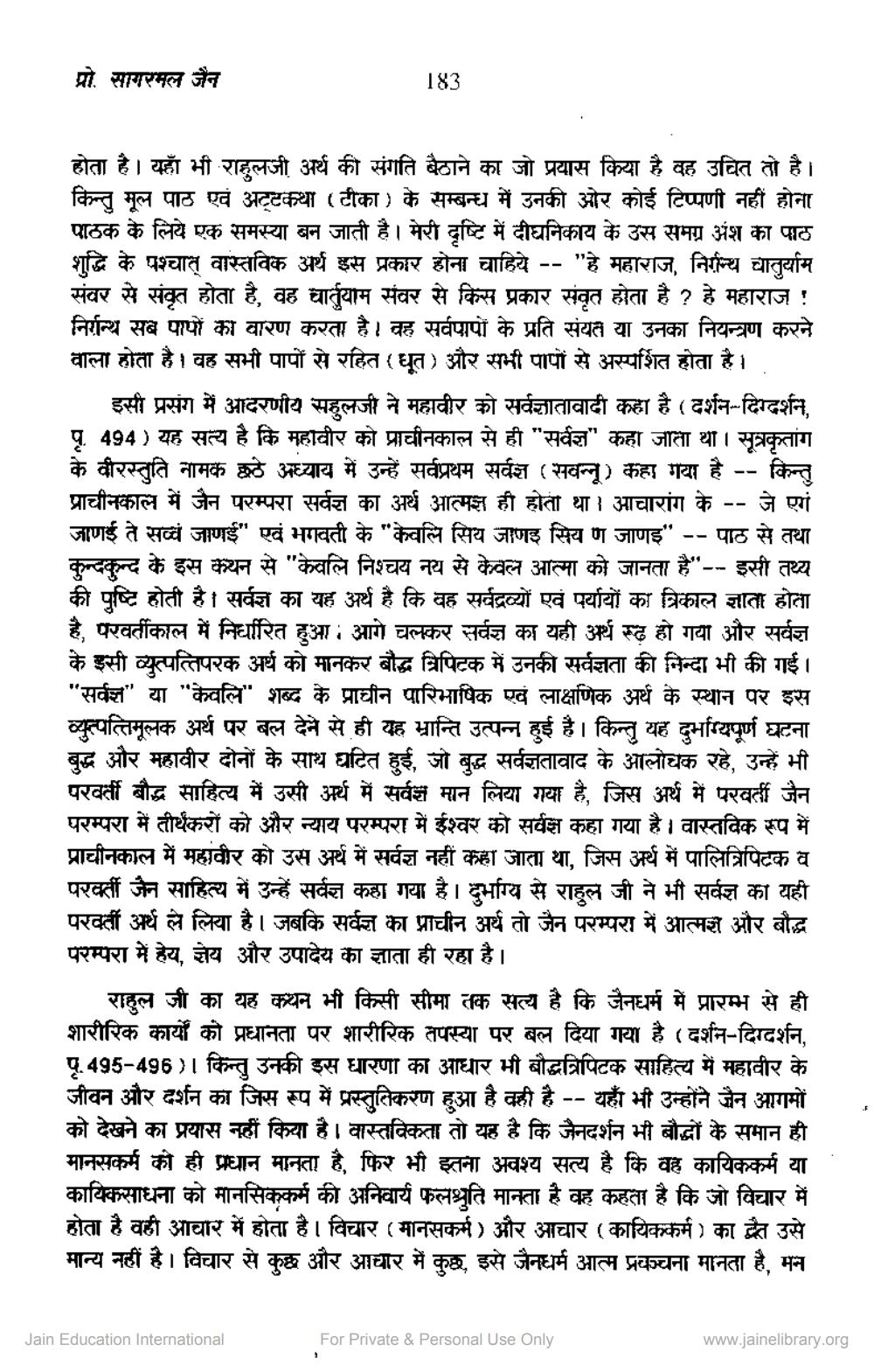Book Title: Maha Pundit Rahul Sankrutyayan ke Jain Dharm Sambandhi Mantavyo ki Samalochna Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sagar_Jain_Vidya_Bharti_Part_1_001684.pdf View full book textPage 5
________________ प्रो. सागरमल जैन 183 होता है। यहाँ भी राहुलजी अर्थ की संगति बैठाने का जो प्रयास किया है वह उचित तो है। किन्तु मूल पाठ एवं अट्टकथा ( टीका ) के सम्बन्ध में उनकी ओर कोई टिप्पणी नहीं होना पाठक के लिये एक समस्या बन जाती है। मेरी दृष्टि में दीघनिकाय के उस समग्न अंश का पाठ शुद्धि के पश्चात् वास्तविक अर्थ इस प्रकार होना चाहिये -- "हे महाराज, निन्थि चातुर्याम संवर से संकृत होता है, वह चार्तुयाम संवर से किस प्रकार संवृत होता है ? हे महाराज : निर्गन्थ सब पापों का वारण करता है। वह सर्वपापों के प्रति संयत या उनका नियन्त्रण करने वाला होता है। वह सभी पापों से रहित (धूत) और सभी पापों से अस्पर्शित होता है। इसी प्रसंग में आदरणीय सहुलजी ने महावीर को सर्वज्ञातावादी कहा है (दर्शन-दिग्दर्शन, पृ. 494) यह सत्य है कि महावीर को प्राचीनकाल से ही "सर्वज्ञ" कहा जाता था। सूत्रकृतांग के वीरस्तुति नामक छठे अध्याय में उन्हें सर्वप्रथम सर्वज्ञ (सवन्नू) कहा गया है -- किन्तु प्राचीनकाल में जैन परम्परा सर्वज्ञ का अर्थ आत्मज्ञ ही होता था। आचारांग के -- जे एगं जाणई ते सव्वं जाणई" एवं भगवती के "केवलि सिय जाणइ सिय ण जाणई" -- पाठ से तथा कुन्दकुन्द के इस कथन से "केवलि निश्चय नय से केवल आत्मा को जानता है"-- इसी तथ्य की पुष्टि होती है। सर्वज्ञ का यह अर्थ है कि वह सर्वद्रव्यों एवं पर्यायों का त्रिकाल ज्ञाता होता है, परवर्तीकाल में निर्धारित हुआ : आगे चलकर सर्वज्ञ का यही अर्थ स्ढ़ हो गया और सर्वज्ञ के इसी व्युत्पत्तिपरक अर्थ को मानकर बौद्ध त्रिपिटक में उनकी सर्वज्ञता की निन्दा भी की गई। "सर्वज्ञ" या "केवलि" शब्द के प्राचीन पारिभाषिक एवं लाक्षणिक अर्थ के स्थान पर इस व्युत्पत्तिमूलक अर्थ पर बल देने से ही यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बुद्ध और महावीर दोनों के साथ घटित हुई, जो बुद्ध सर्वज्ञतावाद के आलोचक रहे, उन्हें भी परवर्ती बौद्ध साहित्य में उसी अर्थ में सर्वज्ञ मान लिया गया है, जिस अर्थ में परवर्ती जैन परम्परा में तीर्थंकरों को और न्याय परम्परा में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है। वास्तविक रूप में प्राचीनकाल में महावीर को उस अर्थ में सर्वज्ञ नहीं कहा जाता था, जिस अर्थ में पालित्रिपिटक व परवर्ती जैन साहित्य में उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है। दुर्भाग्य से राहुल जी ने भी सर्वज्ञ का यही परवती अर्थ ले लिया है। जबकि सर्वज्ञ का प्राचीन अर्थ तो जैन परम्परा में आत्मज्ञ और बौद्ध परम्परा में हेय, ज्ञेय और उपादेय का ज्ञाता ही रहा है। राहुल जी का यह कथन भी किसी सीमा तक सत्य है कि जैनधर्म में प्रारम्भ से ही शारीरिक कार्यों को प्रधानता पर शारीरिक तपस्या पर बल दिया गया है ( दर्शन-दिग्दर्शन, पृ.495-496)। किन्तु उनकी इस धारणा का आधार भी बौद्धत्रिपिटक साहित्य में महावीर के जीवन और दर्शन का जिस रूप में प्रस्तुतिकरण हुआ है वही है -- यहाँ भी उन्होंने जैन आगमों को देखने का प्रयास नहीं किया है। वास्तविकता तो यह है कि जैनदर्शन भी बौद्धों के समान ही मानसकर्म को ही प्रधान मानता है, फिर भी इतना अवश्य सत्य है कि वह कायिककर्म या कायिकसाधना को मानसिककर्म की अनिवार्य फलश्रुति मानता है वह कहता है कि जो विचार में होता है वही आचार में होता है। विचार (मानसकर्म) और आचार ( कायिककर्म ) का द्वैत उसे मान्य नहीं है। विचार से कुछ और आधार में कुछ, इसे जैनधर्म आत्म प्रकचना मानता है, मन Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6